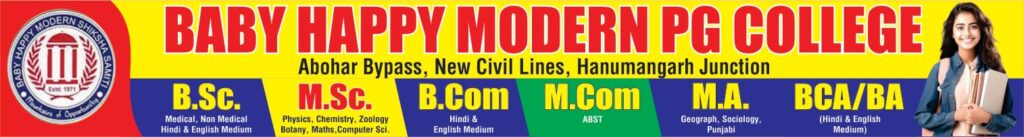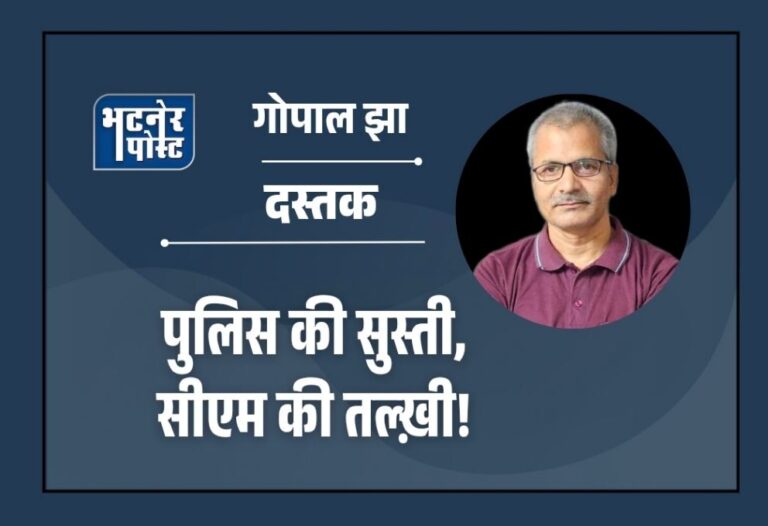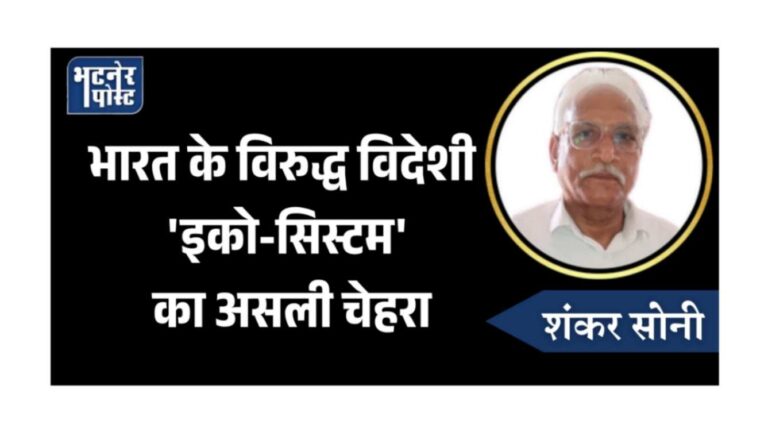गोपाल झा.
22 अप्रैल और 12 जून की तपती दोपहर। एक आम-सी प्रतीत होती तारीख। दोनों अब कैलेंडर में नहीं, इतिहास की काली लकीरों में दर्ज हैं। एक दिन, जब 26 निर्दाेषों की साँसें आतंक के धुएं में घुट गईं। दूसरा दिन, जब 241 जिंदगियाँ आसमान की ऊँचाई से धधकते ज़मीन पर आकर सदा के लिए शांत हो गईं। दो त्रासदियाँ, एक ही सवाल, क्या इन मौतों का कोई जिम्मेदार नहीं?
लोकतंत्र की आत्मा कभी नागरिक की चेतना में बसती थी। आज वह केवल एक शब्द है, खोखला, बुझा हुआ, निर्वात-सा। व्यवस्था, जो कभी जनसेवा की प्रतिज्ञा थी, अब बहानों की शरणगृह बन चुकी है। हर हादसे के बाद वही परिचित संवाद, ‘हमने तुरंत संज्ञान लिया है,’ ‘जांच के आदेश दे दिए गए हैं,’ और फिर वही चिरपरिचित चुप्पी, जैसे व्यवस्था ने भी शोक मनाने से तौबा कर ली हो।
लाल बहादुर शास्त्री का जमीर, जिसने एक रेल दुर्घटना पर बिना दबाव इस्तीफा दे दिया था, अब एक किंवदंती है, जैसे किसी आदर्श लोक की कथा। आज के शासकों में पद छोड़ना तो दूर, गलती मानने का साहस भी विलुप्त होता जा रहा है। दुख की बात यह नहीं कि लोग मरते हैं, दुख यह है कि उनके मरने पर कोई शर्मिंदा नहीं होता।
विपक्ष, जिसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, अब सुविधा की कोठरी में सोता है। उसकी आवाज़ ईडी और सीबीआई की दस्तकों में डूब जाती है। जो कभी सत्ता से सवाल करता था, वह अब अपने ही अतीत के पापों में बंधा हुआ है।
पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, अब गिरवी रखी हुई एक इमारत है, जहाँ सवालों के बदले प्रायोजित स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, और जहां पत्रकार नहीं, प्रवक्ता बैठते हैं। कल तक जो जनता की आवाज़ थे, वे आज सत्ता की गूंज बन चुके हैं।
जनता, जो कभी परिवर्तन की जननी थी, अब भावनाओं के उबाल में विवेक को विसर्जित कर चुकी है। रोटी, पानी, दवा और सुरक्षा की जगह अब धार्मिक नारों, जुलूसों और ट्रोल आर्मी ने ले ली है। सवाल पूछने की कीमत अब सिर्फ बहिष्कार नहीं, चरित्र हनन है। इसलिए लोग चुप हैं, विवश, भयभीत और दिशाहीन।
और फिर, हम पूछते हैं, लोकतंत्र कहां है?
वह कहीं नहीं है। वह संसद की छत के नीचे नहीं, मीडिया की स्क्रीन पर नहीं, न ही मंत्रियों के वक्तव्यों में है। लोकतंत्र अब स्मृति बन चुका है, एक स्वप्न, जो कभी देखा गया था, लेकिन जिसे अब किसी ने ओढ़ना-बिछाना छोड़ दिया है।
267 जिंदगियाँ बुझ गईं, और कोई जिम्मेदार नहीं? क्या हम इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि लाशों की गिनती पर भी आंकड़ों की सफाई देने लगते हैं? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ चुनावों का त्यौहार और सत्ता का उत्सव रह गया है?
यदि आज सवाल नहीं पूछा गया,
यदि आज जवाब नहीं मांगा गया,
तो कल सिर्फ आंकड़े बढ़ेंगे।
और लोकतंत्र की जगह एक सुनसान, सुन्न सन्नाटा ले लेगा, जिसमें ना विवेक होगा, ना संवेदना, और ना ही उम्मीद। वाकई, देश बदल रहा है। पर दिशा क्या है, यह पूछने की हिम्मत अब किसमें बची है? शायद किसी में नहीं। क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। और जब सवाल मर जाते हैं, तब लोकतंत्र भी जीवित नहीं रहता, बस उसका शव पड़ा रहता है, 266 और 1 नई लाश के साथ।