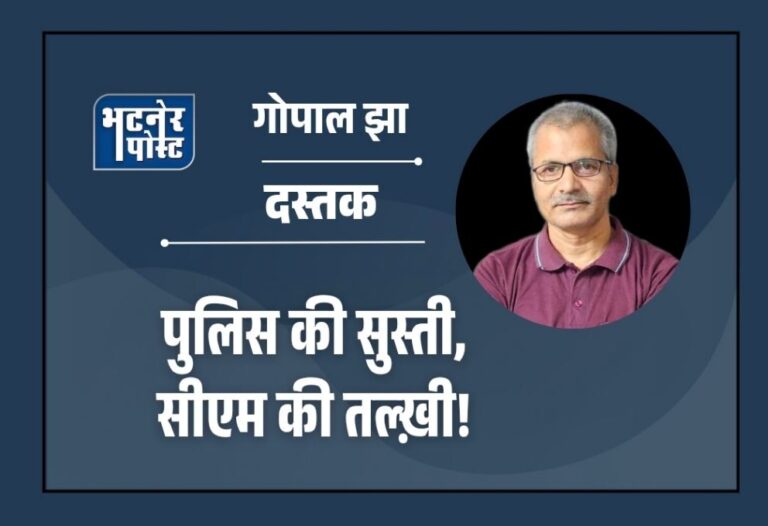गोपाल झा.
पुलिस को समाज का रक्षक और न्याय का पहला द्वार कहा जाता है। आमजन जब भी किसी संकट, अन्याय या अपराध का शिकार होता है, तो सबसे पहले उसी संस्था की ओर देखता है, जो संविधान के नाम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए है। लेकिन यह विडंबना ही है कि जो संस्था पीड़ितों को न्याय दिलाने की पहली और अनिवार्य कड़ी है, वही आज खुद बेइंतहा दर्द से कराह रही है। राजस्थान पुलिस दिवस केवल एक समारोह नहीं, बल्कि आत्ममंथन और चिंतन का अवसर होना चाहिए। एक ऐसा मौका जिसमें हम पुलिस की भूमिका, उससे जनता की अपेक्षाएँ, और इस पूरी व्यवस्था की चुनौतियों को ईमानदारी से समझें।
यह सच है कि हाल के वर्षों में पुलिस की साख पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। किसी निर्दाेष को झूठे मुकदमे में फंसाना, आरोपी को बिना जांच के दोषी मान लेना, राजनीतिक दबाव में काम करना, एफआईआर दर्ज न करना व रिश्वखोतरी जैसे आरोप आम होते जा रहे हैं। इन घटनाओं ने आमजन और पुलिस के बीच की दूरी बढ़ा दी है। यह दूरी केवल अविश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था की नींव भी हिलने लगी है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए केवल पुलिस को दोषी ठहराया जा सकता है? हम भूल जाते हैं कि वर्दी पहनने वाले ये लोग भी हमारे ही समाज से आते हैं। वे भी किसी के बेटे-बेटी, किसी के पति-पत्नी, पिता-माता और किसी परिवार के सदस्य होते हैं। 12-14 घंटे की ड्यूटी, त्योहारों पर ड्यूटी, गर्मी-सर्दी की परवाह किए बिना हर मौके पर तैनाती, और ऊपर से मानसिक दबाव, यह सब एक आम पुलिसकर्मी की दिनचर्या का हिस्सा है।
राजस्थान में आज भी अधिकांश पुलिसकर्मी एक साप्ताहिक अवकाश से वंचित हैं। छुट्टी मिलना ‘उपलब्धि’ समझी जाती है। थानों में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कई बार एक ही पुलिसकर्मी को कई मामलों की विवेचना करनी पड़ती है, जिससे निष्पक्षता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है।
आमजन की अपेक्षा होती है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, अपराध पर नियंत्रण रखे, और हर परिस्थिति में निष्पक्षता बरते। लेकिन इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन और सुविधाएं जरूरी हैं, वे नदारद हैं।
राजस्थान में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। जब एक थाना कई गाँवों या शहर के हिस्सों की जिम्मेदारी अकेले निभाता है, तो क्या हर केस में समय और ध्यान देना संभव है? कई थानों में आज भी आधुनिक उपकरणों की भारी कमी है। साइबर क्राइम जैसे आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और तकनीक अब भी कई पुलिसकर्मियों के लिए दूर की कौड़ी है। राजनीतिक हस्तक्षेप, मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया पर छवि खराब करने की घटनाएं पुलिसकर्मियों के मनोबल को प्रभावित करती हैं।
ऐसे में सवाल वाजिब है कि पुलिस और समाज के बीच का सेतु कैसे मजबूत हो? दरअसल, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, समयबद्ध ड्यूटी और ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त सुविधा दी जानी चाहिए। थानों में स्टाफ की पर्याप्त पूर्ति से यह संभव हो सकता है। तनाव और डिप्रेशन से जूझते पुलिसकर्मियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। ‘मनोबल क्लिनिक’ जैसे प्रयासों को संस्थागत रूप दिया जाए। बदलते अपराध स्वरूपों के अनुरूप पुलिस को निरंतर प्रशिक्षित करना आवश्यक है। साइबर क्राइम, डिजिटल ट्रैकिंग, और साक्ष्य प्रबंधन में दक्षता अनिवार्य हो चुकी है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल को अपनाना होगा। ‘बीट कॉन्स्टेबल’ की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए स्पष्ट नियमावली बने। पुलिस का ट्रांसफर-पोस्टिंग पारदर्शी तरीके से हो। मीडिया और समाज दोनों को चाहिए कि अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करें। सम्मान और प्रशंसा भी मनोबल बढ़ाने का अहम माध्यम है।
राजस्थान पुलिस दिवस केवल सम्मान का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन है। यह अवसर है पुलिस व्यवस्था को केवल आलोचना के नजरिए से नहीं, बल्कि सुधार की दृष्टि से देखने का। यह स्वीकार करना जरूरी है कि पुलिस की भूमिका समाज में अनिवार्य और चुनौतीपूर्ण है। यदि हम उनसे बेहतर सेवाओं की अपेक्षा रखते हैं, तो उन्हें बेहतर संसाधन, बेहतर वातावरण और बेहतर सम्मान देना भी हमारा दायित्व है। एक सशक्त पुलिस बल ही एक सशक्त लोकतंत्र की गारंटी है। और यह तभी संभव है जब हम ‘वर्दी के पीछे के इंसान’ को भी उतना ही सम्मान दें, जितना ‘कानून के रक्षक’ को।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर हैं