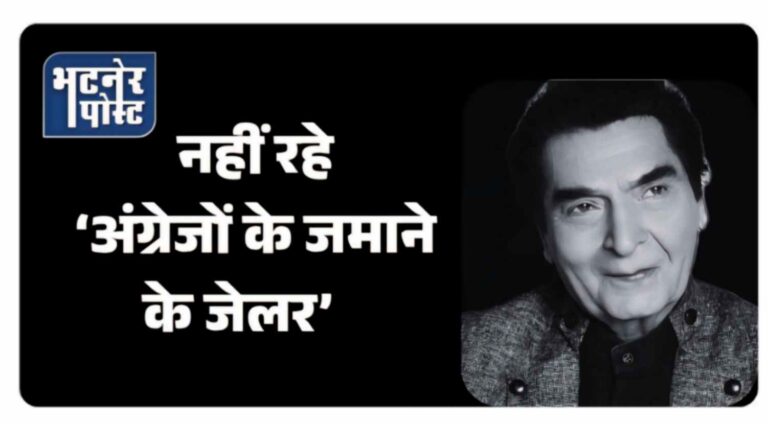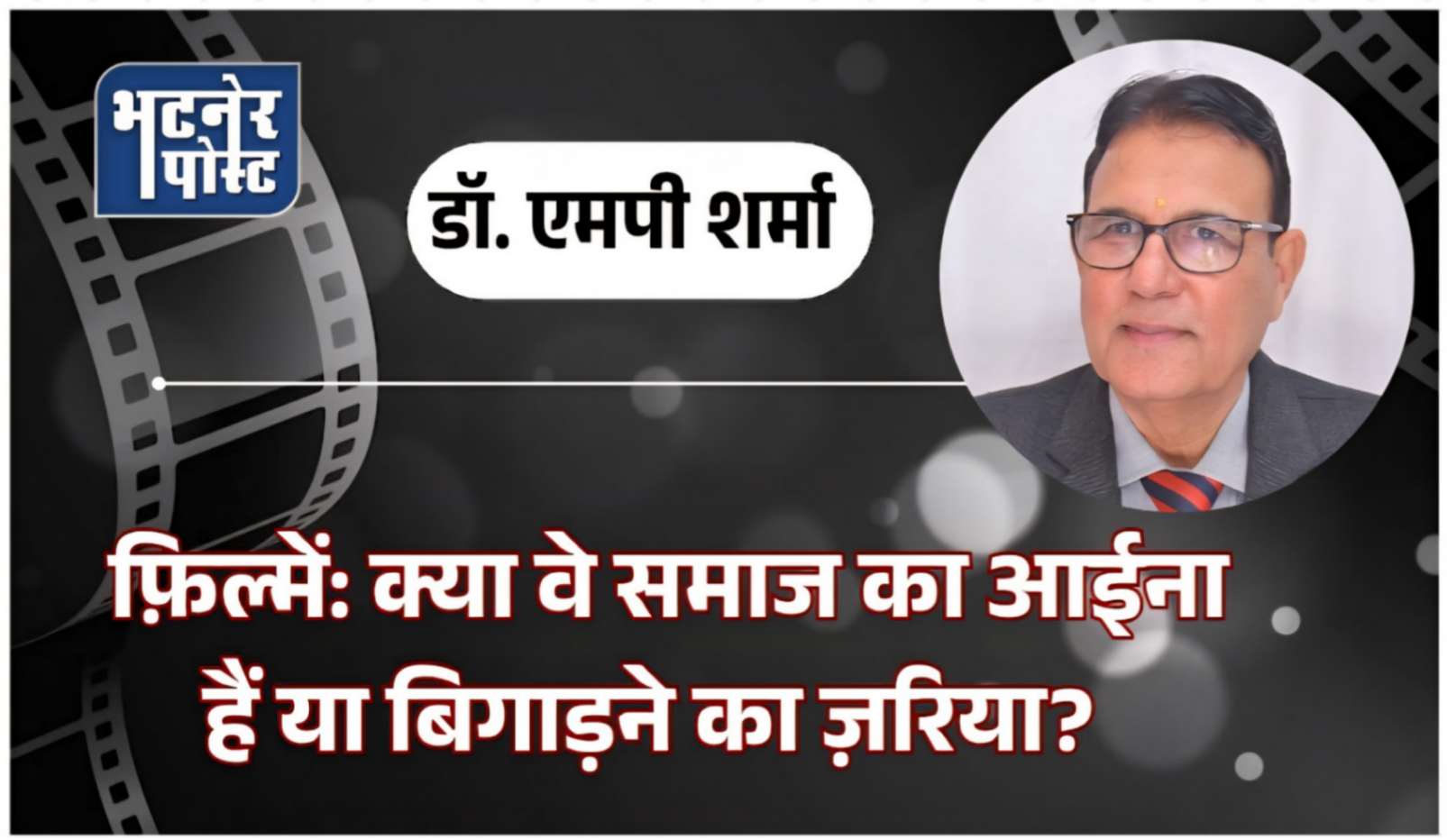

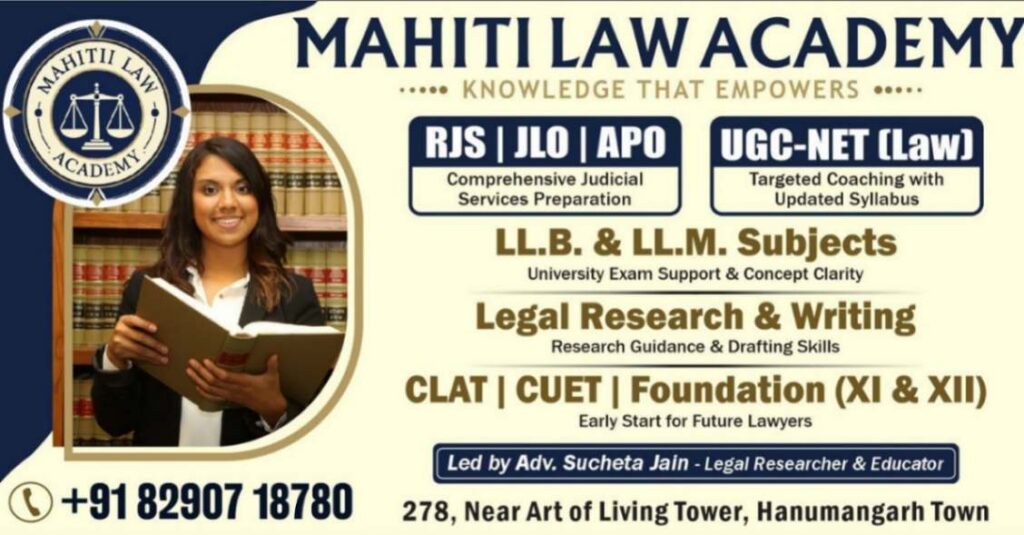


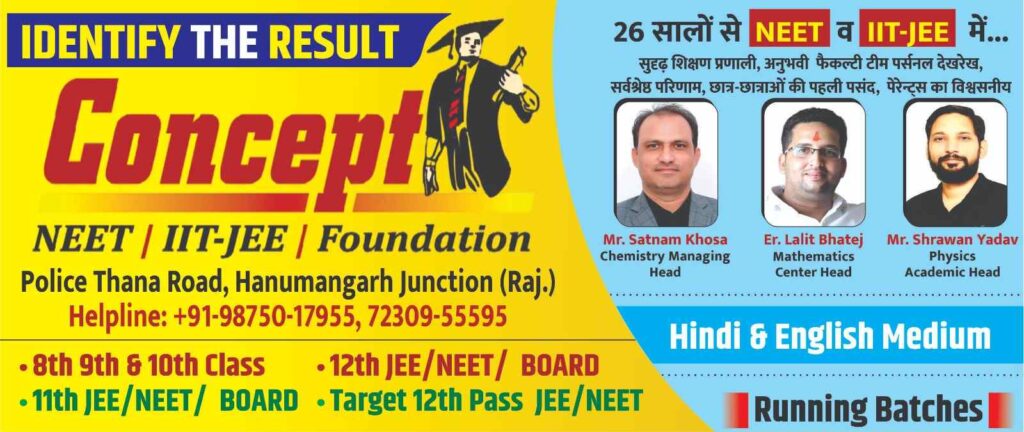

डॉ. एमपी शर्मा.
आज के दौर में फ़िल्में महज़ दो-तीन घंटे का मनोरंजन नहीं रह गई हैं। वे हमारे समाज, संस्कृति और सोच का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं, जो हमें हमारी ही हकीकत दिखाती हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये युवाओं को बिगाड़ती हैं और समाज में अपराध और भौतिकता को बढ़ावा देती हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या फ़िल्में सिर्फ दर्पण हैं या दिशाहीन करने वाली राहें?
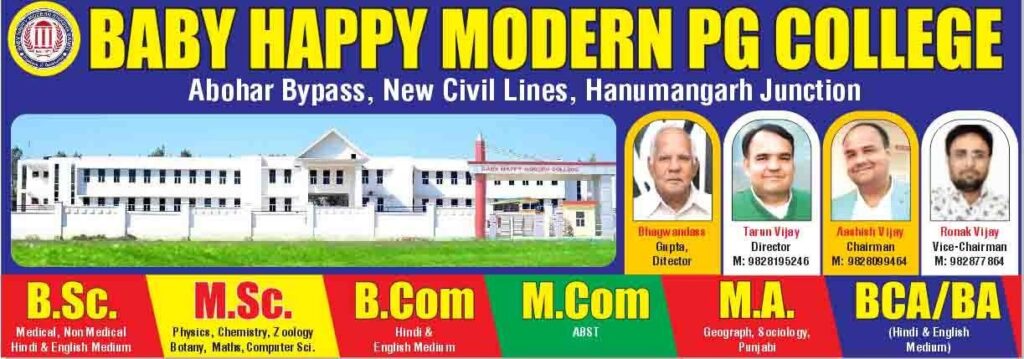
भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फ़िल्में बनी हैं जिन्होंने समाज की कड़वी सच्चाइयों को बेबाकी से पेश किया। ये फ़िल्में सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि उस दौर के सामाजिक दस्तावेज़ थीं।
‘सत्यकाम’ (1969): यह फ़िल्म आदर्शवाद और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई को दिखाती है। धर्मेंद्र अभिनीत यह फ़िल्म उस समय की ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की कसौटी पर खरी उतरती है।
‘अर्धसत्य’ (1983): ओम पुरी के शानदार अभिनय ने पुलिस तंत्र और राजनीति के गठजोड़ को उजागर किया। यह फ़िल्म दिखाती है कि कैसे एक ईमानदार पुलिसवाला इस सिस्टम में फँसकर अपनी पहचान खोने लगता है।
‘अर्थ’ (1982): महेश भट्ट की यह फ़िल्म रिश्तों और विवाह के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देती है। इसने स्त्री की आत्मनिर्भरता और उसके अपने निर्णय लेने के अधिकार पर एक नई बहस छेड़ दी।
‘पथेर पांचाली’ (1955): सत्यजित राय की यह कालजयी फ़िल्म भारतीय ग्रामीण जीवन की गरीबी और संघर्ष का अद्भुत चित्रण करती है। इसे दुनिया भर में भारतीय यथार्थवाद का प्रतीक माना गया।

इन फ़िल्मों ने दर्शकों को सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उन्हें अपने समाज की कमज़ोरियों और संघर्षों को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। गंभीर सिनेमा के अलावा, भारतीय फ़िल्म उद्योग ने हमेशा व्यावसायिक और मनोरंजक फ़िल्में भी बनाई हैं, जो लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाती हैं।

‘बॉबी’ (1973): इस फ़िल्म ने किशोर प्रेम को पर्दे पर एक नई पहचान दी और युवा पीढ़ी की भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया।
‘हम आपके हैं कौन’ (1994): यह फ़िल्म परिवार, रिश्ते और भारतीय विवाह की परंपरा का भव्य उत्सव थी। इसने लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया।
‘कुछ कुछ होता है’ (1998): दोस्ती और प्यार के आधुनिक संबंधों को दिखाती इस फ़िल्म ने युवाओं के बीच एक नई लहर पैदा की। ये फ़िल्में भले ही शिक्षाप्रद न हों, लेकिन ये जीवन को हल्का-फुल्का और खुशनुमा बनाने में ज़रूरी भूमिका निभाती हैं।
क्या फ़िल्में समाज को बिगाड़ती हैं?
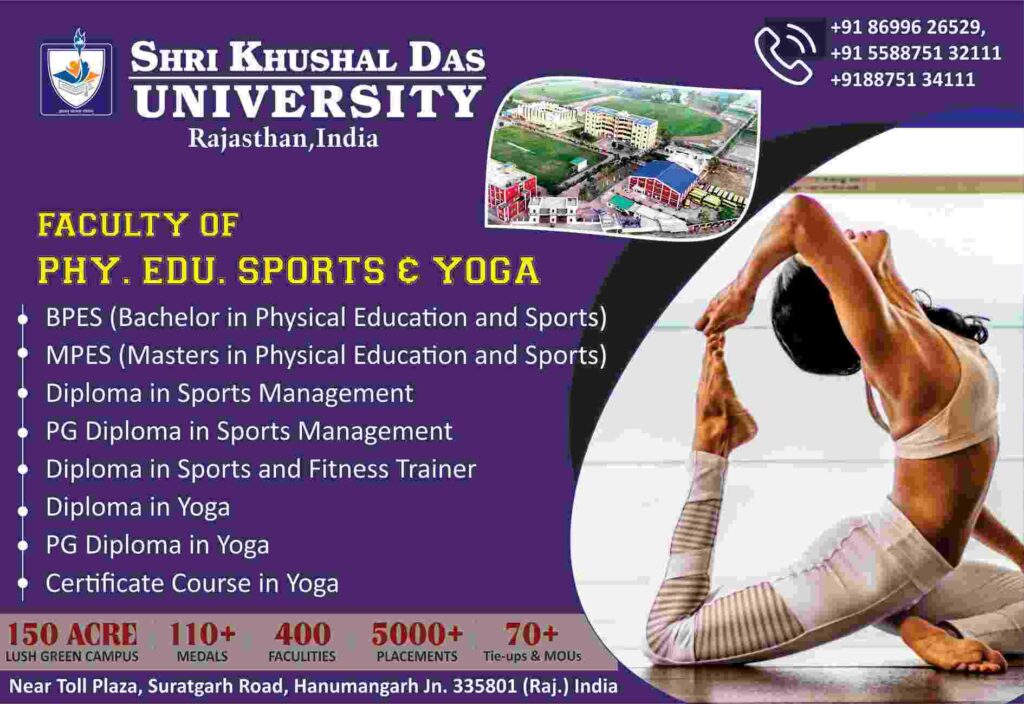
यह सवाल अक्सर उठता है कि फ़िल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा, ग्लैमर और नकारात्मक किरदार क्या समाज को नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं? फ़िल्मों में नायक का सिगरेट पीना या ‘एंटी-हीरो’ किरदारों का महिमामंडन, जैसे ‘शोले’ के गब्बर या गैंगस्टर फ़िल्मों के पात्र, युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं।
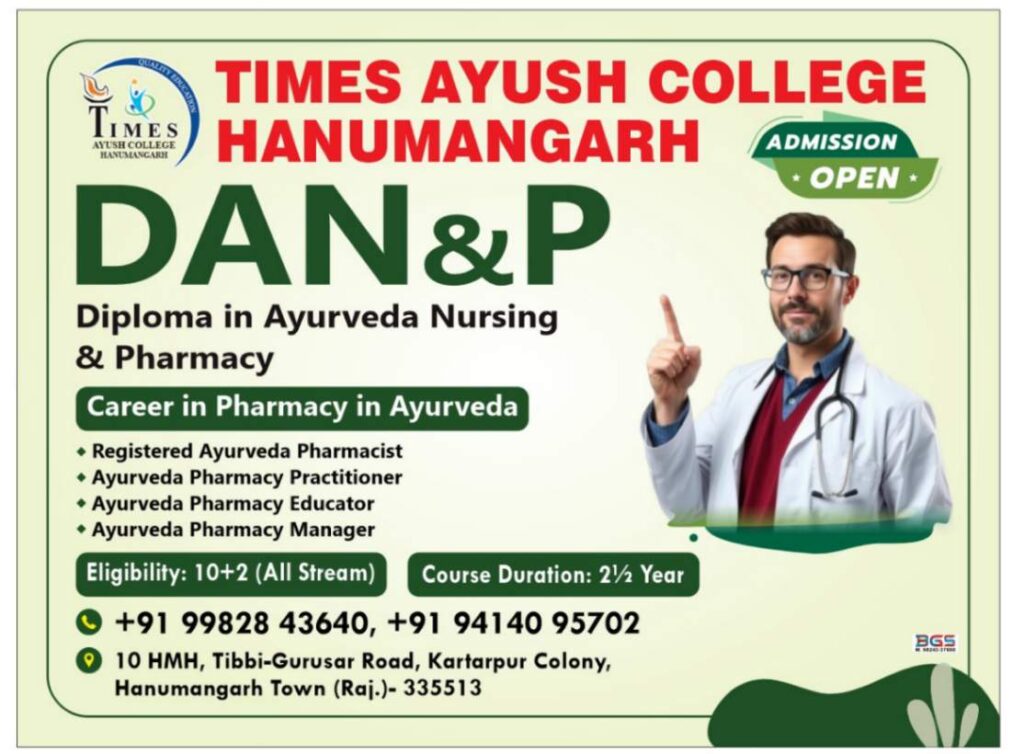
यह सच है कि ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ (2010) जैसी फ़िल्मों ने माफ़िया की दुनिया को ग्लैमरस बनाकर पेश किया, जिससे कुछ लोग अपराध को ‘हीरोइक’ मानने लगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर दर्शक का अपना विवेक होता है। जिस तरह एक समाचार देखकर कोई हिंसक नहीं हो जाता, उसी तरह एक फ़िल्म देखकर कोई अपना जीवन पूरी तरह वैसा नहीं बना लेता।
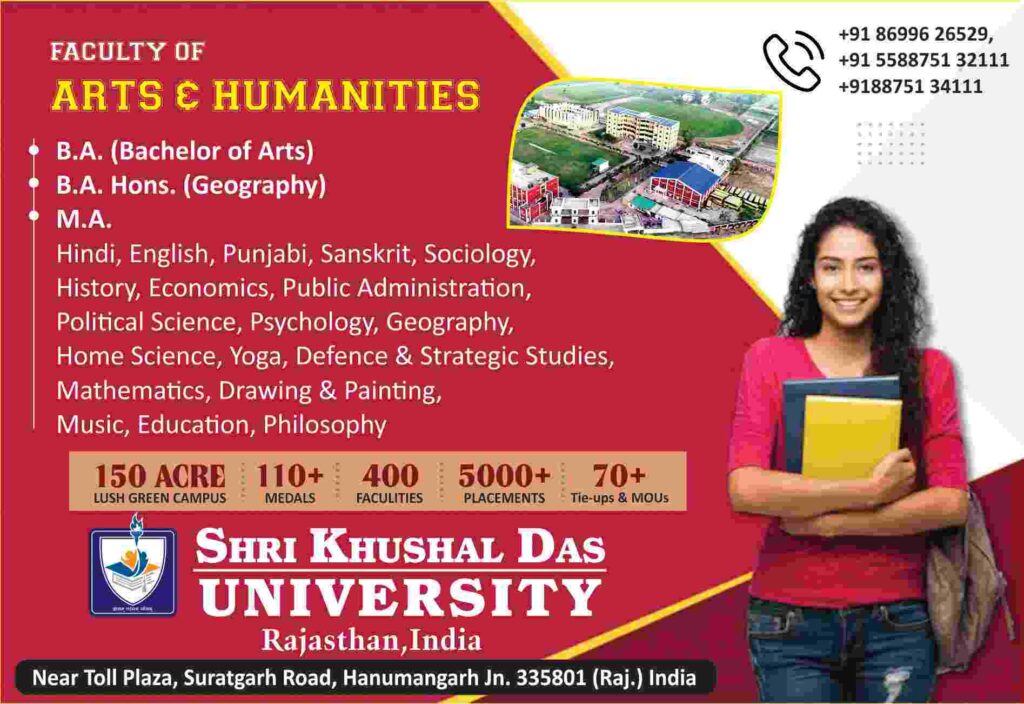
फ़िल्में न तो केवल समाज का आईना हैं और न ही सिर्फ बिगाड़ का ज़रिया। वे कल्पना और यथार्थ का एक मिला-जुला रूप हैं। कुछ फ़िल्में हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारे संघर्षों को सामने लाती हैं, जबकि कुछ सिर्फ़ मनोरंजन का साधन होती हैं।
दर्शक के रूप में, ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम क्या ग्रहण करते हैं। हमें फ़िल्मों को वास्तविकता समझकर नहीं जीना चाहिए। हमें मनोरंजन के लिए हल्की-फुल्की फ़िल्में भी देखनी चाहिए, और हमें सोचने पर मजबूर करने वाली गंभीर फ़िल्में भी देखनी चाहिए।
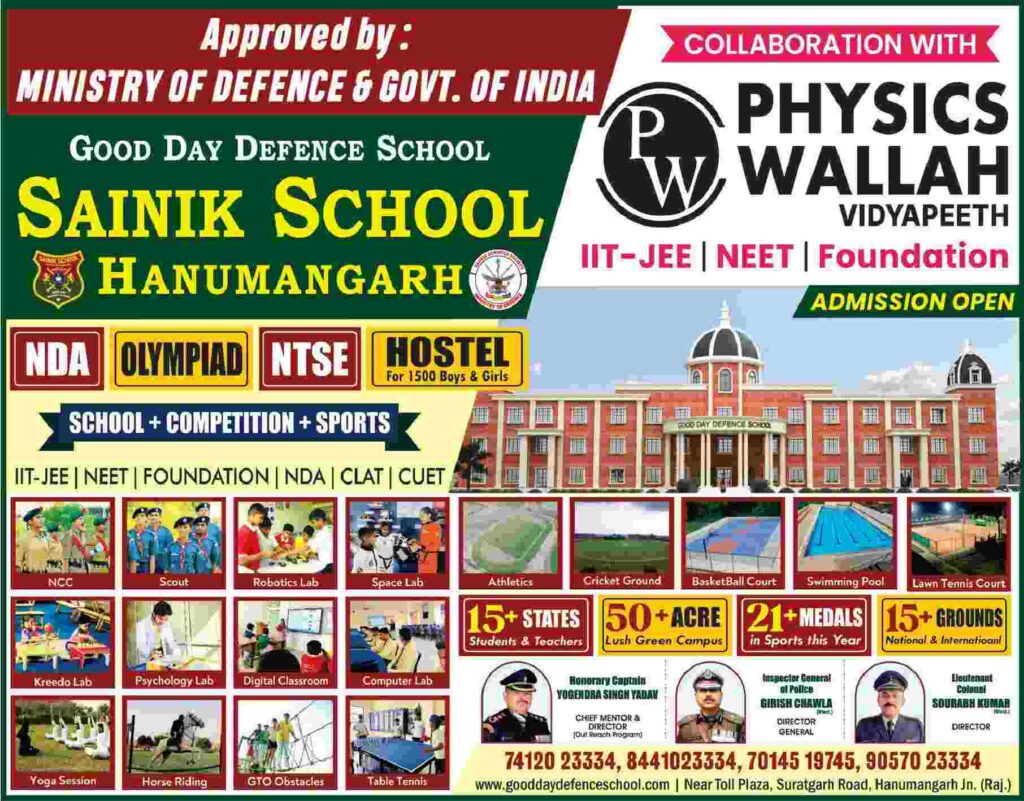
जैसे भोजन में मिठाई भी होती है और औषधि भी, उसी तरह फ़िल्में भी कभी हमें हँसाती हैं, कभी हमें रुलाती हैं, और कभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमें इन सभी का संतुलन के साथ आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में, फ़िल्मों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं।
-लेखक सीनियर सर्जन और आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं