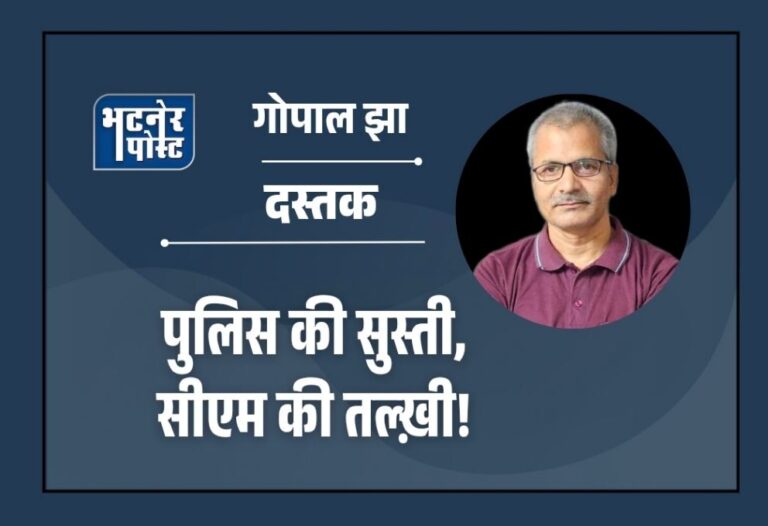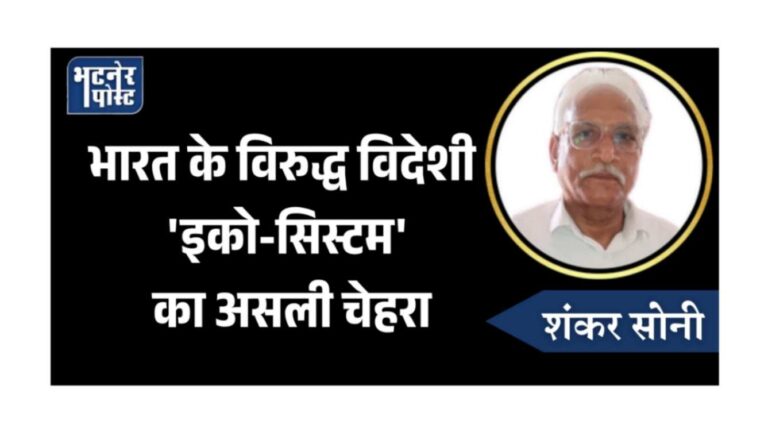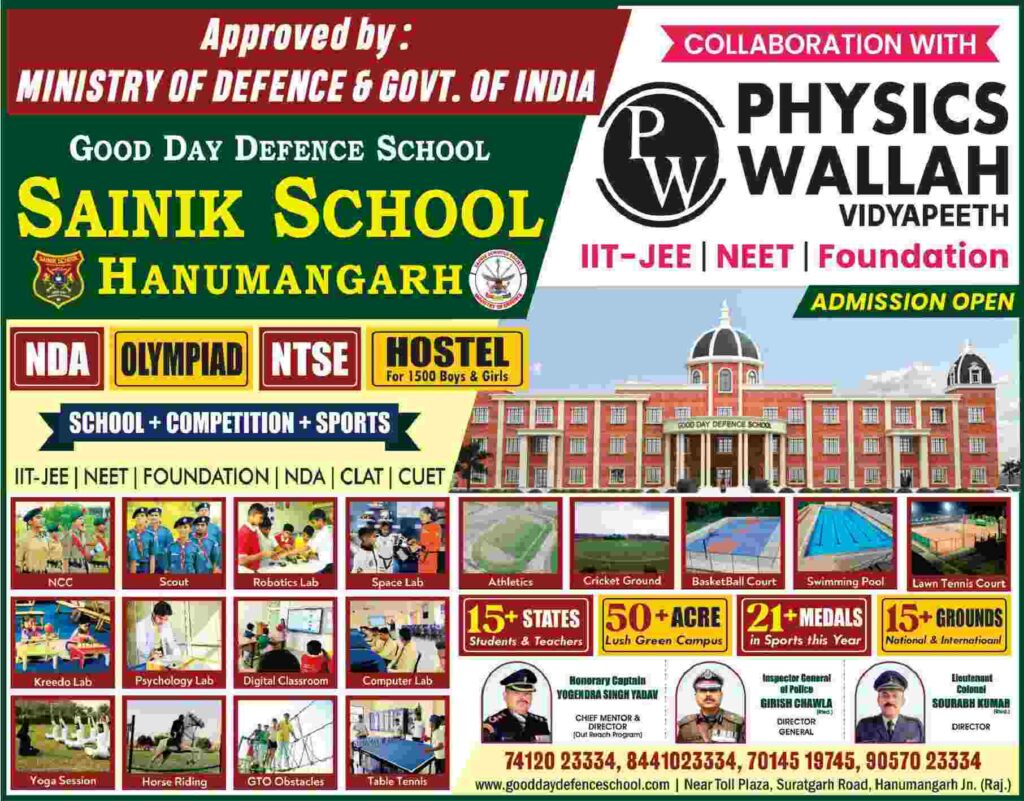
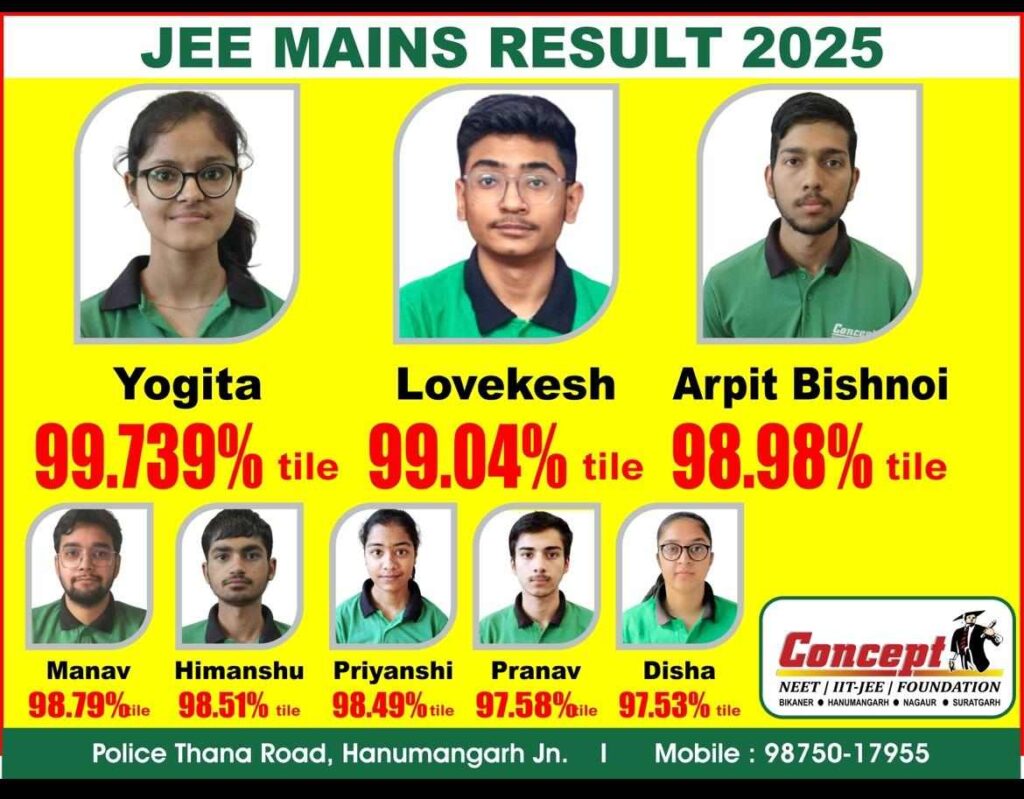
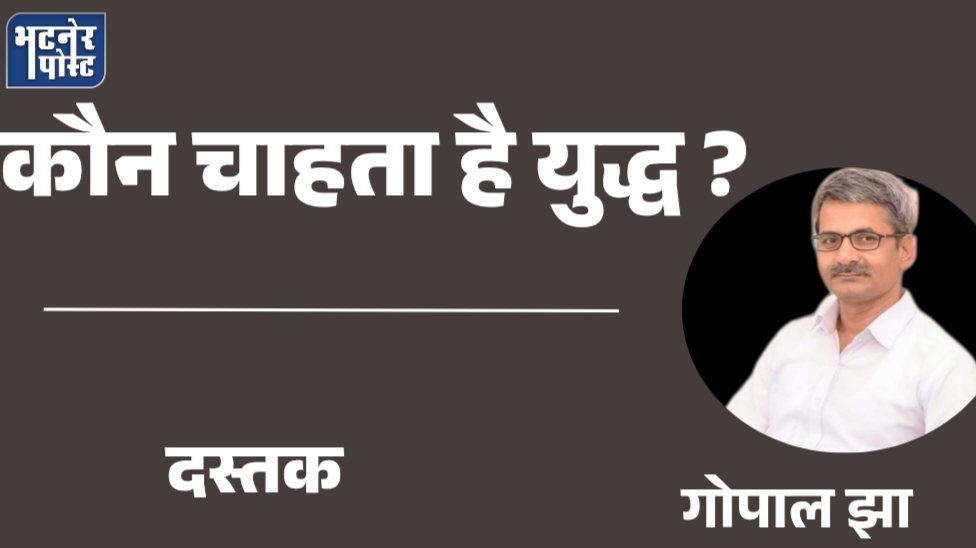
गोपाल झा.
भारत और पाकिस्तान। दो देश लेकिन सवाल एक। क्या, दोनों देशों के सैनिक अब चौथी बार आमने-सामने होंगे? दरअसल, युद्ध की चर्चा सरेआम है। लेकिन क्या, युद्ध इतना आसान है ? सच तो यह है, युद्ध को लेकर समाज दो हिस्सों में बंट जाता है, एक ओर वे जो युद्ध को राष्ट्र की आन-बान-शान का प्रतीक मानते हैं, दूसरी ओर वे जो इसके भयावह परिणामों की कल्पना मात्र से सिहर उठते हैं। दुर्भाग्यवश, जो सबसे अधिक मुखर होकर युद्ध की पैरवी करते हैं, वे अक्सर खुद युद्ध के मैदान से कोसों दूर होते हैं। न वे बंदूक उठाते हैं, न सीमा पर तैनात होते हैं, और न ही उनका परिवार किसी वीरगति को प्राप्त होने के जोखिम से गुजरता है। बलिदान की आंच सिर्फ और सिर्फ सैनिकों और उनके परिवारों को झुलसाती है।
राजनीति में बैठे लोगों की भूमिका इस संदर्भ में और भी अधिक जटिल हो जाती है। वे युद्ध के पक्ष में जनभावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। युद्ध की घोषणाएं, सैनिकों के पराक्रम की प्रशंसा और राष्ट्रवाद की भावनात्मक लहरें जनमानस को प्रभावित करती हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध का दंश झेलते हैं वे निर्दाेष नागरिक, जो सीमाओं पर रहते हैं, जिनके घर बमों की गूंज से हिलते हैं, और जिनके जीवन पल में उजड़ जाते हैं।

इतिहास गवाह है कि जब-जब युद्ध हुए हैं, नुकसान केवल सीमा पर नहीं, घरों के भीतर हुआ है। 1947 के विभाजन के समय बंटे परिवारों की पीड़ा आज भी जीवित है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध हो चुके हैं, लेकिन दोनों ओर की आम जनता में आज भी आपसी रिश्ते, संवेदनाएं और प्यार की कहानियाँ मौजूद हैं। आज भी सीमापार रिश्तेदारों से मिल पाने की उम्मीद में कितने ही परिवार वीज़ा कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। सवाल यह है कि क्या हम सरहदों की सीमाएं तो तय कर सकते हैं, लेकिन दिलों की सीमाएं कौन तय करेगा?
जहां तक पाकिस्तान की भूमिका की बात है, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वह वर्षों से कट्टरपंथियों के प्रभाव में रहा है। आतंकवाद को पनाह देना, धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काना और वैश्विक मंचों पर दोहरी नीति अपनाना उसकी पुरानी आदत है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर पाकिस्तानी आतंकी नहीं होता, जैसे हर भारतीय शांतिवादी नहीं होता। कट्टरता और अज्ञानता का मेल इंसान को दानव बना देता है, यह किसी एक देश की समस्या नहीं, समूची मानवता के लिए खतरा है।

भारत जैसे देश, जिसने ष्वसुधैव कुटुम्बकम्ष् का संदेश दिया है, के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। भारत की सैन्य क्षमता पर कोई संदेह नहीं हैकृहमारी सेना ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। लेकिन युद्ध का विकल्प तभी आना चाहिए जब सभी राजनयिक, कूटनीतिक और सुरक्षात्मक प्रयास विफल हो जाएं। आतंकियों की हर हरकत का जवाब देना आवश्यक है, लेकिन यह जवाब भावनाओं की नहीं, रणनीतिक चतुराई की भाषा में होना चाहिए।
हाल ही में हुए आतंकी हमलों में सरकार की खुफिया तंत्र की विफलता भी उजागर हुई है। पहलगाम जैसी घटनाएं बताती हैं कि हमें युद्ध नहीं, पहले अपनी खुफिया और सुरक्षा प्रणाली को अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें जनता के जीवन की रक्षा करनी है, न कि भावनात्मक लहर में बहकर निर्दाेषों की जान को संकट में डालना है।

राजनेताओं की भूमिका यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वे देशहित में तटस्थ और विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे, या फिर जनभावनाओं की सवारी करके चुनावी लाभ उठाएंगे? क्या वे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देंगे या फिर विदेश यात्राओं और भाषणों तक सीमित रहेंगे? और यह सवाल केवल सरकार से नहीं, आम जनता से भी है, क्या हम सोशल मीडिया पर ष्युद्ध चाहिएष् की पोस्ट शेयर कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं?
युद्ध कोई फिल्म नहीं, जिसमें अंत में हीरो जीतता है। यह रक्तपात की वह त्रासदी है जिसमें मानवता हारती है, सभ्यता रोती है और पीढ़ियाँ खामोश हो जाती हैं। इसलिए, यह समय युद्ध के लिए उकसाने का नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा नीति, खुफिया तंत्र और सामरिक संतुलन को मजबूत करने का है।
भारत की आत्मा शांति में बसती है, लेकिन आत्मरक्षा उसका धर्म है। यदि कोई उसकी सीमाओं, नागरिकों या अस्मिता पर हमला करता है, तो वह एकजुट होकर उसका मुँहतोड़ जवाब देना जानता है। परंतु यह प्रतिकार युद्ध के शोर में नहीं, बल्कि विवेक, तैयारी और सामूहिक संकल्प में निहित होना चाहिए।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर हैं