


गोपाल झा.
देश आजादी की वर्षगांठ की सिल्वर जुबली मनाकर सुस्ता रहा था। इसके करीब दो साल बाद हमारी पीढ़ी दुनिया में आई। भूख की व्याकुलता। अभाव की चिंता। दकियानुसी समाज। अशिक्षा का अभिशाप। अनिश्चितताओं का दौर था वह। भोग और विलासिता चंद परिवारों की गुलाम थी। माहौल कुछ ऐसा ही था। पूरे गांव में शायद ही किसी के पास मोटरसाइकिल हो। कार-जीप का तो कहना ही क्या!
हां, इन सबके बावजूद लोग बेहद दिलदार थे। सूखी रोटी के साथ चुटकी भर नमक खाकर भी मस्त रहते थे। तन ढकने लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं लेकिन इज्जत और सम्मान में कोई कमी नहीं। लोगों के पास स्वाभिमान था। वे बातों के धनी थे। बात और बाप को एक समझने वाले।

करीब पांच दशक बाद जब अतीत के पन्ने को पलटते हैं तो लगता है, दुनिया बदल गई है। लोग बदल गए हैं। समाज बदल गया है। और तो और, हम भी बदल गए हैं। क्या, इस ‘बदलाव’ का जश्न मनाना उचित होगा ?
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और भी अन्य क्षेत्रों में हमने विकास की रफ्तार की तीव्रता को महसूस किया है। कहना न होगा, जिस तेजी से विकास हुआ, नैतिक पतन का सिलसिला भी उसी गति से जारी है। उस वक्त विद्वान लोग फिक्रमंद नजर आते कि कहीं विकास के नाम पर देश के लोग पश्चिमी सभ्यता की प्रदूषित हवा के कारण अनैतिकता के ‘संक्रमण’ की चपेट में न आ जाएं। सच तो यह है कि उनकी चिंता उचित थी। देश में राष्ट्रवाद व हिंदुत्व का ‘बोलबाला’ है। हकीकत यह है कि राष्ट्रवाद व हिंदुत्व की सवारी करने वालों के पैरों तले संस्कृति की जमीन ही नहीं। सियासत ने धर्म के मर्म को निगल लिया और हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी गौरवशाली संस्कृति को। धर्म और संस्कृति के नाम पर हम ‘ढोंगी’ बनकर रह गए हैं।

परिणाम सामने है। अनाप-शनाप पैसे कमाने वालों के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे। अनैतिक कारोबार के कारण उन पर मुकदमों का अंबार है। कोर्ट-कचहरी का चक्कर। कर्ज का बोझ। चौन से दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। परिवार का सुख तो जैसे मयस्सर ही नहीं। भला, संपत्ति अर्जित करने का यह कैसा नशा है ? इससे क्या हासिल होगा, पता नहीं।
पैसा नहीं था, परिवार का साथ था। सुख सुविधाएं नहीं थीं, परिजनों के साथ रहने से नैसर्गिक सुख की अनुभूति होती थी। हवाई यात्रा उबाऊ लगने लगी है लेकिन कभी मांग कर ली गई साइकिल पर चढ़ने का भी अलग ही आनंद था। परिवार में रिश्तों का बंधन था। मसलन, मां-बाप, भाई-बहिन, दादा-दादी, काका-काकी, भाभी, बेटा-बेटी, भतीजा-भतीजी, बूआ-फूफा, मौसा-मौसी, नाना-नानी, मामा-मामी, साला-साली, साढू, ननद-भौजाई वगैरह। रिश्ते आज भी हैं, अर्थ बदल गए हैं। अपनापन की जगह ‘औपचारिकता’ ने ले ली है।

रुहानी रिश्ते अर्थ खोते जा रहे हैं और औपचारिक रिश्ते ‘प्रगाढ़’ होने का दिखावा करते दिख रहे। जब परिवार से असलियत गायब होती है तो जिंदगी में खोखलापन की शुरुआत होती है। धन और वैभव के बावजूद नीरसता खुद की जगह बनाने लगती है। मन तो वैसे भी चंचल होता है, उसे समझाना बेहद मुश्किल है। मन और माहौल बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। सच कहिए तो इंसान फिर इंसान नहीं रह जाता है। वह मशीन में परिवर्तित होने लगता है। याद रखिए, मशीन के पास ‘चलने’ के अलावा कुछ नहीं होता। उसमें विवेक नहीं होता। धैर्य नहीं होता। समझ नहीं होती। चेतना नहीं होती। आज मनुष्य अपने मूल स्वभाव को छोड़ता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद मन स्थिर नहीं। अज्ञात भय से त्रस्त। हर वक्त पाने की चाहत। धैर्य धारण करने में असमर्थता। निगाहों में उलझन है, दिलों में उदासी। आखिर क्यों ?
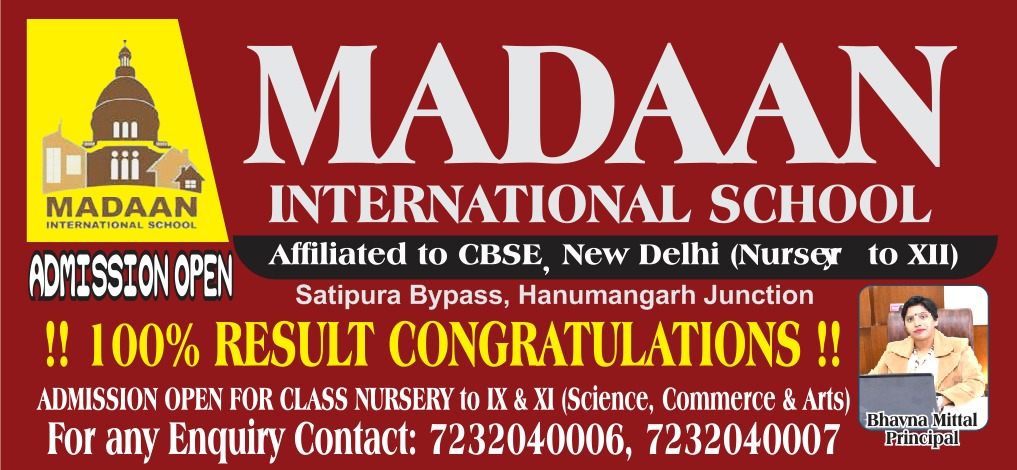
हमने अभाव को देखा नहीं, भोगा भी है। उसमें भी खुशी की अनुभूति हासिल की है। अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने वालों का पतन देखा है। कभी आसमान में उड़ने वालों को फिर जमीं पर रेंगते हुए देखा है। कहते हैं न, अति सर्वत्र वर्जयेत। धन के लिए मन को मारना महापाप है। मन को निर्मल रखना सबसे बड़ी चुनौती है और आसान भी। मन पवित्र है तो मिजाज खुश रहेगा। मिजाज खुश है तो दिमाग तरोताजा। दिमाग में ताजगी है तो कोई व्याधि आपको छूने से भी घबराएगी। सच तो यह है कि जिसके माध्यम से हम सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सुख है ही नहीं। सुख को खोजने का रास्ता ही गलत है।
बहरहाल, आज इतना ही। अगले अंक में तलाशेंगे सुख का वास्तविक रास्ता। बस, जुड़े रहिए…. ‘ज से जिंदगी….’ के साथ। हर मंगलवार।



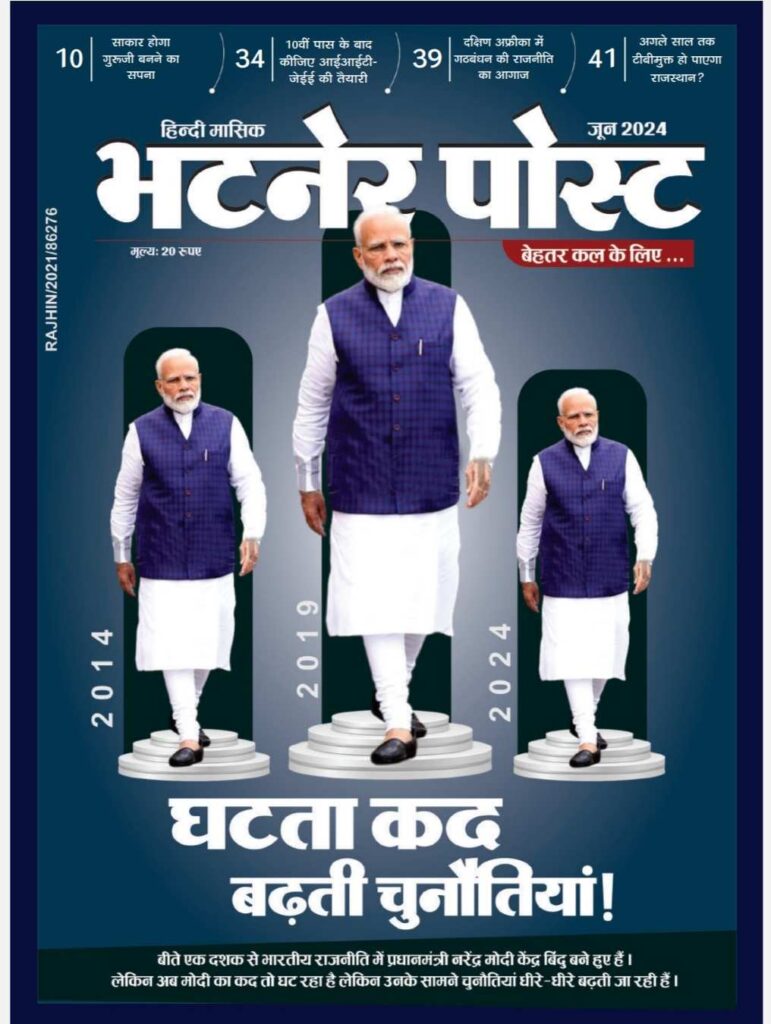

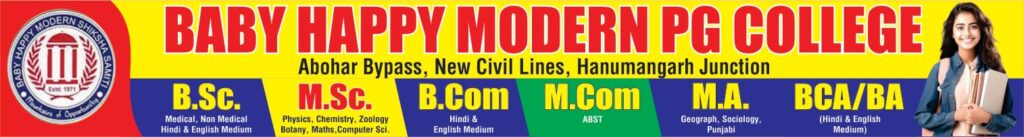




बेहतरीन बात बेहतरीन तरीके से रखी आपने गोपाल भाई
अजब बात यह है कि आज नैतिक व्यक्ति भी निंदक होता जा रहा है हमेशा दूसरों का। क्योंकि उसका सारा रस ही इस बात में है कि वह नैतिक है और दूसरे लोग नैतिक नहीं हैं। इसलिए जो कौम इस तरह से नीति के चक्कर में पड़ जाती है, वह निंदक हो जाती है। हम अपने ही मुल्क में इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं।
अभी संस्कृति ,आदर्श ,चरित्र ,जीवन मूल्यों पर ग्रहण चल रहा है । इस ग्रहण को हटने में अभी कम से कम 40 वर्ष और लगेंगे।
इस इन व्यवस्थाओं में बस शरीर को जिंदा रखना है , आत्मा को सुलाए रखना है । लक्ष्य विहीन जिंदगी को किसी तरह से पूरा करना है यही जीवन है ….. ज ……से जिंदगी
वाह भाई गोपाल जी ! बेहद शानदार आलेख लिखा है । तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी शब्द हमें सम्बल देता है । आप जैसे मित्रों के आलेख पढ़कर कुछ घुटन कम होती है । उदासी के बावजूद कुछ अच्छा होने की लालसा में चेहरे पर उदासी के बादल छंटने लगते हैं । बड़ा खतरनाक दौर है । आजादी के समय प्रगतिशील लोगों ने क्या सपने देखे थे । किसने सोचा था ऐसा दौर भी आएगा । इस उम्मीद से लिखते रहिए की शब्द कभी भौंतरे नहीं होते । प्रेमादर