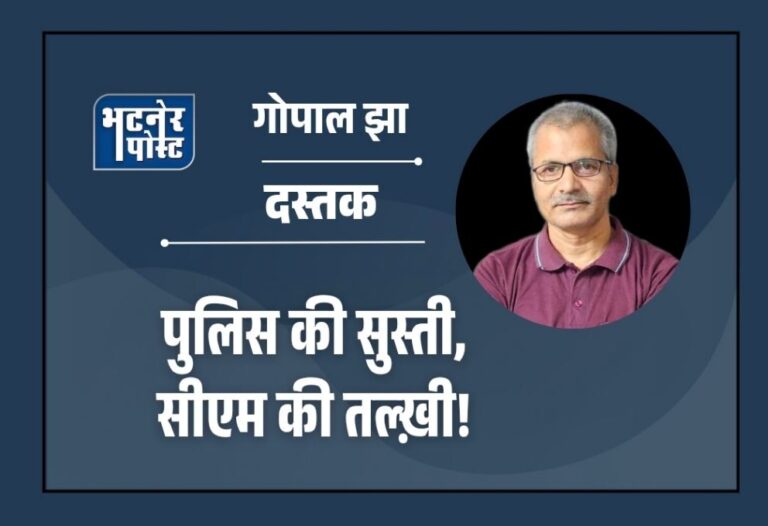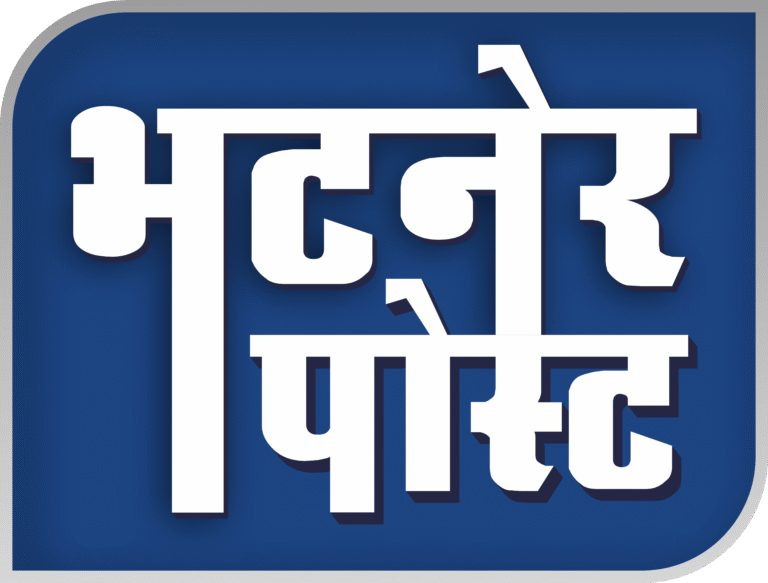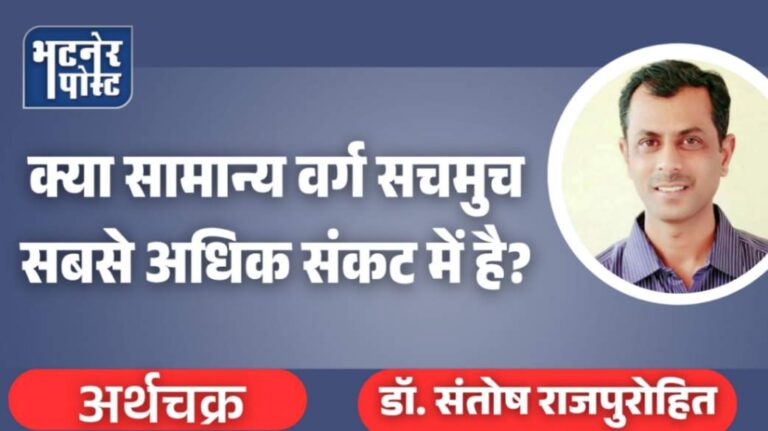गोपाल झा.
आज का समय, जिसे हम तकनीक और संचार क्रांति का युग कहते हैं, एक विचित्र विरोधाभास लेकर आया है, एक ओर मनुष्य चांद पर बसने की योजनाएं बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अपने ही भीतर सिमटता जा रहा है। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन स्वयं के ‘मैं’ से बाहर झांकने की फुर्सत नहीं है। यही ‘मैं’ जब आवश्यकता से अधिक हो जाए, जब हर आईना उसी की तस्वीर दिखाए, जब हर संवाद का केंद्र वही हो, तब वह ‘आत्ममुग्धता’ बन जाती है, एक ऐसी मानसिक स्थिति, जो धीरे-धीरे व्यक्ति को भीतर से खोखला करती जाती है।
आत्ममुग्धता कोई साधारण प्रवृत्ति नहीं है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जो व्यक्ति को दूसरों की दृष्टि से देखने की क्षमता से वंचित कर देती है। आत्ममुग्ध व्यक्ति को अपना ही स्वर मीठा लगता है, अपना ही चेहरा प्रिय लगता है और अपनी ही राय अंतिम सत्य लगती है। वह आत्म-प्रशंसा के चश्मे से दुनिया को देखता है और अपने ही महत्व में इस कदर डूब जाता है कि अन्य किसी का मूल्यांकन, विचार या योगदान उसे नगण्य लगने लगता है।
इस मानसिक विकृति को बढ़ाने का कार्य आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बखूबी किया है। इन मंचों पर लोग अपनी उपलब्धियों, चेहरे, विचारों और गतिविधियों को इस तरह प्रदर्शित करते हैं मानो विश्व का समूचा अस्तित्व उनके इर्द-गिर्द घूम रहा हो। ‘लाइक’, ‘कमेंट’ और ‘शेयर’ की आभासी दुनिया में आत्ममुग्धता को मान्यता और सम्मान का मुखौटा मिल गया है। अब तो जैसे हर व्यक्ति ‘ब्रांड’ बनना चाहता है, अपने आप का प्रचारक, अपने विचारों का वाहक और अपने जीवन का केंद्र।
इस आभासी आत्मप्रशंसा की दौड़ में लोग यह भूल जाते हैं कि समाज केवल ‘मैं’ से नहीं, ‘हम’ से बनता है। केवल अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जब समाज में हर व्यक्ति केवल अपने महत्त्व का गान करने लगे और दूसरों के गुणों को नकारने लगे, तब वह समाज आत्मकेंद्रितता की दलदल में फंस जाता है।
आत्ममुग्धता की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह व्यक्ति को अकेला कर देती है। शुरू में लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, उसकी आत्मप्रशंसा को सुनते हैं, परंतु धीरे-धीरे वह दूसरों के लिए उबाऊ और आत्मकेंद्रित प्रतीत होने लगता है। ऐसे लोग संवाद नहीं करते, केवल भाषण देते हैं; वे संबंध नहीं निभाते, केवल अपेक्षा करते हैं; वे सराहना नहीं करते, केवल चाहते हैं कि उनकी सराहना हो।
इस प्रवृत्ति का सामाजिक प्रभाव और भी घातक होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति को परिवार का सुख, समाज की ज़रूरतें और राष्ट्र की प्राथमिकताएँ गौण लगती हैं। उसके लिए केवल उसकी पहचान, प्रतिष्ठा और प्रगति मायने रखती है। राजनीति में ऐसे लोगों की बढ़ती उपस्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डालती है, क्योंकि वे केवल अपनी छवि के निर्माण और बचाव में लगे रहते हैं, जनहित उनके लिए एक साधन मात्र होता है।
हमें यह समझना होगा कि आत्ममुग्धता का इलाज आत्म-निरीक्षण और विनम्रता से ही संभव है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह पूर्ण नहीं है, कि उसके अलावा भी कई लोग हैं जिनके विचार, अनुभव और योगदान मूल्यवान हैं, तभी वह एक परिपक्व मनुष्य बन पाता है।
सच्चा नेतृत्व और महानता वहीं पनपती है जहां अपने साथ-साथ दूसरों की भी कद्र हो। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने न केवल स्वयं कुछ हासिल किया, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित किया, रास्ता दिखाया, उनका गुणगान किया। जैसे गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन-आंदोलन बनाया, नेहरू ने युवा भारत को वैज्ञानिक दृष्टि दी, और अंबेडकर ने शोषितों को न्याय दिलाया, इनमें आत्मविश्वास था, पर आत्ममुग्धता नहीं।
समाज का सौंदर्य विविधता, सहयोग और आपसी सम्मान में है। यदि हम एक स्वस्थ, सशक्त और सहानुभूतिपूर्ण समाज चाहते हैं, तो आत्ममुग्धता को तिलांजलि देना होगी। दूसरों की उपलब्धियों का उत्सव मनाइए, उनके विचारों को सम्मान दीजिए, और अपने भीतर उस विनम्रता को स्थान दीजिए जो मनुष्य को बड़ा बनाती है।
सच कहिए तो आत्ममुग्धता कोई आकर्षक गुण नहीं, बल्कि एक आत्मघाती कमजोरी है। यह न केवल व्यक्ति को अकेला और असंतुलित बनाती है, बल्कि समाज को भी बाँझ कर देती है, जहां प्रेरणा, सहयोग और करुणा जैसी भावनाएं दम तोड़ने लगती हैं। अतः हमें आत्ममुग्धता से मुक्त होकर आत्मचिंतन, परस्पर संवाद और विनम्रता की ओर बढ़ना होगा, ताकि हम न केवल स्वयं के लिए, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकें। यही मनुष्य की सच्ची सुंदरता और समाज की वास्तविक शक्ति है।