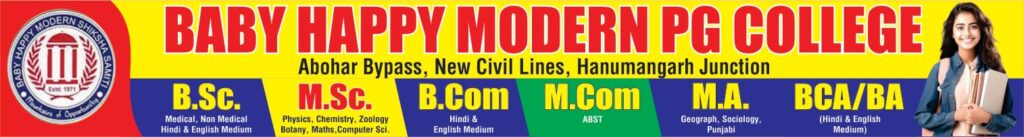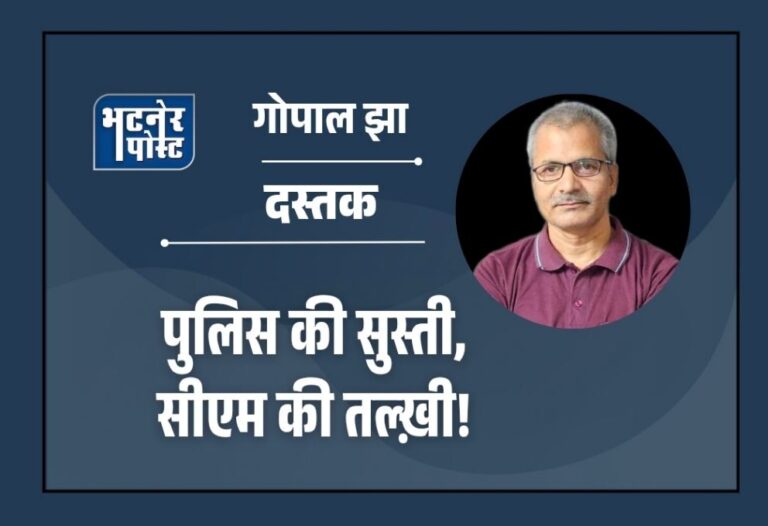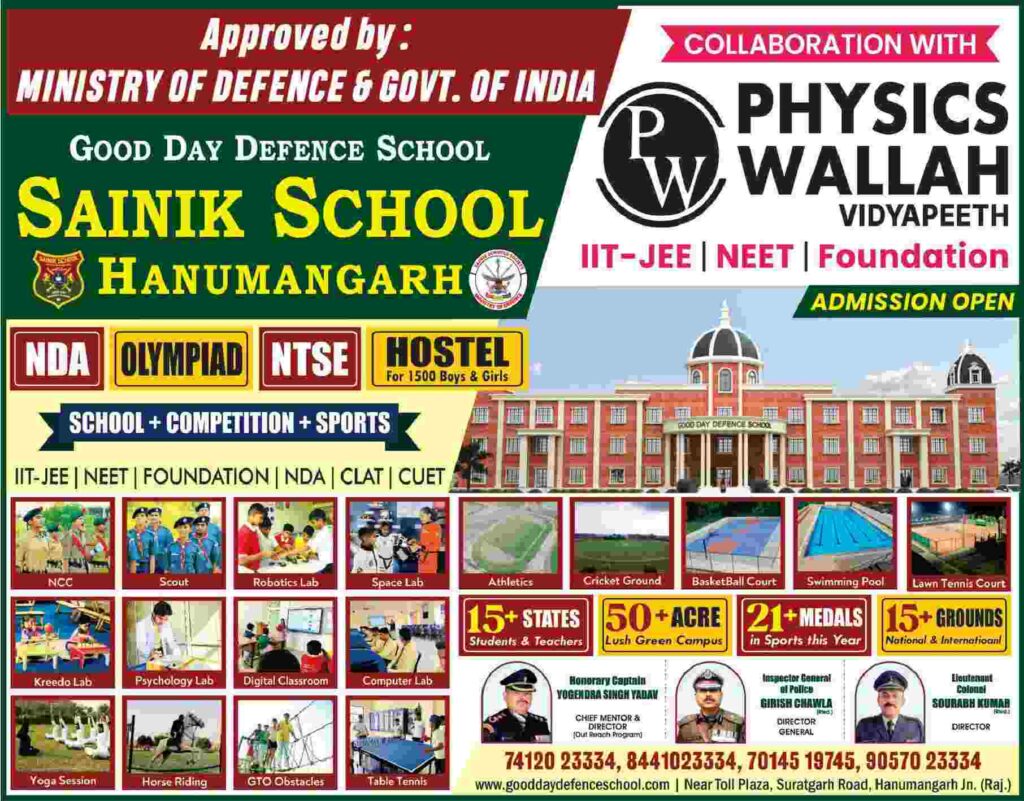

गोपाल झा.
देश को आजाद हुए 78 साल बीत गए। तिरंगे पर सलामी देने वाले हाथों में अब स्मार्टफोन है, और परचम के नीचे खड़े चेहरों पर गर्व के साथ-साथ गहरी बेपरवाही भी। अंग्रेज़ तो बहुत पहले चले गए, पर उनकी छोड़ी हुई सोच की बेड़ियाँ अब भी हमारे दिमाग पर ताले लगाए बैठी हैं। हम आज भी नेता की जाति, पार्टी की विचारधारा और भीड़ के नारे में अपनी राय डुबो देते हैं। सच पूछिए तो हमने लोकतंत्र को मतपेटी में कैद कर दिया है, जहाँ वोट है, पर विवेक नहीं; आज़ादी है, पर सवाल करने की हिम्मत नहीं। यह वही ‘मानसिक गुलामी’ है जो राष्ट्रगान के बीच भी कान में फुसफुसाती है, ‘चुप रहो, भीड़ के साथ चलो, वरना देशद्रोही कहलाओगे।’ सवाल सिर्फ इतना है, इस अदृश्य जंजीर को तोड़ेगा कौन? कोई मसीहा, या हम खुद?

जिस आज़ादी के लिए भगतसिंह फाँसी पर झूले, गांधी ने सत्याग्रह किया, नेताजी ने आज़ाद हिन्द फौज बनाई, वह आज़ादी क्या केवल सत्ता हस्तांतरण थी? क्या आज़ादी का अर्थ मात्र अंग्रेज़ों के जाने भर से पूर्ण हो गया था? शायद नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता केवल भौगोलिक नहीं होती। स्वतंत्रता का मर्म मानसिक, वैचारिक और आत्मिक विमुक्ति में छिपा होता है। और अफ़सोस, इस मोर्चे पर हम आज भी पराजित से हैं।

आज हम तकनीक में तरक्की कर रहे हैं, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहे हैं, विश्वमंचों पर अपने भाषणों से ‘वाहवाही’ बटोर रहे हैं, पर क्या हम अपने ही सोच के दायरे से बाहर निकल पाए? नहीं। क्योंकि हम आज भी ‘नेता की जाति’, ‘पार्टी की विचारधारा’, और ‘भीड़ की राय’ को अपनी सोच से ऊपर मानते हैं। हमारी वोट की ताक़त, जो लोकतंत्र की रीढ़ है, वह आज भी भावनाओं, जातियों और झूठे वादों की गिरफ़्त में है। हमने आज़ादी को वोट देने के अधिकार तक सीमित कर दिया है, पर सोचने के अधिकार का उपयोग करना आज भी बहुतों के लिए पराया है। ये कैसी आज़ादी है, जहाँ सवाल पूछने वाला ‘देशद्रोही’ कहलाता है, और चुपचाप सहने वाला ‘देशभक्त’?

दरअसल, हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन उनकी बनाई ‘मानसिक जेल’ में अब भी बंद हैं। पहले हम ‘सरकार बहादुर’ के सामने झुकते थे, अब हम ‘साहब’ और ‘नेता जी’ के चरणों में लोटते हैं। पहले हुकूमत हमारे नाम पर शासन करती थी, अब हम स्वयं सत्ता को अपना भाग्यविधाता मान बैठे हैं। यह ‘मानसिक गुलामी’ का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो और क्या है?
हमारे भीतर एक ‘पिछलग्गूपन’ घर कर गया है। हम सोचने से डरते हैं, अलग चलने से घबराते हैं, क्योंकि हमने ‘भीड़ के साथ होना ही सुरक्षित होना’ मान लिया है। और यहीं से हमारी बौद्धिक आज़ादी की पराजय शुरू होती है। ध्यान रहे, लोकतंत्र की नींव स्वतंत्र चेतना पर टिकी होती है। जब नागरिक प्रश्न करना बंद कर दें, जब वह सत्ता से संवाद नहीं, केवल अनुसरण करे, उसकी ‘हां में हां’ मिलाए तो वह लोकतंत्र नहीं, एक दिखावा मात्र रह जाता है।
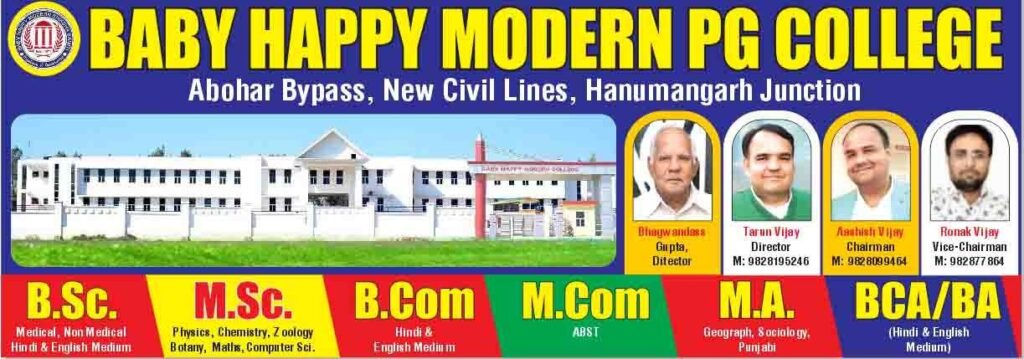
हमें यह स्वीकारना होगा कि कोई भी राजनीतिक दल दुश्मन नहीं हैं, वह एक व्यवस्था हैं। लेकिन हर व्यवस्था को विवेक की कसौटी पर कसना आवश्यक होता है। जब हम केवल पार्टी के झंडे देखकर मतदान करते हैं, तब हम अपने विवेक का अपमान करते हैं। तब हम एक मतदाता नहीं, एक मूक कठपुतली बन जाते हैं, जिसे कोई भी रंग पहनाकर मंच पर नचा सकता है।
इसलिए आवश्यक है कि इस स्वाधीनता दिवस पर हम सिर्फ झंडा न लहराएँ, बल्कि अपनी सोच को भी ऊँचाई दें। हम अपने भीतर बैठे गुलाम को पहचानें, और उससे विद्रोह करें।

सच्ची आज़ादी तब ही होगी जब हम विचारों के स्वतंत्र हो सकेंगे, जब वोट डालने से पहले विवेक जागेगा, जब हम दल नहीं, चरित्र को देखेंगे, जब हम चाटुकारिता नहीं, ईमानदार आलोचना करेंगे, और जब हम सत्ता के सम्मोहन से बाहर आकर, संविधान के प्रहरी बनेंगे। याद रखें, हर बार तिरंगे को सलाम करना ही देशभक्ति नहीं होती। कभी-कभी अपनी आत्मा से सवाल करना भी राष्ट्रसेवा होती है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर हैं