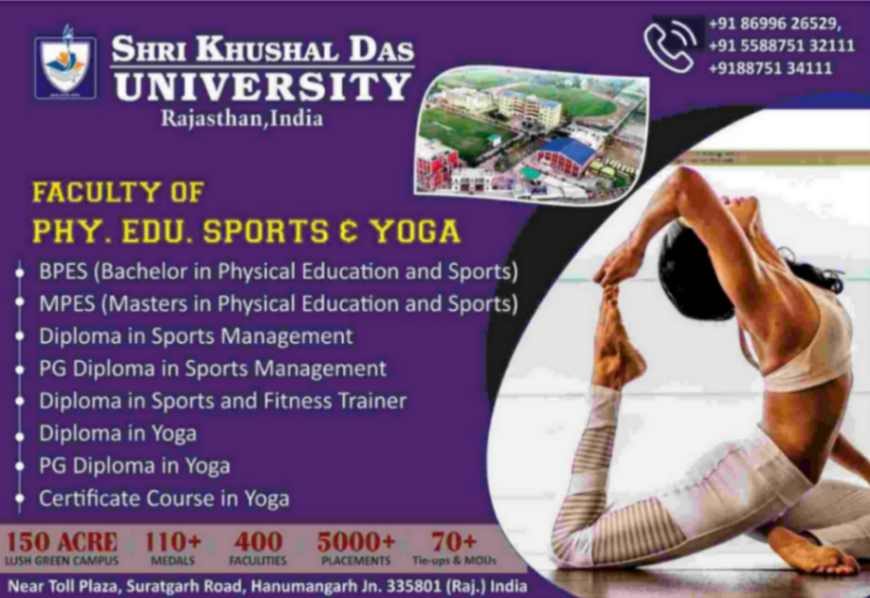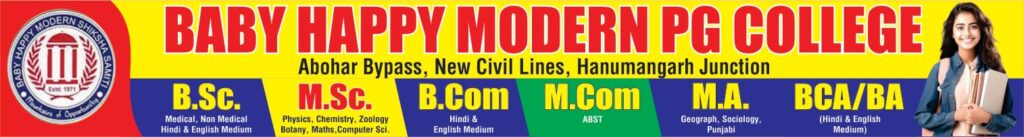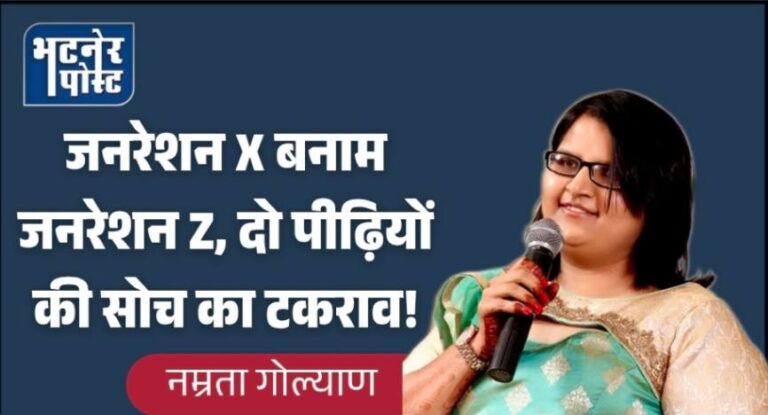डॉ. एमपी शर्मा.
मनुष्य के जन्म के साथ ही एक सत्य उसके साथ चल पड़ता है, मृत्यु। यह न किसी राजा को छोड़ती है, न किसी संत को, न धनवान को, न निर्धन को। फिर भी विडंबना यह है कि मनुष्य ऐसा जीवन जीता है मानो उसे इस संसार में स्थायी पट्टा मिल गया हो। यही भूल, यही विस्मृति, धीरे-धीरे मोह को जन्म देती है। और मोह से निकलते हैं वे कर्म, जो व्यक्ति को ही नहीं, पूरे समाज को विकृत कर देते हैं, अन्याय, शोषण, लालच, घृणा और विभाजन।

आध्यात्मिक दृष्टि हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। सामाजिक चेतना कहती है कि इसलिए हर क्षण उत्तरदायी बनो। इन दोनों का संगम ही सच्चा जीवन मार्ग है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, तब वह अपने कर्मों के प्रति सजग होता है। वह जानता है कि हर निर्णय, हर व्यवहार, किसी न किसी रूप में उसकी पहचान बनेगा।

आध्यात्मिक बोध का मूल प्रश्न यही है, मैं क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊँगा? भीतर झांकने पर उत्तर साफ मिलता है। न हम कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाएँगे। शरीर भी उधार का है, सांस भी उधार की है। फिर इतनी होड़ किस बात की? इतना संग्रह किसलिए? यह प्रश्न मनुष्य को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे विवेक देता है। आध्यात्मिक चिंतन संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार को सही दृष्टि से जीने की समझ देता है।

अक्सर मोह के त्याग को परिवार, संबंध और जिम्मेदारियों के त्याग से जोड़ दिया जाता है। यह एक बड़ी भूल है। मोह का त्याग मतलब अपनों से दूर जाना नहीं, बल्कि स्वार्थ से ऊपर उठना है। परिवार के साथ रहते हुए भी स्वार्थहीन होना संभव है। जिम्मेदारियाँ निभाते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। यही संतुलन मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है।

जब आध्यात्मिक संतुलन नहीं होता, तब समाज में विकृतियाँ बढ़ने लगती हैं। पद के लिए सिद्धांत छोड़े जाते हैं, धन के लिए ईमान बेचा जाता है। जाति, वर्ग और भाषा के नाम पर दीवारें खड़ी की जाती हैं। शक्ति की दौड़ में संवेदनशीलता खो जाती है। मनुष्य भूल जाता है कि मृत्यु के बाद उसकी पहचान उसके बैंक खाते से नहीं, उसके व्यवहार से होगी। समाज का सबसे बड़ा संकट बाहरी अभाव नहीं, बल्कि भीतर का खालीपन है।

मृत्यु का स्मरण डर पैदा करने के लिए नहीं है। यह जीवन को सही दिशा देने का साधन है। जब हमें याद रहता है कि समय सीमित है, तब हम उसे व्यर्थ नहीं गंवाते। अवसर सीमित हैं, इसलिए सेवा का महत्व बढ़ जाता है। संबंध सीमित समय के हैं, इसलिए उन्हें प्रेम और सम्मान से निभाने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है, वह जीवन को हल्के में नहीं लेता। वह उसे एक पवित्र जिम्मेदारी मानता है।

सच्ची आध्यात्मिकता पूजा-पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं रहती। वह समाज में उतरती है, व्यवहार बनकर। उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं, कमजोर के प्रति करुणा, व्यवस्था के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, मतभेद के बीच सम्मान और सफलता के साथ विनम्रता। ऐसा व्यक्ति मंदिर भी जाता है और मनुष्य की पीड़ा भी समझता है। वह प्रार्थना भी करता है और प्रयास भी। यही कर्मयोग है, जहाँ चिंतन और कर्म एक-दूसरे से अलग नहीं होते।

यदि मृत्यु निश्चित है, तो जीवन का सही उपयोग क्या है? उत्तर बहुत साधारण है, पर गहरा भी। जितनों को उठा सको, उठाओ। जितनों का दुःख बाँट सको, बाँटो। जितना सत्य बोल सको, बोलो। जितना न्याय कर सको, करो। अंत में मनुष्य अपने कर्मों की छाया में ही विश्राम पाता है। वही उसके साथ चलता है, बाकी सब यहीं रह जाता है।
मृत्यु अंत नहीं है, वह स्मरण है कि समय कम है। मोह बंधन नहीं, एक परीक्षा है कि तुम क्या चुनते हो। आध्यात्मिकता पलायन नहीं, आचरण की शुद्धि है। सामाजिक चेतना कोई नारा नहीं, मनुष्यता का विस्तार है। ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए, तो वह अंत न लगे, बल्कि एक पूर्णता का बोध कराए।
-लेखक पेशे से विख्यात सर्जन व आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं