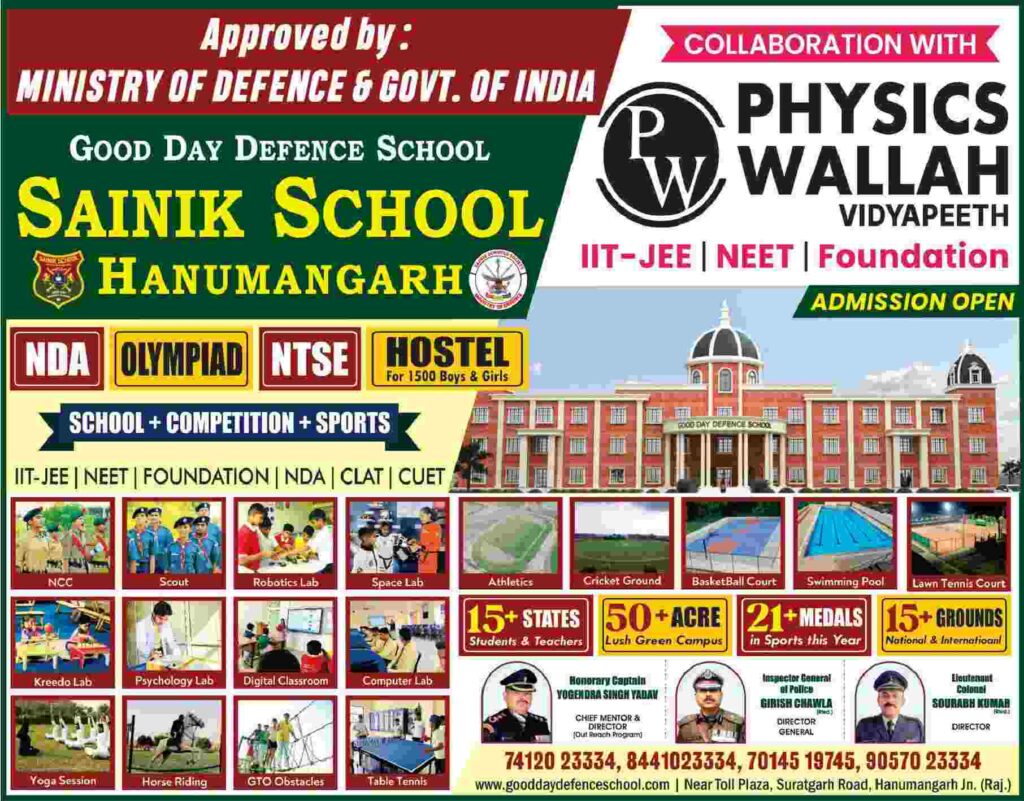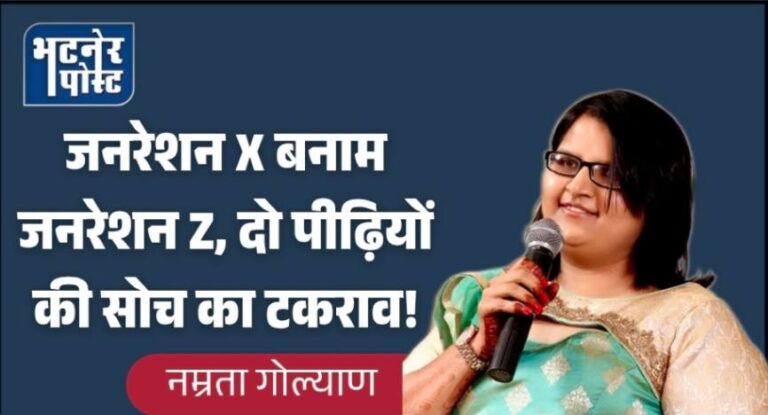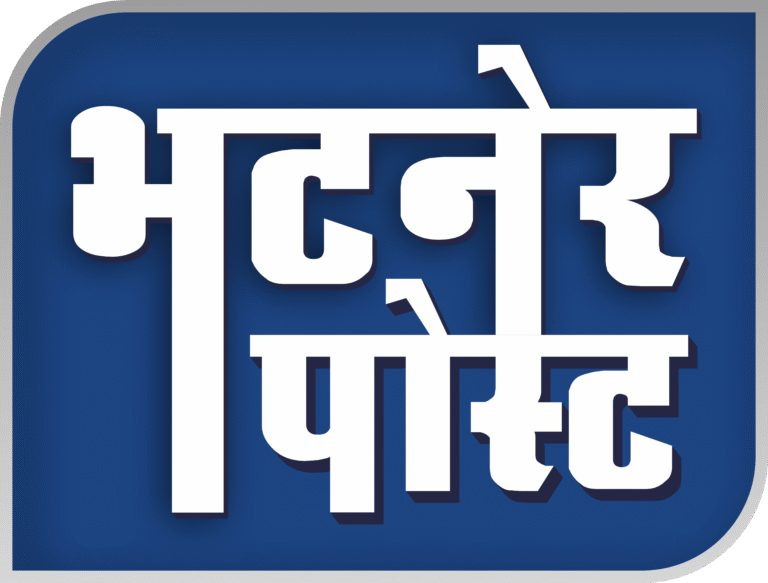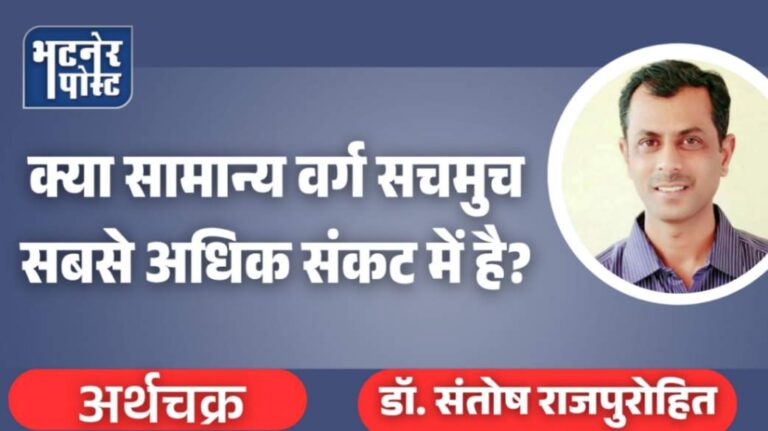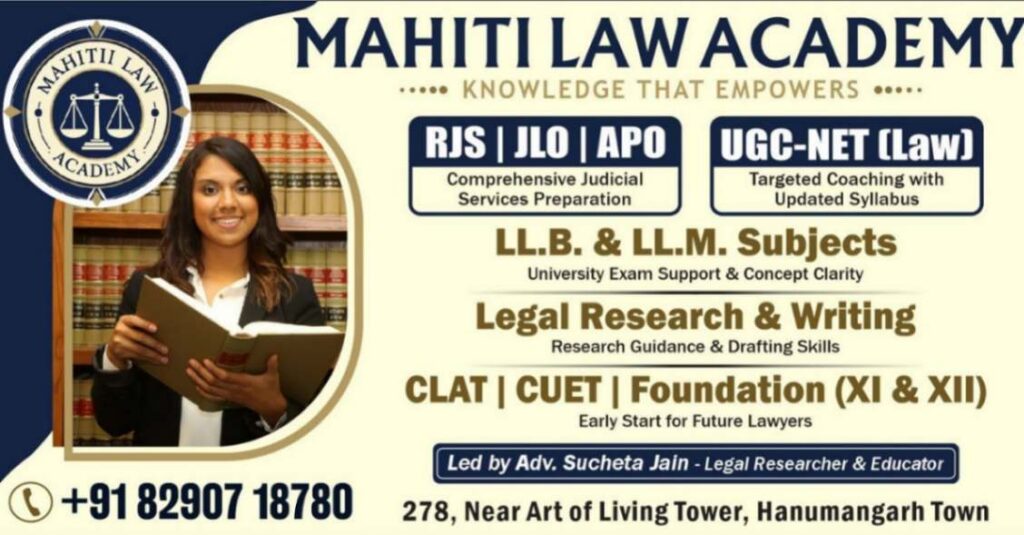

डॉ. एमपी शर्मा.
देश में नशे की समस्या सिर्फ़ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, यह परिवारों की टूटन, कानून-व्यवस्था की जटिलताओं और सामाजिक ताने-बाने पर गहरी चोट है। शराब और तंबाकू को छोड़ दें तो कैनाबिस, हेरोइन, ओपिओइड, ऑक्सीकोडोन जैसी दवाएँ, इंजेक्टिंग ड्रग्स और सॉल्वेन्ट का प्रयोग नई पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। सरकार और राज्य प्रशासन ने नशामुक्ति के लिए कई योजनाएँ और अभियान चलाए हैं। सवाल है, क्या यह प्रयास उतने ही असरदार हैं, जितनी उनकी घोषणा?
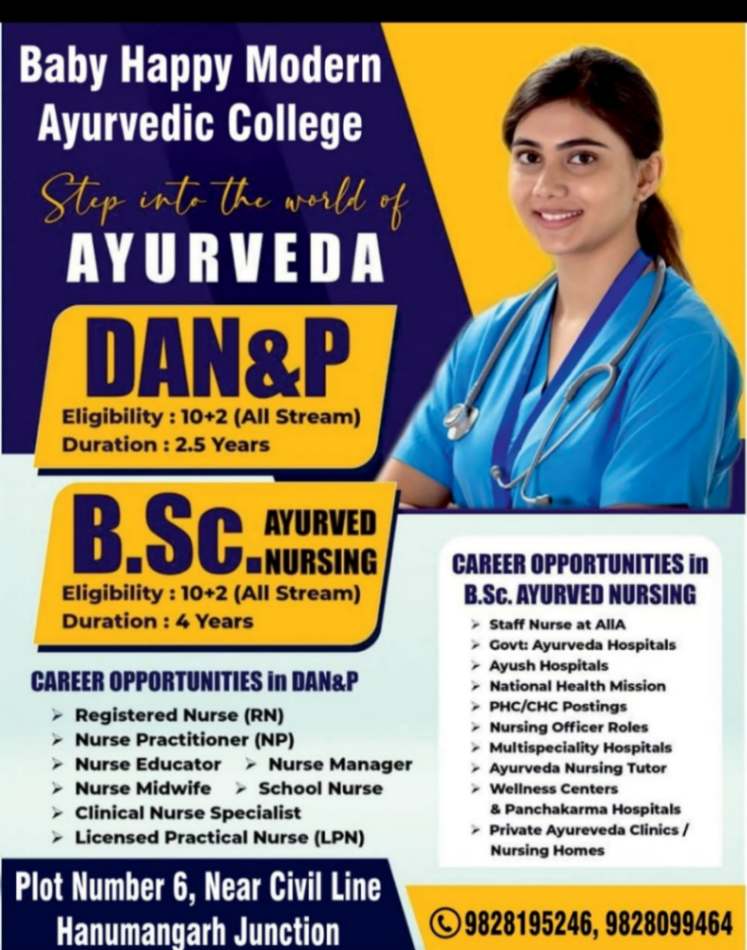
केंद्र सरकार ने रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, क्षमता निर्माण और समुदाय-आधारित गतिविधियों को जोड़कर एक समेकित रूपरेखा बनाई है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फंड और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में डी-एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं। कई राज्यों ने सामाजिक न्याय विभाग और एनजीओ के सहयोग से इनका विस्तार किया है।
राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और रिपोर्टों ने नशे के पैटर्न को सामने रखा। आंकड़े बताते हैं कि डी-एडिक्शन केन्द्रों में इलाज लेने वालों की संख्या 2015-16 में लगभग 1.46 लाख थी, जो 2023-24 तक बढ़कर 5.82 लाख हो गई। यह निश्चय ही एक बड़ा इजाफा है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संख्या नशे के वास्तविक मामलों का बहुत छोटा हिस्सा है। इलाज तक पहुँच और जरूरतमंद आबादी के बीच अभी भी बड़ी खाई है।

नशे की स्थिति राज्यों के बीच एक समान नहीं है। कुछ पूर्वाेत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंजेक्टिंग ड्रग्स का उपयोग बहुत अधिक है। वहीं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में गिनती के डी-एडिक्शन सेंटर ही हैं। नतीजा यह है कि इलाज का कवरेज असमान रहता है और कई प्रभावित जिलों में लोग आज भी उचित सुविधा से वंचित हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि नशे से लड़ाई में परिवार की भूमिका बेहद अहम है। अक्सर परिजन कलंक या सामाजिक डर के कारण रोगी को छिपाते हैं और इलाज में देर करते हैं। पर अध्ययनों में पाया गया है कि पारिवारिक काउंसलिंग और फैमिली थैरेपी से बेहतर नतीजे आते हैं। सरकार की योजनाओं में पारिवारिक सहभागिता का प्रावधान है, मगर व्यवहार में इसकी पकड़ कमज़ोर है।

भारत का एनडीपीएस अधिनियम तस्करी रोकने के लिए कड़ा है। पर आलोचना यह भी है कि इसमें स्वास्थ्य-उन्मुख दृष्टिकोण उतना मजबूत नहीं है। छोटे स्तर के उपभोक्ता कई बार डीलिंग में भी उलझ जाते हैं। यदि उन्हें सिर्फ़ सज़ा मिले और पुनर्वास या रोज़गार का विकल्प न मिले, तो समस्या और गहरी हो जाती है। पुलिस-स्वास्थ्य समन्वय की कमी भी असर घटाती है।
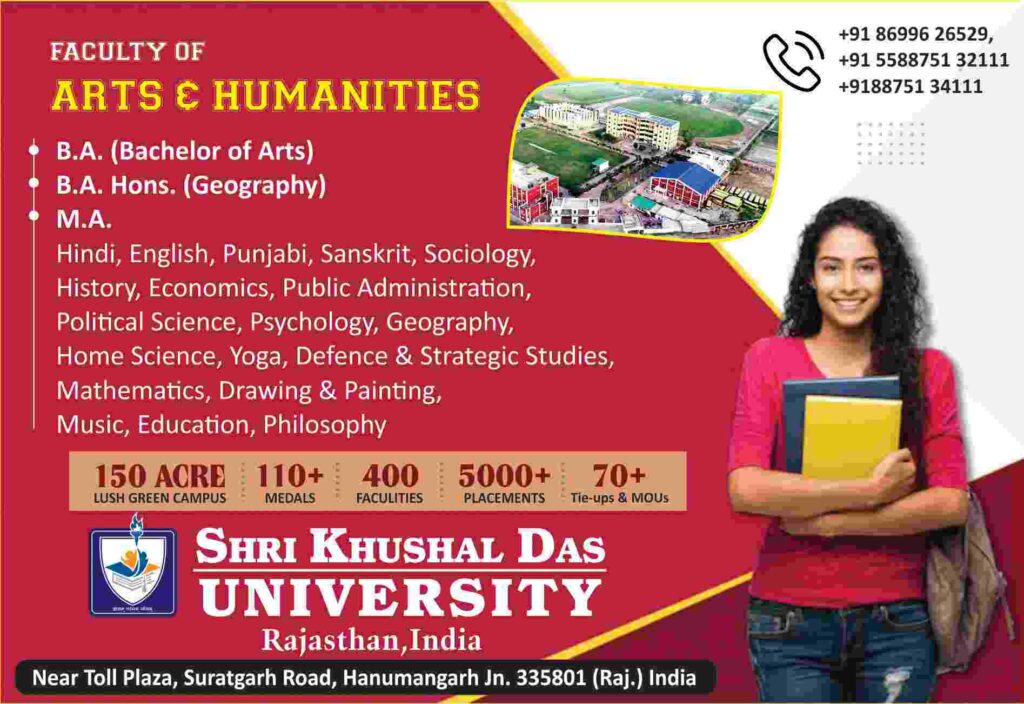
इंजेक्टिंग ड्रग्स से एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ड्रग यूज़र्स में टीबी का जोखिम भी अधिक पाया गया है। हृदय, लीवर और मानसिक रोगों पर असर के प्रमाण भी सामने आए हैं। यानी नशे की समस्या केवल लत की नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का प्रवेशद्वार भी है।

केंद्र और राज्य सरकारों के पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक समेकित, रियल-टाइम, राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी अधूरा है। अगर हर इलाज केंद्र, एनजीओ और दवा-वितरण केंद्र का डेटा तुरंत उपलब्ध हो, तो नीतियों का असर नापना आसान होगा। वर्तमान में आंकड़े बिखरे हुए हैं और अक्सर समय से अपडेट नहीं होते।
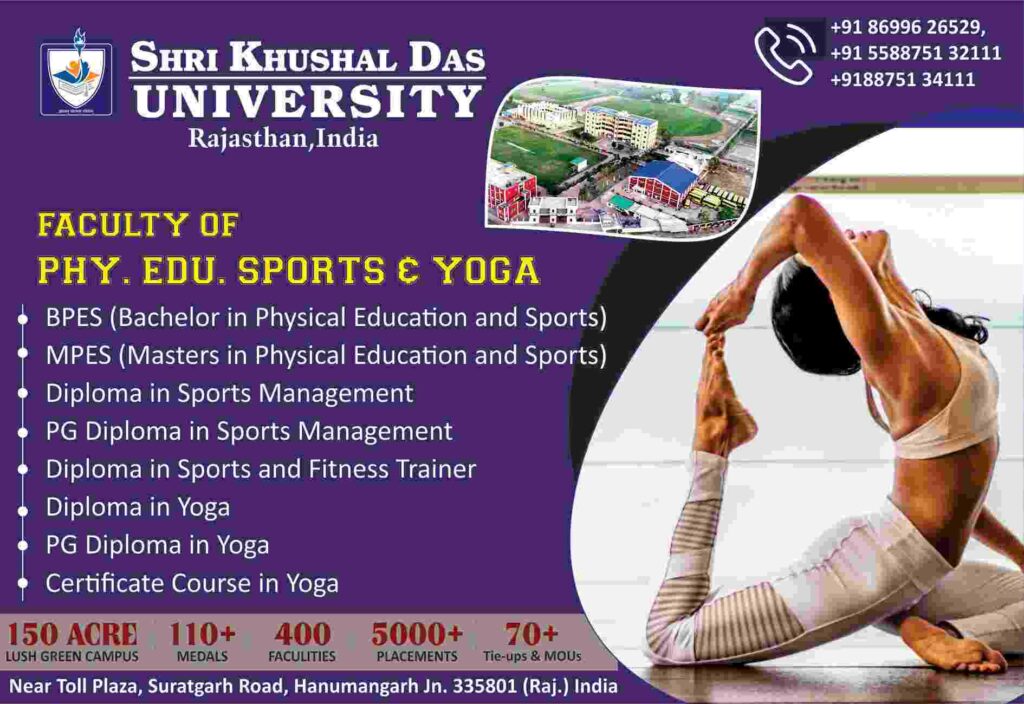
विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ़ घोषणाओं से बात नहीं बनेगी। हर डी-एडिक्शन सेंटर को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना होगा। बुप्रेनोर्फाइन जैसी दवाओं के लिए कड़े प्रोटोकॉल और फार्मेसी-लेवल ट्रैकिंग जरूरी है, ताकि ब्लैक-मार्केट में दवाइयाँ न पहुँचें। स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान, माता-पिता की ट्रेनिंग और फैमिली काउंसलिंग को मज़बूत करना होगा। पुलिस को बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि छोटे उपभोक्ताओं को इलाज तक पहुँचाना प्राथमिकता बननी चाहिए।

सरकारी नशामुक्ति अभियान ने निश्चित रूप से इलाज तक पहुँच को बढ़ाया है और नीति का रुख स्पष्ट किया है। लेकिन राज्यों के बीच असमानता, दवा-निगरानी की चुनौतियाँ और सामाजिक कारण अभी भी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। असली जंग तभी जीती जा सकती है, जब स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर डेटा-आधारित और इंसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएँ।
-लेखक सीनियर सर्जन और आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं