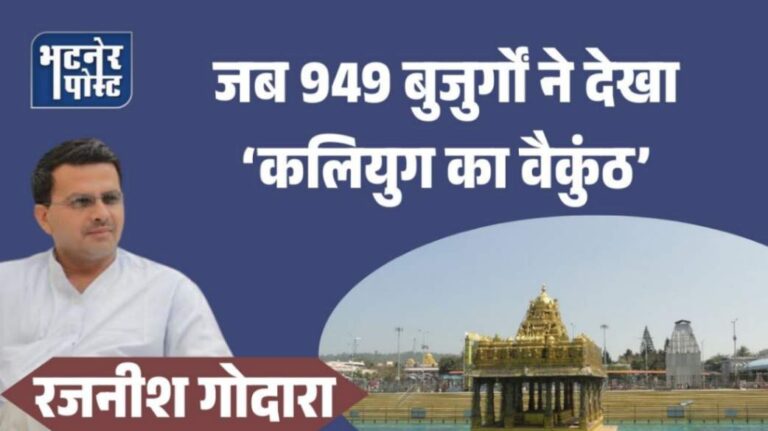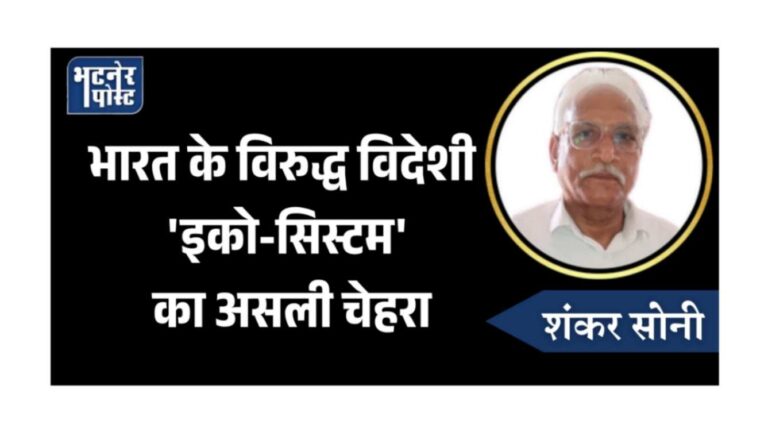एडवोकेट मिताली अग्रवाल.
समाज की वास्तविक प्रगति केवल सड़कों, इमारतों या तकनीक से नहीं मापी जाती; इसका असली पैमाना यह होता है कि उसमें महिलाएँ कितनी सम्मानित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हैं। जब एक महिला निर्भय होकर अपने निर्णय ले सकती है, अपने अधिकारों को जानती है और अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तभी समाज मज़बूत बनता है। आज हम तेज़ी से बदलते समय में जी रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कई सवाल अब भी वहीं खड़े हैं। इन प्रश्नों को नज़रअंदाज़ करना मतलब आने वाली पीढ़ियों से समझौता करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर महिला जागरूक हो, कानून को जाने और समाज अपनी ज़िम्मेदारी निभाए।

हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा से आधारस्तंभ रही है, घर की जिम्मेदारियाँ हों या शिक्षा, नौकरी, राजनीति और सामाजिक नेतृत्व, महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि उन्हें आज भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, दहेज के नाम पर उत्पीड़न, कार्यस्थल पर शोषण, सड़क से लेकर इंटरनेट तक असुरक्षा, ये चुनौतियाँ आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। बहुत-सी महिलाएँ परिस्थितियों से घिरी हुई चुप रह जाती हैं, जबकि चुप्पी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती; कई बार वही चुप्पी अपराधियों का हौसला बन जाती है।

कानून हर महिला को सुरक्षा और अधिकार देता है, पर कानून तब ही कारगर होता है जब उसे जाना जाए और समय पर उपयोग किया जाए। भारतीय विधिक प्रणाली ने महिलाओं के हित में कई सख्त प्रावधान बनाए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इस बात को स्वीकार करता है कि हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं होती, बल्कि मानसिक, आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक शोषण भी उतना ही गंभीर अपराध है। यह कानून पीड़ित महिला को सुरक्षा, निवास का अधिकार, आर्थिक सहायता और संरक्षण आदेश दिलाने की सुविधा देता है।

इसी तरह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 ने कामकाजी महिलाओं के लिए बेहद मजबूत ढांचा तैयार किया है। इस कानून के तहत हर संस्था, सरकारी हो या निजी, आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है, ताकि महिलाएँ सुरक्षित वातावरण में बिना डर काम कर सकें।

तकनीक के तेज़ विस्तार के साथ साइबर अपराधों का बढ़ना भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। मॉर्फिंग, फर्जी प्रोफाइल, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकी, अशोभनीय संदेश, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दंडनीय अपराध हैं। ऐसे मामलों में महिलाएँ तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकती हैं। शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज होती है, जिससे अपराधी तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है।

हिंसा का असर केवल शारीरिक नहीं होता। मानसिक क्षति कई बार शरीर पर दिखने वाले घावों से भी ज्यादा गहरी होती है। आत्मविश्वास टूटना, लगातार भय में जीना, सामाजिक रूप से अलगाव। ये परिणाम किसी भी महिला की प्रगति को रोक सकते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना, काउंसिलिंग लेना, और अपने आसपास के भरोसेमंद लोगों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एक परिवार तब ही स्वस्थ माना जाता है, जब उसमें बेटियाँ और बहुएँ सम्मान, बराबरी और भरोसा महसूस करें। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं को अवसर देना ही पर्याप्त नहीं; उन्हें सुरक्षित माहौल देना भी उतना ही आवश्यक है। यही माहौल आगे चलकर आत्मनिर्भर और जागरूक महिलाओं की पीढ़ी तैयार करता है।

महिलाओं की सहायता के लिए सरकार ने अनेक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं, 181 महिला हेल्पलाइन, 1091 पुलिस सहायता, 112 आपातकालीन सेवा और 1098 बच्चों के लिए चाइल्डलाइन। इन सेवाओं का उद्देश्य यही है कि पीड़ित महिला को सहायता पाने में एक पल भी देरी न हो। हर वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना केवल एक महिला का नहीं, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है।
आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हर महिला अपने अधिकारों को जाने, परिस्थिति के सामने झुकने के बजाय खड़ी हो, सुरक्षा के प्रति सचेत रहे और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में संकोच न करे। जब महिलाएँ जागरूक होंगी, तभी वे सशक्त बनेंगी, और जब महिलाएँ सशक्त होंगी तभी समाज सही मायनों में प्रगतिशील कहलाएगा।
-लेखिका सशक्त नारी फ़ाउंडेशन की संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ता हैं