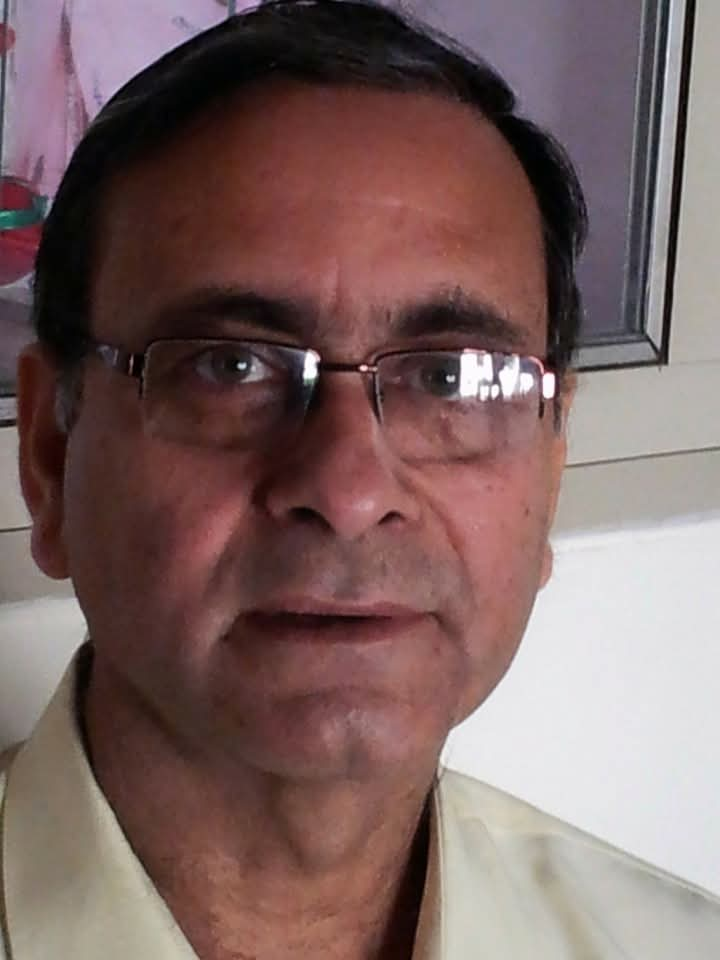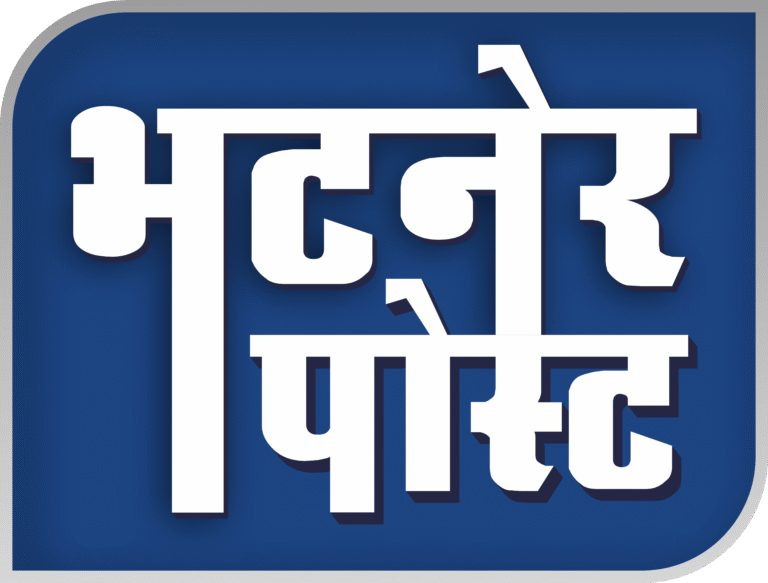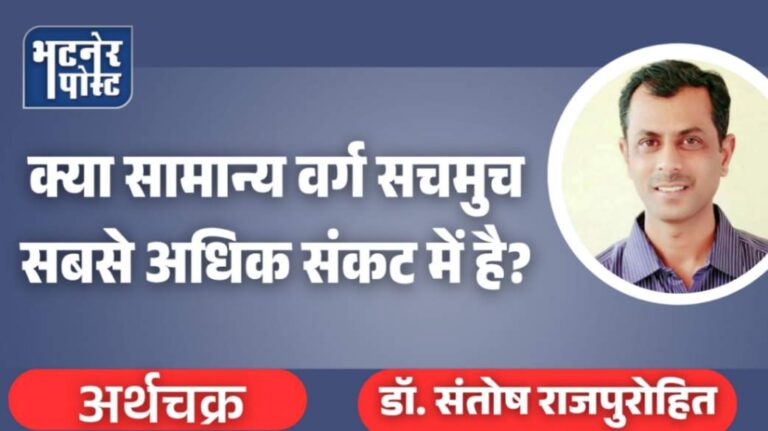डॉ. एमपी शर्मा.
एक दौर था जब गाँव में झोले वाले डॉक्टर से लेकर शहर के विशेषज्ञ चिकित्सक तक को लोग ‘भगवान का दूसरा रूप’ मानते थे। मरीज आंख मूंदकर इलाज कराता, डॉक्टर तन्मयता से इलाज करता और यह रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता था। लेकिन आज तकनीक, इलाज और दवाइयों की सुविधा बढ़ने के बावजूद, डॉक्टर और मरीज के इस रिश्ते की डोर जैसे कमजोर होती जा रही है। आए दिन अस्पतालों में हिंसा, सोशल मीडिया पर ट्रायल, डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर, ये घटनाएं इस डोर के टूटने की पीड़ा को दर्शाती हैं। यह सवाल अब बार-बार उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला जिसने इस रिश्ते की गरिमा को झकझोर कर रख दिया?
डॉक्टर और मरीज़ के संबंधों में दरार की शुरुआत कई कारणों से हुई। सबसे पहली वजह है, संवादहीनता। एक ओर डॉक्टर बढ़ते केस लोड, सीमित संसाधनों और प्रशासनिक दबावों में उलझा रहता है, दूसरी ओर मरीज़ अपने कष्ट, डर और भ्रम से घिरा होता है। जब डॉक्टर को मरीज़ के साथ बमुश्किल 2-3 मिनट ही मिलते हैं, तो मरीज़ को लगता है कि उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। वहीं डॉक्टर के लिए यह रोजमर्रा की व्यस्तता का हिस्सा बन चुका है।
दूसरी वजह है सोशल मीडिया और इंटरनेट की आधी-अधूरी जानकारी, जिससे मरीज़ भ्रमित हो जाता है और चिकित्सक के फैसले पर तुरंत सवाल उठाता है। हर मरीज़ ‘गूगल डॉक्टर’ से लैस होकर आता है, और अगर डॉक्टर का परामर्श इससे मेल न खाए तो शक और अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है। सरकारी योजनाओं की जटिलता भी भ्रम पैदा करती है। मरीज़ सोचता है कि आयुष्मान या सरकारी योजना में सब मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन जब वास्तविक प्रक्रियाएं सामने आती हैं, तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे गुमराह कर रहे हैं।

डॉक्टर की भी अपनी पीड़ा है
एक चिकित्सक के रूप में मैं जानता हूं कि डॉक्टर की दुनिया बाहर से जितनी सम्मानजनक दिखती है, भीतर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। मेडिकल शिक्षा के 8-10 साल, फिर रेजिडेंसी की रातें, और इसके बाद हर दिन का 12-16 घंटे का तनावपूर्ण काम, यह सब डॉक्टर की जिंदगी का हिस्सा है। हर बार डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति के आगे जब कुछ नहीं हो पाता, तो दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है। आज का डॉक्टर व्यावसायिकता और सेवा भावना के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद में जी रहा है। हर केस में उसे न सिर्फ इलाज करना है, बल्कि यह भी ध्यान रखना है कि कोई नाराज़ न हो, सोशल मीडिया पर गलत संदेश न चला जाए, और अस्पताल की छवि पर आंच न आए।
मरीज़ भी निराश
मरीज़ की पीड़ा भी कम नहीं है। वह अस्पताल आता है अपनी अंतिम उम्मीद लेकर। लेकिन कई बार उसे ठंडी प्रक्रिया, लंबी कतारें, अप्रत्याशित खर्च और डॉक्टर से जुड़ाव की कमी मिलती है। उसे लगता है कि डॉक्टर मशीनों, रिपोर्ट्स और पैसों में उलझ गया है। यह भावना विश्वास को धीरे-धीरे खत्म कर देती है।
क्या है समाधान ?
इस अविश्वास को खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है संवाद का पुल बनाना। डॉक्टर को यदि हर मरीज़ के साथ सिर्फ 5 मिनट अतिरिक्त मिलें, तो न केवल उसका विश्वास बढ़ेगा, बल्कि गलतफहमियों की गुंजाइश भी घटेगी। वहीं मरीज़ को भी समझना होगा कि डॉक्टर भी इंसान है, वह देवता नहीं, जिसकी हर कोशिश सौ प्रतिशत सफल हो। मेडिकल शिक्षा में ‘कम्युनिकेशन स्किल’ को अनिवार्य करना, डॉक्टरों को मरीज से भावनात्मक जुड़ाव की कला सिखाना और अस्पतालों में ‘पेशेंट रिलेशन डेस्क’ जैसी व्यवस्थाएं इस दिशा में कारगर साबित हो सकती हैं।
समाज की जिम्मेदारी
आईएमए जैसी संस्थाएं डॉक्टरों के लिए संवाद और सहानुभूति आधारित कार्यशालाएं आयोजित करती हैं। सरकार को चाहिए कि वह डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए सख्त और लागू होने योग्य कानून बनाए, ताकि कोई हिंसा या अभद्रता की सोच भी न सके। मीडिया को भी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी। किसी घटना को ब्रेकिंग न्यूज बनाने से पहले तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। अन्यथा यह समाज में और भ्रम फैलाता है।
डॉक्टर और मरीज: एक-दूसरे के पूरक
डॉक्टर और मरीज़ एक-दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर के बिना मरीज़ की राहत अधूरी है और मरीज़ के बिना डॉक्टर का उद्देश्य अधूरा। यह रिश्ता सहानुभूति, धैर्य और पारस्परिक सम्मान से ही मजबूत होगा। आज ज़रूरत है उस दौर को लौटाने की जब डॉक्टर का हाथ थामकर मरीज़ कहता था, ‘डॉक्टर साहब, आप हैं तो हम ठीक हो जाएंगे’ और डॉक्टर पूरे मन से कहता था, ‘चिंता मत करो, हम हैं ना।’ इस रिश्ते को फिर से वही गरिमा और विश्वास दिलाना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।
-लेखक सीनियर सर्जन और आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं