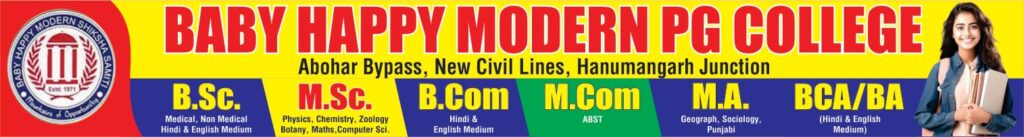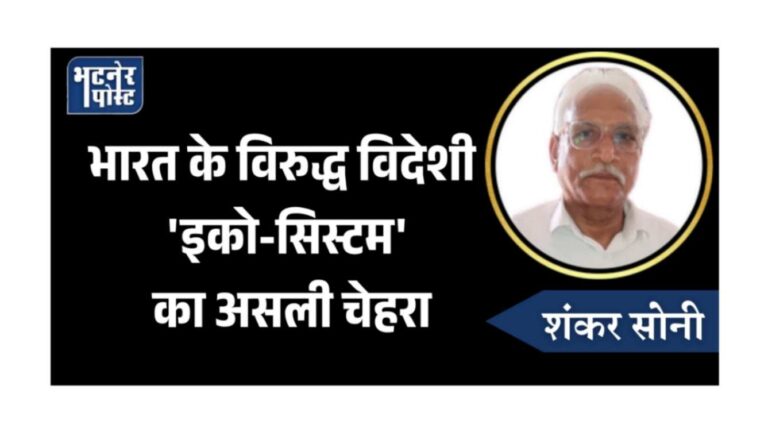हरजिंद्र सिंह सैनी.
सुबह छह बजे का अलार्म, गूगल से हर सवाल का जवाब, दो मिनट में नूडल्स वाला नाश्ता, एक कमांड पर संगीत, वीडियो और जानकारी और एक क्लिक पर पूरी दुनिया की खरीदारी। यह है आज की जिन्दगी। तेज, चमकदार और पूरी तरह तकनीक में डूबी हुई। जेब में बाजार है, हाथ में मोबाइल है और आंखों के सामने स्क्रीन। सुविधाएं बेशुमार हैं, विकल्प अनगिनत हैं, पर इसी चमक के पीछे एक गहरी छाया भी फैल रही है।
टेक्नोलॉजी से घिरे इस समाज में कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं, लेकिन इनमें सबसे नाजुक और सबसे तेज तर्रार है जेन जी। वह पीढ़ी जिसका जन्म ही स्क्रीन, इंटरनेट और बाजार के बीच हुआ है। इस पीढ़ी को न इंतजार करना पड़ा, न लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। खाना, कपड़ा, शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान। सब कुछ एक क्लिक पर, वो भी असीमित विकल्पों के साथ। समय और श्रम बचा, लेकिन उस बचे हुए समय को भी इन्होंने फिर से उसी स्क्रीन में डाल दिया। यहीं से शुरू होती है असली त्रासदी, अकेलापन और सामाजिकता का क्षरण।

बदलती जीवनशैली, सरकारी नीतियां, बढ़ते खर्च और करियर की दौड़ ने परिवारों को छोटा कर दिया। एक या दो बच्चों तक सिमटी दुनिया। संयुक्त परिवार लगभग इतिहास बनने को हैं। बुआ, मौसी, मामा, ताया जैसे रिश्ते अब किताबों के शब्द लगने लगे हैं। बच्चों के लिए परिवार का मतलब सिर्फ मम्मी-पापा रह गया है।

ऊपर से ओवर-केयरिंग। स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, एक्टिविटी क्लास, बच्चा टाइमटेबल में कैद है। खेल, मस्ती, बेफिक्री, सब शेड्यूल में बंध गए हैं। जिस उम्र में बच्चा गलियों में धूल उड़ाता था, उस उम्र में वह स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा है।
कभी इस अकेलेपन की भरपाई संयुक्त परिवार करते थे। चाचा-चाची, ताया-ताई, मौसी-मौसा, मामा-मामी, इन रिश्तों की गर्माहट बच्चे को समाज से जोड़ती थी। अब जब यह ढांचा ढह रहा है, तो समाज के पास एक ही रास्ता बचता है, पड़ोस को परिवार बनाना।
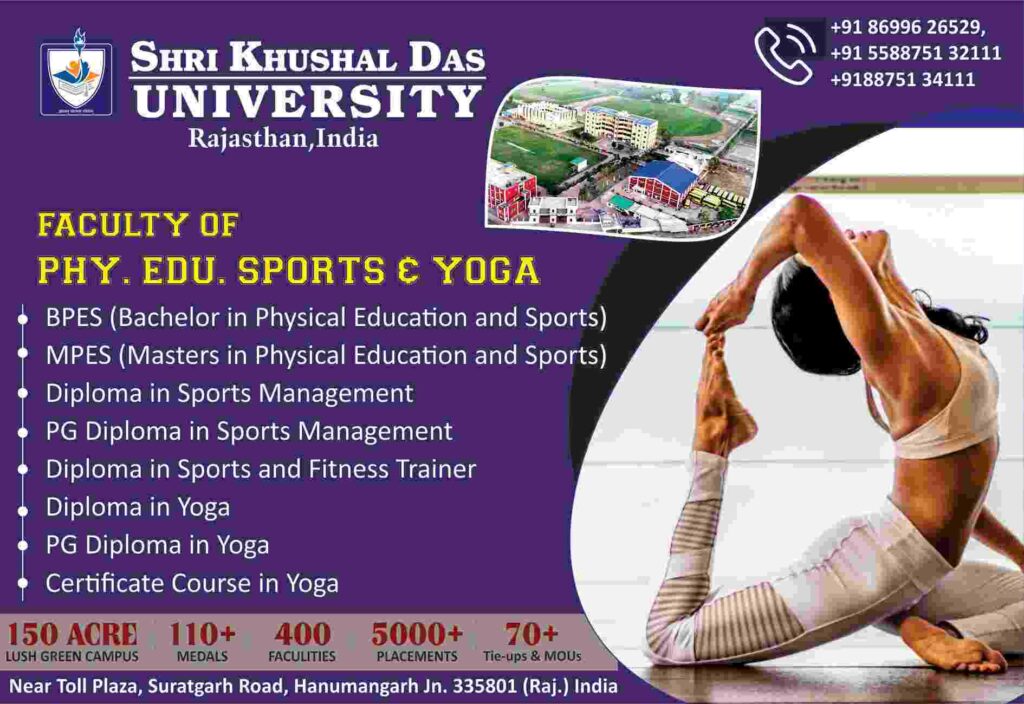
परिवार वह जगह है जहां रिश्ते औपचारिक नहीं होते, जहां अधिकार होता है, अपनापन होता है। वहां अंकल-आंटी नहीं, ताया-ताई, चाची-मौसी होती हैं। वहीं भांजे-भतीजों की किलकारी गूंजती है। वहीं बच्चा बेधड़क डांट भी खाता है और दुलार भी।
महानगरों की सोसायटी संस्कृति अब छोटे शहरों तक पहुंच रही है। फ्लैट के दरवाजे बंद हैं, दिल और ज्यादा बंद। बच्चे बालकनी में अकेले खेल रहे हैं। बाल मनोविज्ञान साफ कहता है, बच्चे को कई अनौपचारिक रिश्तों की जरूरत होती है। अलग-अलग स्वभाव, अलग-अलग लहजे, अलग-अलग प्यार। यही बच्चे को इंसान बनाते हैं। अगर हमने अब भी पड़ोस की संस्कृति को नहीं जगाया, तो यह पीढ़ी रिश्तों की मिठास से वंचित रह जाएगी। दोस्ती औपचारिक होगी, व्यवहार नीरस होगा और भावनाएं सूखी।
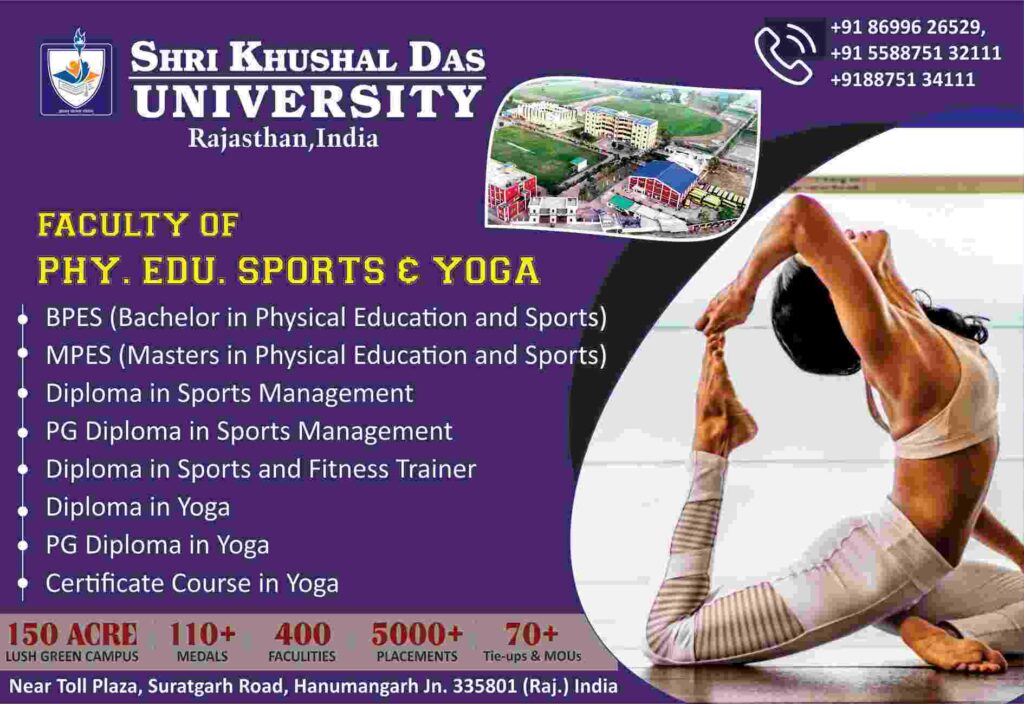
तो आइए, फिर से पड़ोस को जिंदा करें। आंगन खोलें। दरवाजे खोलें। बच्चों को बेफिक्र खेलने दें। चाची-मौसी के रिश्ते लौटाएं। भांजे-भतीजों की शरारतें फिर से गूंजने दें। क्योंकि स्क्रीन सब कुछ दे सकती है, लेकिन गोद, गली और गले लगाना सिर्फ इंसान ही दे सकता है। बचपन जिंदाबाद।
-लेखक सामाजिक चिंतक और अध्यापक हैं