


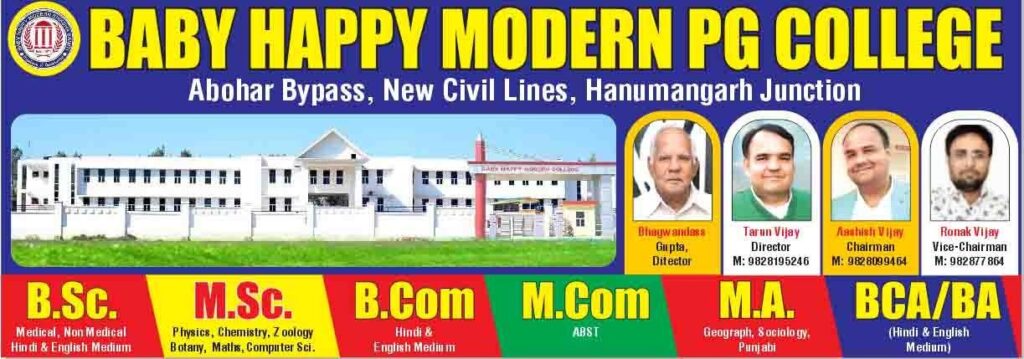

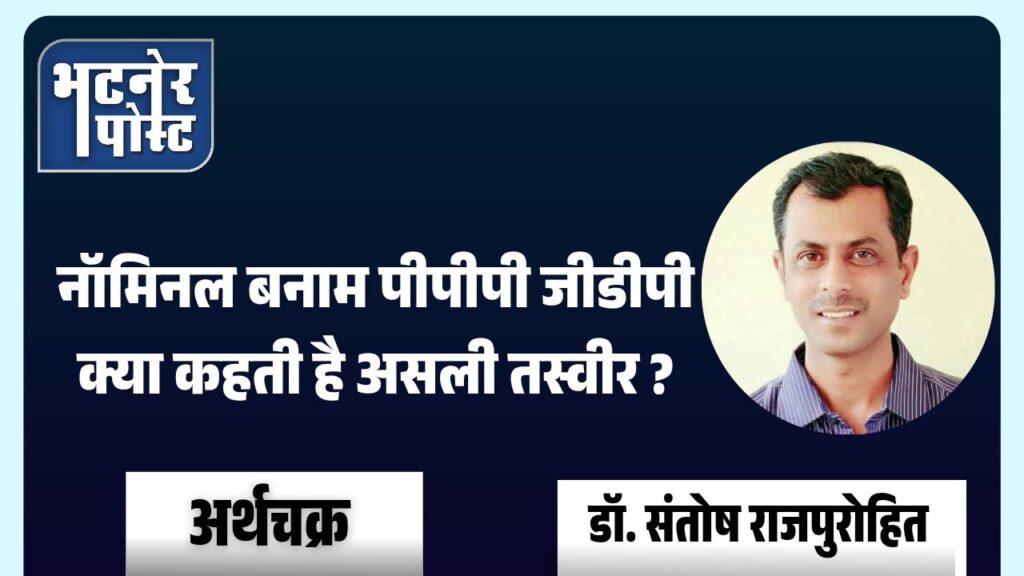
डॉ. संतोष राजपुरोहित.
भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह वाक्य पिछले कुछ वर्षों में न केवल नीति मंचों पर बार-बार गूंजा, बल्कि राजनीतिक भाषणों और मीडिया रिपोर्टों का स्थायी हिस्सा बन गया। नवंबर 2023 में जब भारत ने अस्थायी रूप से 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को छुआ, तो इसे एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह उपलब्धि वास्तव में आर्थिक मजबूती की सूचक है या फिर यह केवल मुद्रा विनिमय दर और आँकड़ों की बाज़ीगरी का नतीजा?
यह आलेख इसी पृष्ठभूमि में भारत की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है, नाममात्र जीडीपी और पीपीपी के फर्क से लेकर विकास की असमानता, समावेशिता और जनता तक लाभ पहुंचाने की वास्तविकता तक। आखिर हम महाशक्ति बनने की दौड़ में हैं, लेकिन क्या सबको साथ लेकर?
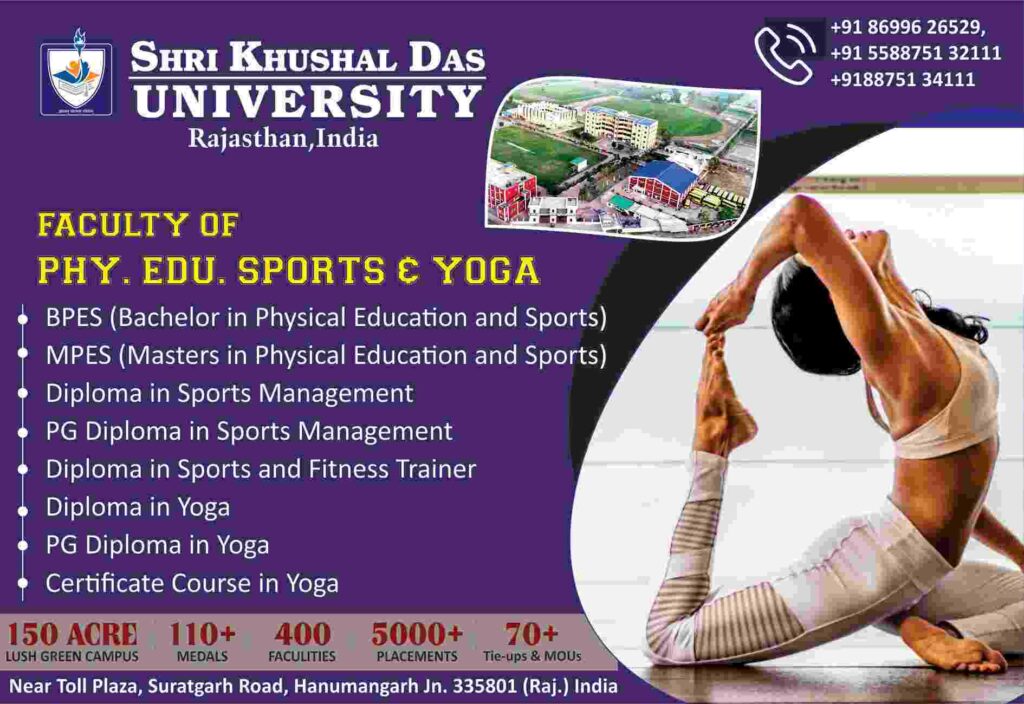
दरअसल, किसी देश की अर्थव्यवस्था को डॉलर के रूप में आंकने के पीछे दो मुख्य तरीके होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और क्रय शक्ति समता। भारत की नॉमिनल जीटीपी को डॉलर में परिवर्तित करने के लिए हमें रुपया-डॉलर विनिमय दर को देखना पड़ता है, जो समय के साथ बदलती रहती है। ऐसे में यह संभव है कि वास्तविक घरेलू उत्पादन में ज्यादा वृद्धि न होते हुए भी अगर डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा मज़बूत हो जाए, तो नॉमिनल जीडीपी डॉलर में अधिक दिखने लगती है।
भारत ने नवंबर 2023 में अस्थायी रूप से 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को छुआ ज़रूर था, लेकिन यह आँकड़ा स्थिर नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी वर्ष 2024 के लिए लगभग 3.7-3.8 ट्रिलियन डॉलर आँकी है। यानी भारत अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की स्थायी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, बल्कि यह एक अस्थायी सीमा रेखा भर थी।
जहाँ तक पीपीपी के आधार पर जीडीपी की बात है, भारत काफी समय से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसका आकार लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इसका अर्थ यह है कि भारत में लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, और यहाँ की वस्तुएँ और सेवाएँ अपेक्षाकृत सस्ती हैं। यह वास्तविक घरेलू क्षमता का बेहतर चित्रण करता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती है।
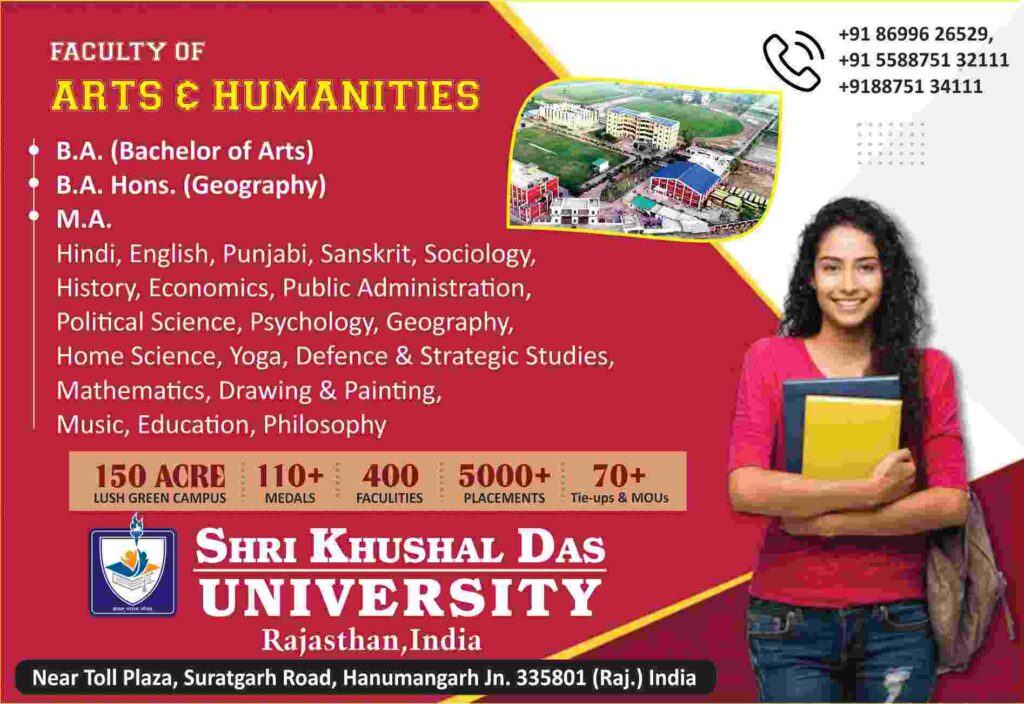
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह प्रचार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है? अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारें जीडीपी आँकड़ों का इस्तेमाल अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए करती हैं। लेकिन जब आम जनता को यह स्पष्ट नहीं बताया जाता कि यह जीडीपी नॉमिनल है और इसमें मुद्रा विनिमय दर की भूमिका अत्यधिक होती है, तो यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। इससे जनता को यह आभास हो सकता है कि अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध हो गई है, जबकि बेरोजगारी, असमानता, ग्रामीण संकट, और मध्यमवर्ग की आय स्थिरता जैसे मुद्दे यथावत बने रहते हैं।
यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, डिजिटलीकरण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार, सेवा क्षेत्र की मजबूती, और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने समग्र अर्थव्यवस्था को गति दी है। भारत लगातार 6-7 फीसद की विकास दर बनाए रखने वाला दुनिया का प्रमुख देश है। इन सबके बावजूद विकास की गुणवत्ता और समावेशिता पर सवाल खड़े होते रहे हैं।
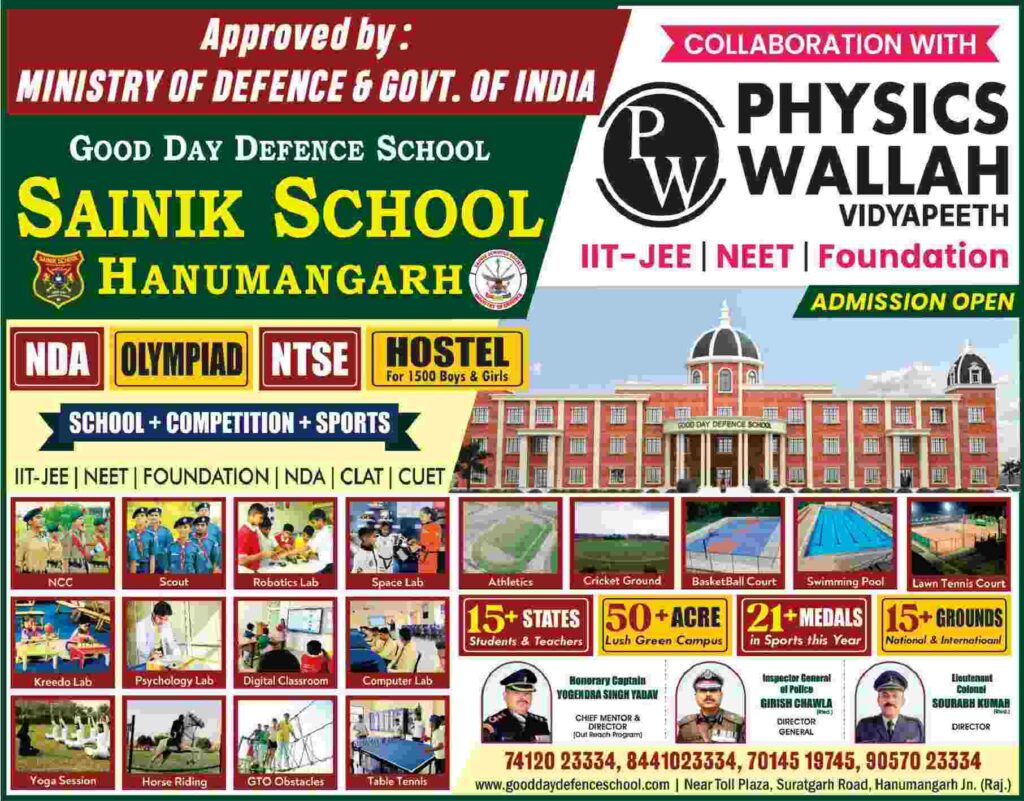
यदि जीडीपी बढ़ भी रही है लेकिन उसका लाभ केवल शीर्ष 10 फीसद जनसंख्या तक सीमित रह जाए, तो यह विकास असमानता को और बढ़ाता है। यही कारण है कि सिर्फ जीडीपी का आँकड़ा विकास का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। हमें मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, और समावेशी रोजगार जैसे कारकों पर भी ध्यान देना होगा।
इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में प्रगति कर रही है, लेकिन जीडीपी के आँकड़े उस प्रगति का आधा चित्र ही दिखाते हैं। न तो हमें इसे पूरी तरह नकारना चाहिए, और न ही सिर्फ इसी के आधार पर गर्व करना चाहिए। देश की आर्थिक वास्तविकता, जमीनी हालात और सामाजिक संतुलन को समझे बिना सिर्फ जीडीपी की ट्रिलियन-दर्शी सोच अधूरी है।
भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह आँकड़ों का एक जटिल खेल भी है, जिसे आमजन को सही परिप्रेक्ष्य में समझाना जरूरी है। आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत अग्रसर है, लेकिन यह यात्रा तभी सार्थक होगी जब विकास समान, समावेशी और स्थायी होगा, केवल आँकड़ों पर आधारित नहीं।
-लेखक भारतीय आर्थिक परिषद के सदस्य हैं













