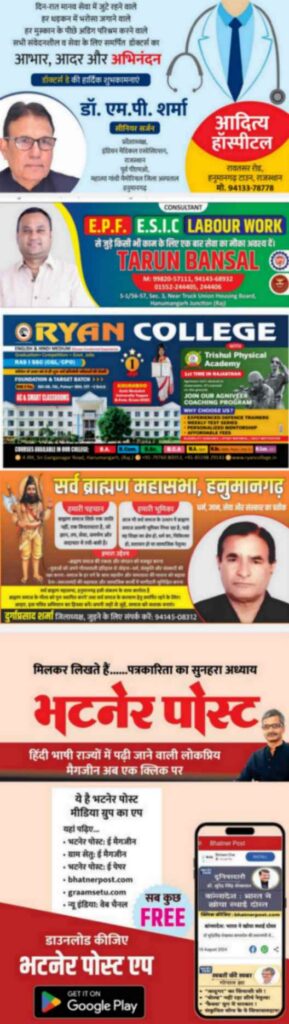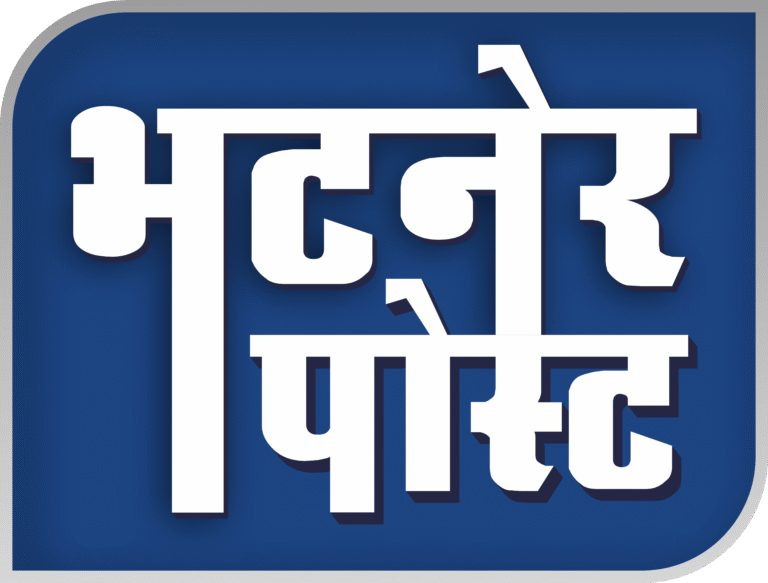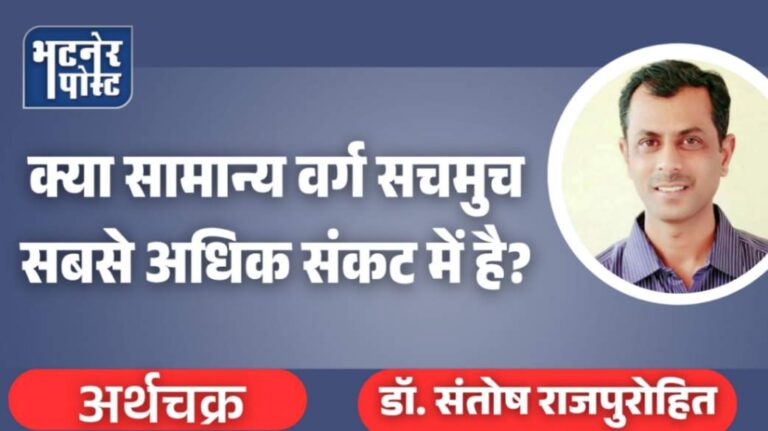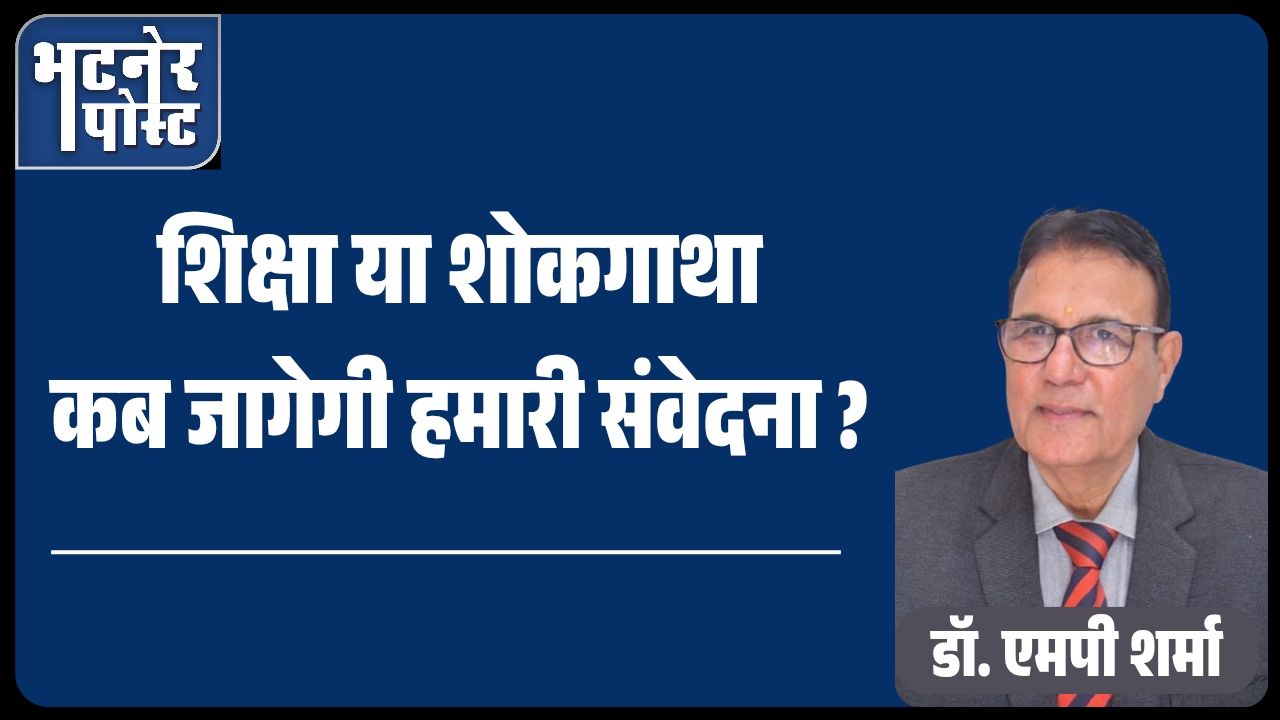
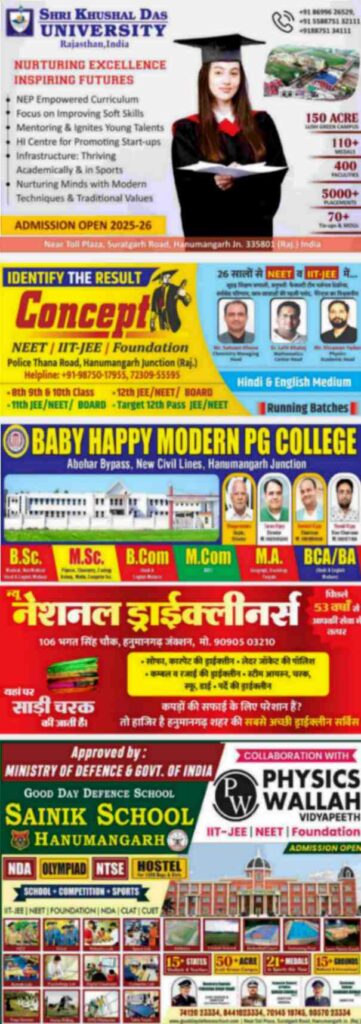
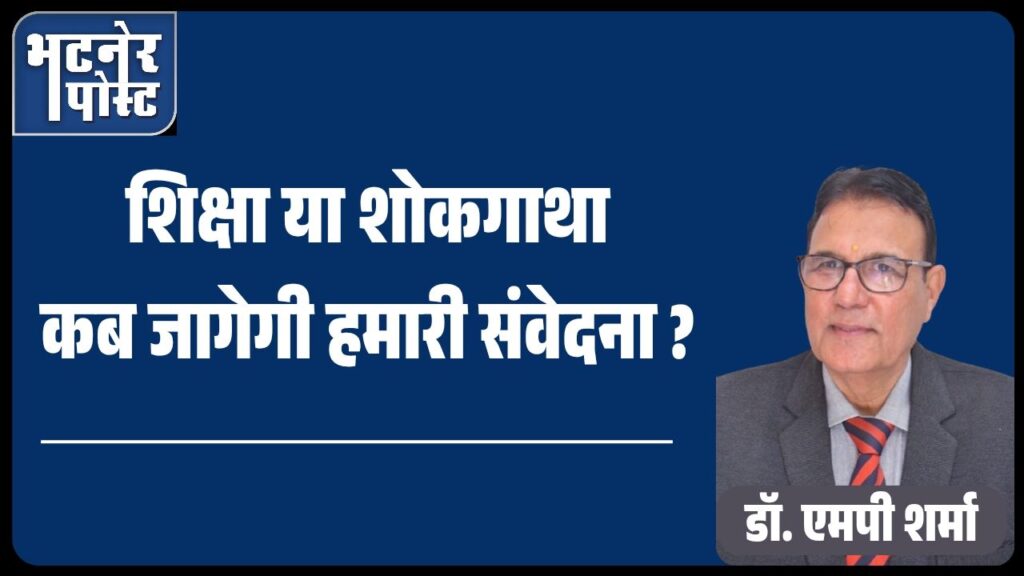
डॉ. एमपी शर्मा.
राजस्थान के झालावाड़ में हाल ही में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई मासूम बच्चों की मौत कोई पहली या आखिरी त्रासदी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था की असंवेदनशीलता, गैर-जवाबदेही और पथराई आंखों पर एक करारा तमाचा है। शिक्षा, जो जीवन निर्माण का माध्यम होनी चाहिए, वह आज जानलेवा बन गई है, कभी ढहती इमारतों के नीचे दबकर, तो कभी अंधी प्रतिस्पर्धा में घुटकर।
इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा अपराधी है, हमारी सामूहिक चुप्पी और ढीली व्यवस्था। नेता केवल चुनावी मौसम में स्कूलों की चौखट पर नजर आते हैं, वादों के ढेर लगते हैं लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं। अधिकारी सरकारी फाइलों में ‘सब ठीक है’ की मोहर लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, जबकि ज़मीनी सच्चाई चीख-चीखकर बदहाल हालात बयां करती है। शिक्षक और स्कूल प्रशासन निरीक्षण और मरम्मत की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था रामभरोसे ही है। कई स्कूल ऐसे हैं, जिनकी इमारतों को 30-40 साल बीत गए लेकिन एक ईंट तक बदली नहीं गई। नतीजा, मासूम जिंदगियां मलबे में दब जाती हैं, माताओं की गोद उजड़ जाती है, फिर भी कोई दोषी नहीं, कोई दंड नहीं। हर बार की तरह ‘मजिस्ट्रियल जांच’ का ढोल पीटा जाता है और मामला दबा दिया जाता है।
क्या यह मात्र हादसा है? नहीं। यह हमारी उदासीनता, हमारी चुप्पी और हमारी खोखली प्राथमिकताओं का परिणाम है। अब वक्त है कुछ ठोस कदमों का, हर विद्यालय की अनिवार्य संरचनात्मक ऑडिट हर पांच साल में हो। स्थानीय निकाय और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त जवाबदेही तय की जाए। विद्यालय विकास समितियों को बजट और निर्णय का अधिकार मिले। लापरवाह अधिकारियों व शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सेवा समाप्ति तक की सजा दी जाए। सरकारी स्कूलों में भी न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। लेकिन अगर हम सोचें कि शिक्षा संकट केवल भवनों की जर्जर स्थिति तक सीमित है, तो यह भ्रम होगा।
देश के कोचिंग हब, कोटा, सूरत, हैदराबाद। हर वर्ष सैकड़ों युवाओं की आत्महत्या के गवाह बनते हैं। वहां शिक्षा नहीं, घुटन मिलती है। लाखों की फीस, 16 घंटे की पढ़ाई, टॉपर्स की ब्रांडिंग और मानसिक स्वास्थ्य की पूरी अनदेखी। यह सब मिलकर छात्रों को अवसाद और आत्महत्या की ओर धकेल रहे हैं। एक बच्चा, जो सपने लेकर आता है, जब खुद को लगातार असफल, अकेला और अयोग्य पाता है, तो वह जीवन से हार मान लेता है।
दोष केवल कोचिंग संस्थानों का नहीं, अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वे अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपते हैं, बिना यह समझे कि बच्चे की अपनी रुचि क्या है। संगीत, कला, खेल, समाज सेवाकृये सब अब भी ‘गैर-विकल्प’ माने जाते हैं। समाज की सोच यह हो गई है कि जो बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बना, वह ‘फेल’ है। स्कूल खुद भी अब केवल मार्कशीट देने वाले केंद्र बन गए हैं, शिक्षा वहां कोचिंग में शिफ्ट हो गई है, भावना रहित और व्यवसायिक।
इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं की पहचान हो। कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और साप्ताहिक काउंसलिंग अनिवार्य हो। टॉपर्स ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगे। सरकार वैकल्पिक करियर विकल्पों को बढ़ावा दे, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, और न ही बनाना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोचिंग रेगुलेशन और छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे पर संज्ञान लिया जाना स्वागतयोग्य कदम है, पर इससे आगे बढ़कर समाज को भी आत्मचिंतन करना होगा। हम कब तक हादसों के बाद आंसू बहाकर भूलते रहेंगे? कब तक बच्चों की मौत को आंकड़ा समझते रहेंगे? आज सवाल यह नहीं कि गलती किसकी है। सवाल यह है कि क्या अब भी देर नहीं हुई है?
समय आ गया है कि नीतियों से पहले संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाए। बच्चों की मुस्कान, उनका जीवन और उनका मानसिक संतुलन किसी भी परीक्षा, टॉप रैंक या सरकारी सिस्टम से बड़ा है। अगर हम वाकई अपने बच्चों को देश का भविष्य मानते हैं, तो उनके वर्तमान को सुरक्षित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वरना शिक्षा का यह मंदिर, कब्रिस्तान में बदलता रहेगा, मौन, अंधा और संवेदनहीन।
-लेखक सीनियर सर्जन और आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं