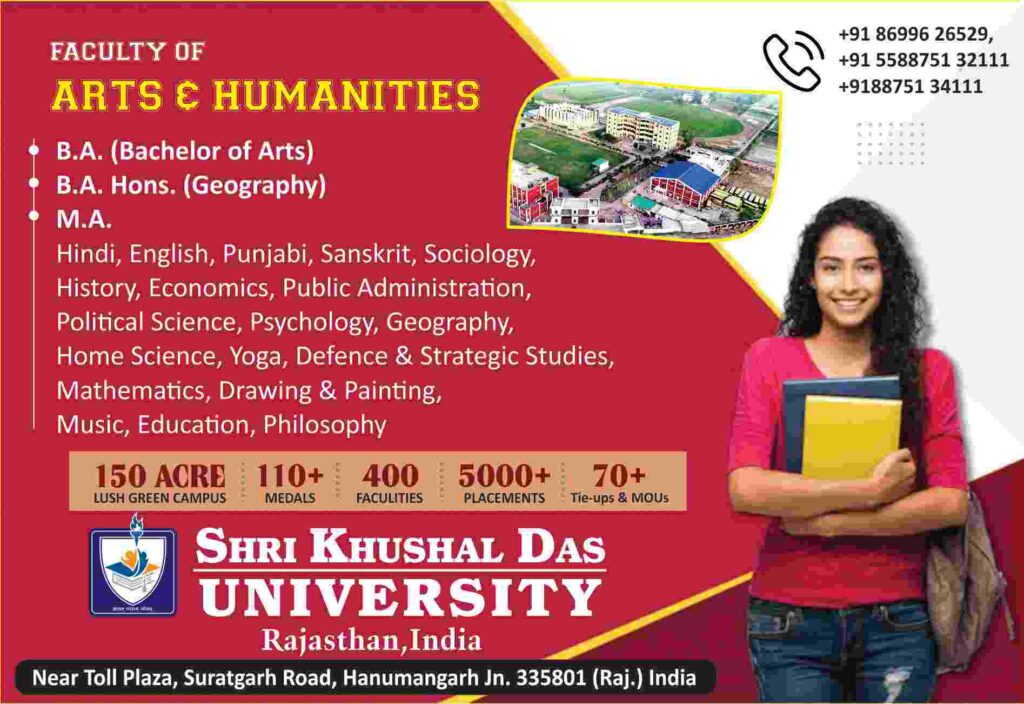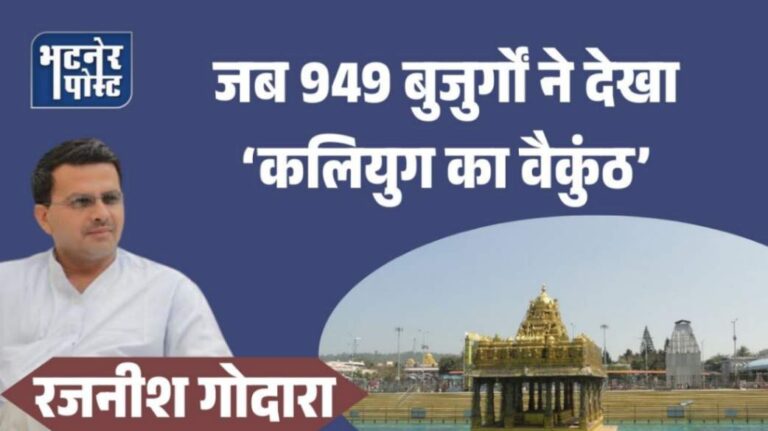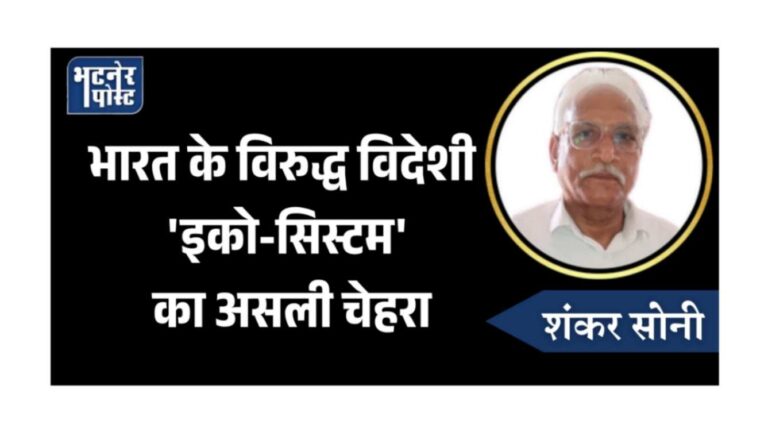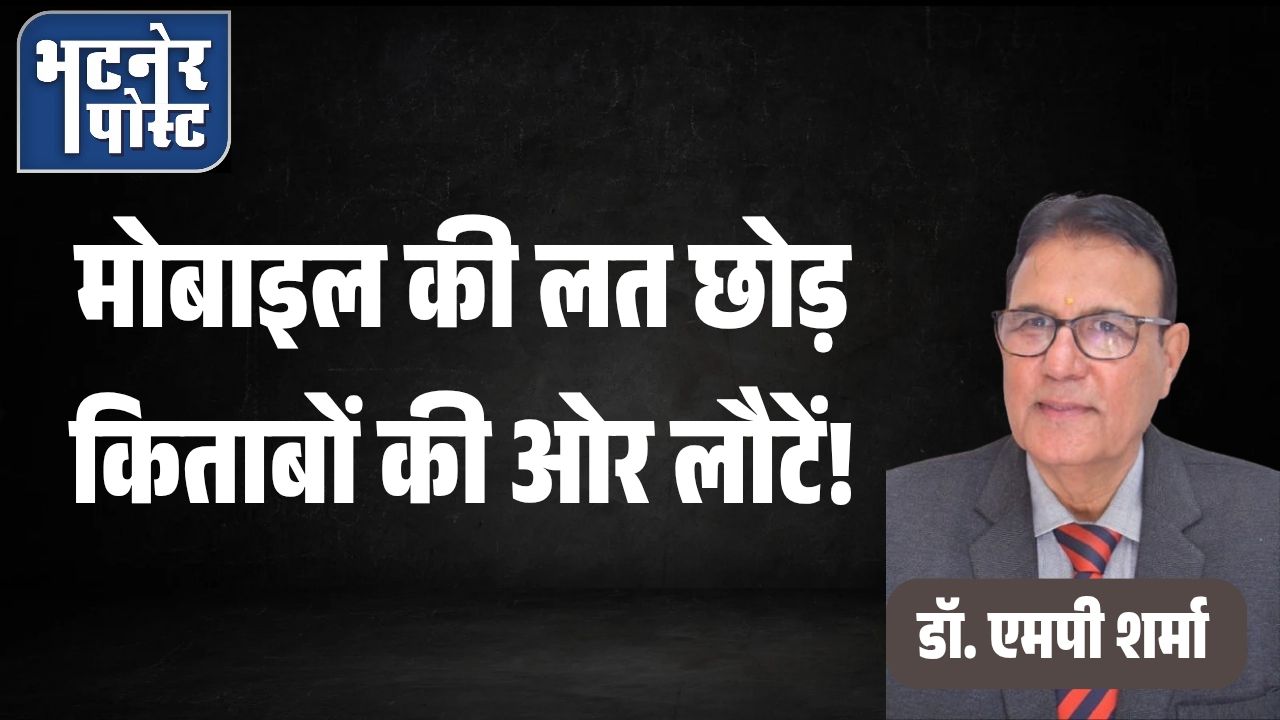

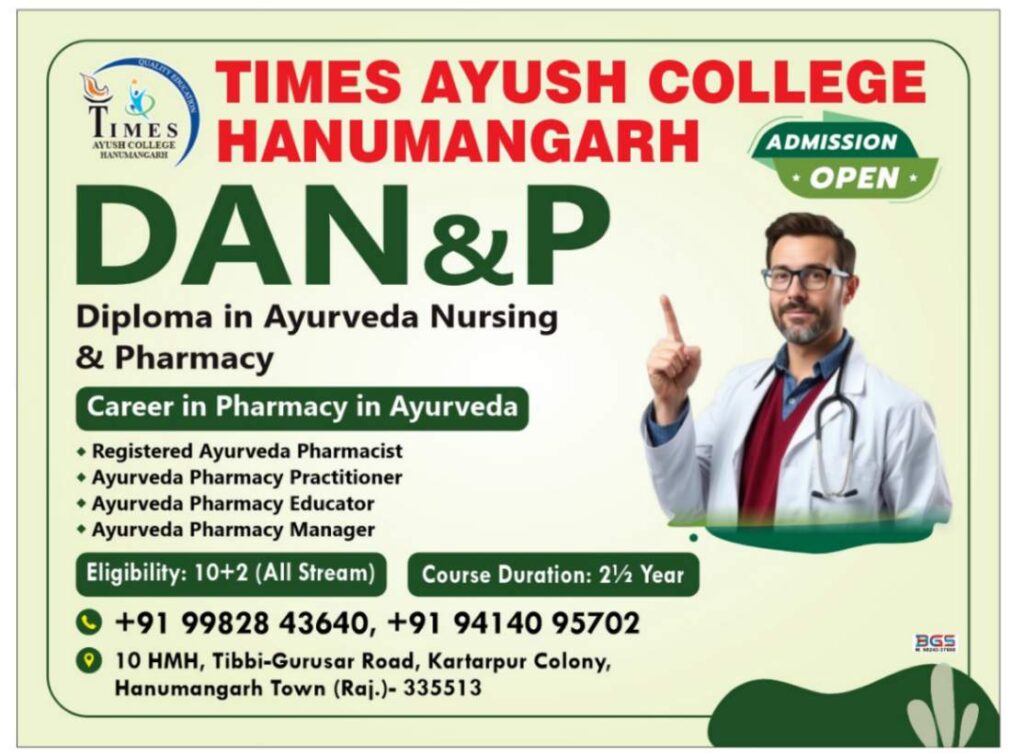


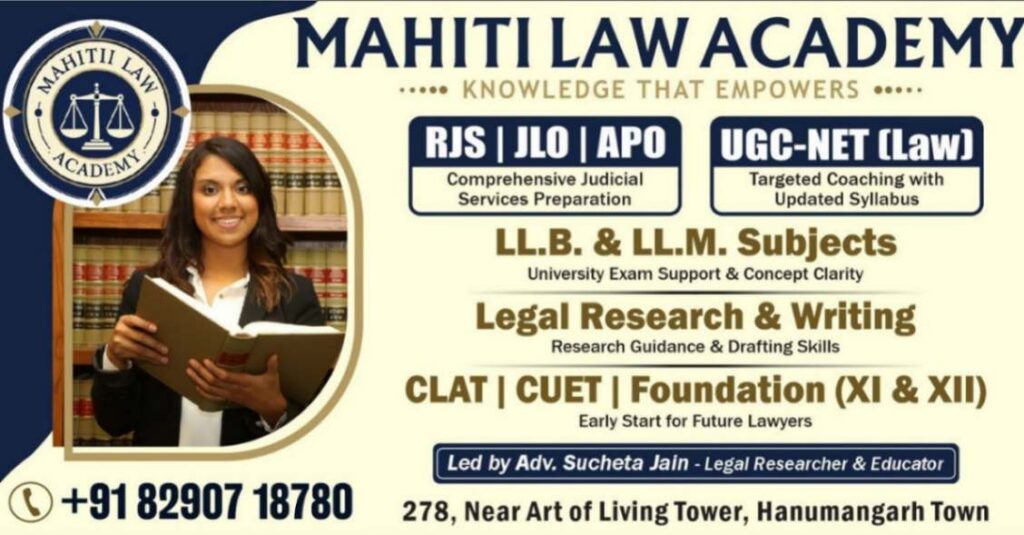

डॉ. एमपी शर्मा.
आज मोबाइल फोन जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल पर नजर डालना और रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन देखना हमारी आदत बन गई है। यह स्थिति केवल बड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चे भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। अक्सर व्यस्तता या सुविधा के कारण माता-पिता छोटे बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं ताकि वे चुप रहें। धीरे-धीरे यह आसान उपाय बच्चों की आदत बन जाता है और वे मोबाइल की रंगीन स्क्रीन में खोने लगते हैं।
बच्चों की दिनचर्या में अब बाहर खेलकूद की जगह मोबाइल गेम्स और कार्टून ने ले ली है। जहां कभी बच्चे पार्क में दौड़ते, साइकिल चलाते और दोस्तों संग मस्ती करते थे, आज वे वर्चुअल दुनिया में उलझे रहते हैं। इसका असर उनकी शारीरिक सेहत, मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार पर सीधा पड़ता है। बाहर खेलने से मिलने वाली ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा और सामूहिकता की भावना मोबाइल स्क्रीन से नहीं मिल सकती।
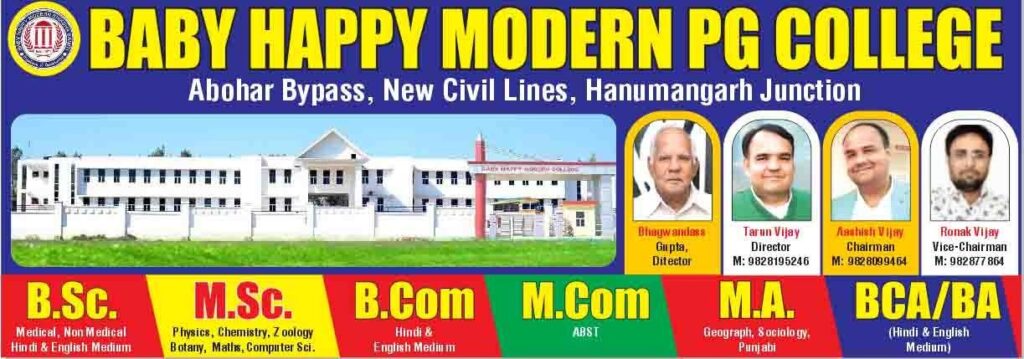
सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी भी मोबाइल पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब ऑनलाइन लेक्चर और ऐप्स पर टिकी है। निश्चित ही तकनीक ने सीखने को सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके दुष्परिणाम भी सामने हैं। किताबों से लगाव लगातार कम हो रहा है। वह कहावत ‘किताबें सच्ची मित्र होती हैं’ धीरे-धीरे केवल कहावत बनकर रह जाएगी।
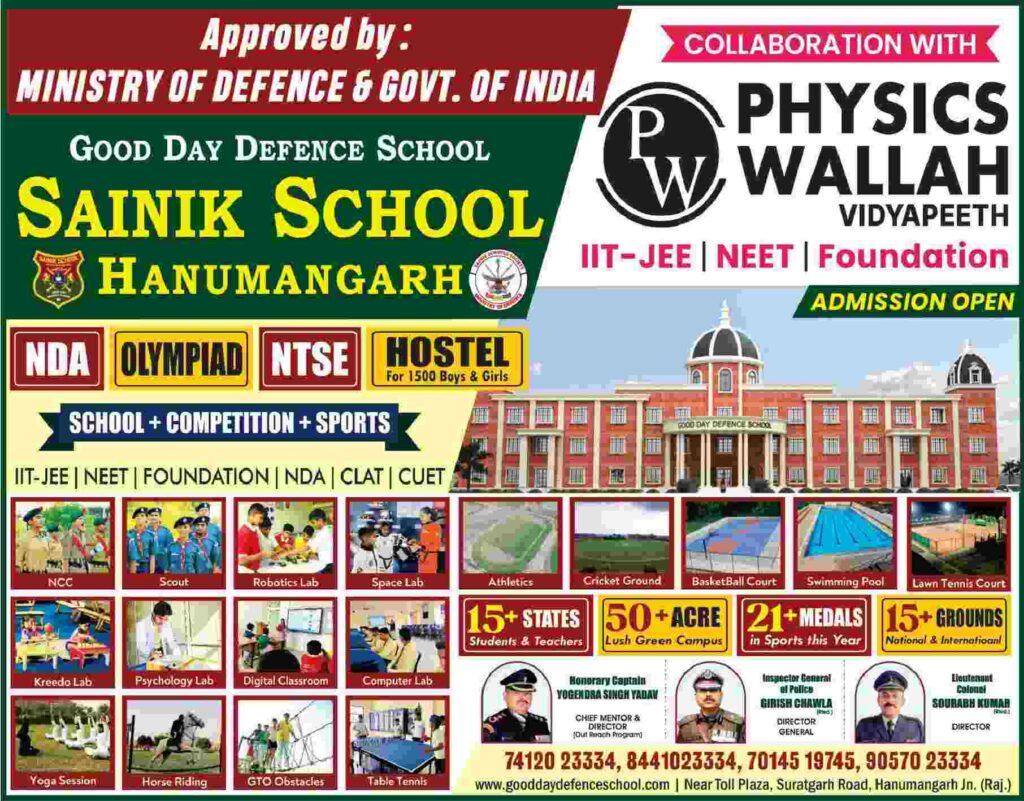
किताब पढ़ना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। किताबें हमारी सोच को गहराई देती हैं, धैर्य सिखाती हैं और कल्पनाशक्ति का विस्तार करती हैं। मोबाइल पर जानकारी तुरंत मिलती है, परंतु वह अक्सर सतही और अधूरी होती है। इसके विपरीत किताब हमें एकाग्रता, गंभीरता और स्वतंत्र सोच प्रदान करती है। किताबों के पन्नों से गुजरना हमें न केवल नया ज्ञान देता है, बल्कि जीवन जीने का सलीका भी सिखाता है।

इतिहास इस बात का गवाह है कि महान व्यक्तित्वों के जीवन में किताबों ने अहम भूमिका निभाई है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बचपन में आर्थिक तंगी के कारण अपने मित्रों से किताबें उधार लेकर पढ़ते थे। उन्होंने स्वयं कहा, ‘किताबें मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत रही हैं।’ अमृतलाल नागर, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, पुस्तकालयों में समय बिताकर न केवल साहित्य पढ़ते, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव अर्जित करते थे। यही आदत उन्हें महान लेखक बना गई। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के महान राष्ट्रपति, गरीब परिवार से आते थे। लकड़ी की रोशनी में किताबें पढ़ते-पढ़ते उन्होंने अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत बनाया कि पूरी दुनिया उन्हें आदर से याद करती है। ये उदाहरण बताते हैं कि किताबें किसी भी कठिन परिस्थिति में जीवन का सबसे बड़ा संबल बन सकती हैं।
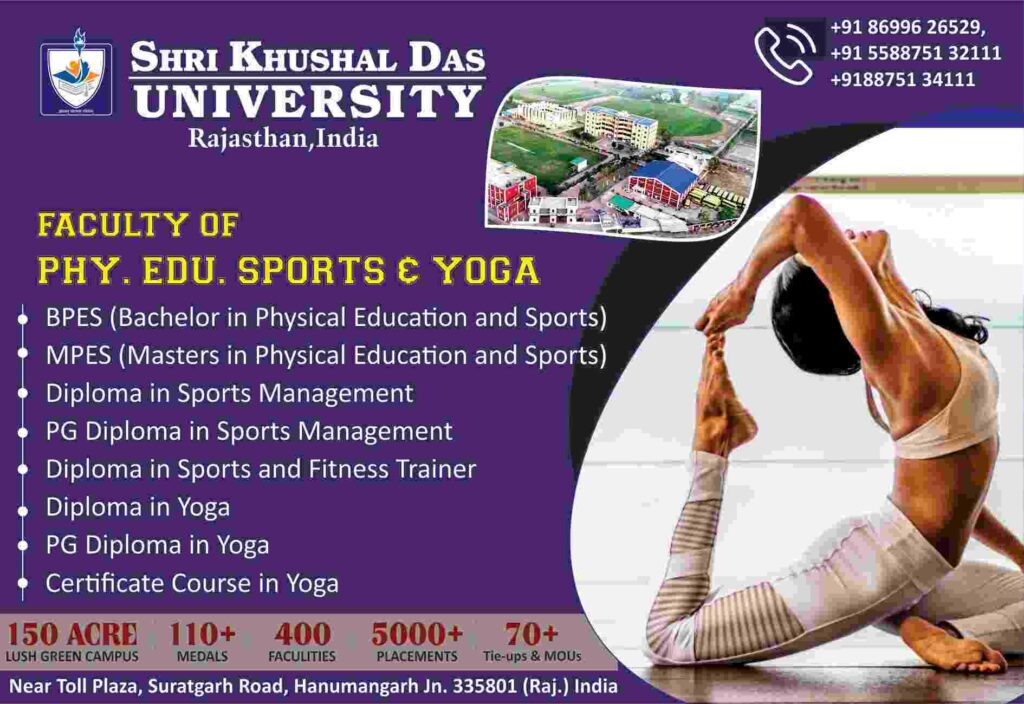
आज स्थिति बदलने की जिम्मेदारी केवल बच्चों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर है। माता-पिता, शिक्षक, स्कूल और समाज सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे। माता-पिता घर में किताबों का माहौल बनाएं, बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ और जन्मदिन पर खिलौनों के साथ किताबें भी उपहार में दें। स्कूल कक्षा में ‘रीडिंग पीरियड’ रखें, जहां बच्चे कहानी, जीवनी या अखबार पढ़ सकें। समाज और पुस्तकालय मोहल्लों और शहरों में बुक फेयर, रीडिंग क्लब और पुस्तकालय की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। मीडिया टीवी, अखबार और सोशल मीडिया किताबों को लोकप्रिय बनाने वाले अभियान चला सकते हैं।

यह भी सच है कि बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर करना न तो संभव है और न ही सही। मोबाइल पढ़ाई और जानकारी का एक बड़ा साधन है, लेकिन इसका प्रयोग सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। घर में ‘नो मोबाइल ज़ोन’ बनाएं, जैसे भोजन के समय या पारिवारिक बैठकों में। स्क्रीन टाइम तय करें और बच्चों को नोट्स किताब में लिखने की आदत डालें। हर हफ्ते परिवार मिलकर कोई किताब पढ़े और उस पर चर्चा करे। पढ़ाई से अलग भी कहानियाँ, जीवनी और उपन्यास पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
मोबाइल और किताब दोनों ही हमारे जीवन के साथी हैं। मोबाइल हमें तेज़ी से जानकारी देता है, पर किताबें हमें समझदारी और गहराई देती हैं। यदि माता-पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों को पढ़ने की आदत डालें, तो आने वाली पीढ़ी भी यह मानने से पीछे नहीं हटेगी कि ‘किताबें ही सच्ची मित्र होती हैं।’
-लेखक सामाजिक चिंतक, सीनियर सर्जन और आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं