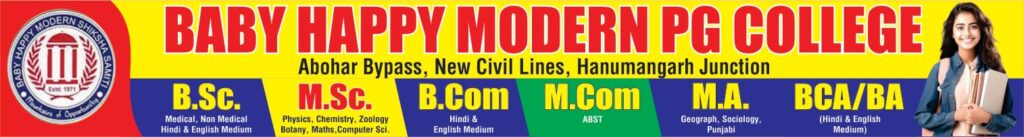गोपाल झा.
धूप ढल रही थी। खिड़की से छनकर आती रोशनी किताबों की कतार पर फैल रही थी। रैक की उस सबसे ऊपरी तह में रखी एक पुरानी डायरी की ओर निगाहें उठ गईं। वर्षों से जिसे छुआ नहीं था, आज अचानक जैसे वह मुझे बुला रही हो। धीरे से उतारी, खोली और पीले पड़ चुके पन्नों में पहली ही पंक्ति पढ़ते ही मन कहीं और चला गया,
‘काश, कबीर आ जाते इक बार!’
यह वाक्य मैंने कोई 30 साल पहले लिखा था, जब पहली बार कबीर के दोहे गहराई से समझे थे। तब मैं छात्र था, धर्म, समाज, राजनीति और और दर्शन में डूबा हुआ एक जिज्ञासु। लेकिन धर्म जितना पढ़ा, उतना उलझता चला गया। आरती, अज़ान, उपदेश और प्रवचनों के बीच एक प्रश्न हमेशा मन में गूंजता, धर्म क्या है? उसी उलझन में एक दिन लाइब्रेरी की किसी धूलभरी अलमारी में कबीर का संकलन हाथ लगा। पहले तो लगा, ये क्या है? न संस्कृत की छटा, न फारसी की लचक। भाषा बिलकुल सीधी। जैसे कोई गांव का बुज़ुर्ग हाथ पकड़कर जीवन समझा रहा हो। और तब पढ़ा था,
माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।
मन का मनका फेर दे, मन का मनका फेर।
दिल के किसी कोने में कुछ खटका। लगा, ये तो मेरी ही स्थिति है! मैं ग्रंथों में गोते खा रहा था लेकिन मन वैसा का वैसा ही था। ये दो पंक्तियाँ मुझे मेरी जगह दिखा गईं। फिर तो कबीर जैसे भीतर उतरते चले गए। जब-जब धर्म को लेकर भ्रमित होता, समाज में जात-पात और धार्मिक घृणा को देखता, तब-तब मन कह उठता, काश, कबीर आ जाते इक बार! वे आते और समाज को फिर से आईना दिखाते। कितना सरल, कितना गहरा उनका चिंतन था,
कंकर-पाथर जोड़ि के मस्जिद लई बनाय।
ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाय?
और इसके जवाब में,
जो हरि को खोजे मन्दिर मा, सो हरि मिले न काहें।
हरि तो बसे जीव के भीतर, चाहे जो तू राहें।
कबीर किसी एक धर्म की आलोचना नहीं करते थे, वे पाखंड पर चोट करते थे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। जब मुझे लगा कि मैं राम के अधिक निकट हूं, तब भी कबीर ने टोका,
पढ़ि-पढ़ि पंडित होय गया, पर दुई न छोड़ी रे।
कहे कबीर अब कहूं का, पढ़ि-पढ़ि भूतम बोली रे।
उनका यह ‘भूतम’ मुझे चुभ गया। क्या सचमुच मैं भी वही कर रहा हूं जो वे ‘पढ़े-लिखे पंडित’ कर रहे थे? समय बीतता गया। पत्रकारिता और अध्यापन मेरे लिए जुनून है। कुछ बरसों तक कॉलेज में पढ़ाया भी। कबीर मेरे भीतर बैठे रहे। मुझे याद है, एक बार किसी युवक ने जातिगत हिंसा पर बात की, तो मेरे मन में सबसे पहले यही पंक्ति आई,
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।
और उस दिन मैंने पहली बार समझाया था, धर्म का मतलब पूजा नहीं, प्रेम है। ज्ञान का मतलब प्रमाणपत्र नहीं, विवेक है। और गुरु वही जो बिना भय दिखाए सच बताए। मुझे आज भी याद है, एक बार कॉलेज में दो छात्र आपस में धर्म को लेकर भिड़ गए थे। बात तल्ख हो चली थी। मैंने शांत स्वर में सिर्फ एक दोहा पढ़ा,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।
कमाल था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जैसे कबीर खुद वहां खड़े हों। सच कहूं, कबीर की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं है, भावों में है। उनके दोहे जैसे किसी उलझे धागे को चुटकी में सुलझा देते हैं। आज जब धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, जब सड़कों पर ईश्वर को लेकर नारे लग रहे हैं, जब मंदिर-मस्जिद चुनावी मुद्दे बन रहे हैं, तब फिर वही पुराना पन्ना मन के किसी कोने से झांकता है,
काश, कबीर आ जाते इक बार!
कबीर आते, और समाज को फिर से यह सिखाते कि
साईं इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए।
वे हमें संतुलन सिखाते, सादगी सिखाते, और सबसे बढ़कर संवेदना सिखाते। आज की इस भागती दुनिया में, धर्म एक उद्योग बन गया है। मोक्ष बिकता है, पुण्य ‘पैक’ हो कर मिलता है। मंदिर और मठों में भव्यता है, लेकिन भीतर शांति का अभाव। ऐसे में कबीर की साखियां फिर से प्रासंगिक हो गई हैं। शायद इसीलिए मैं बार-बार उस डायरी को खोलता हूं, उस पंक्ति को पढ़ता हूं, और फिर से कल्पना करता हूं…
काश… कबीर आ जाते इक बार!
न किसी तिलक की बात करते, न टोपी की। न मंदिर की चिंता करते, न मस्जिद की। वे बस यह पूछते, ‘तेरे मन में प्रेम है क्या?’ और यही पूछते हुए फिर से कहीं बाज़ार में खड़े हो जाते,
कबीरा खड़ा बाज़ार में, सबकी मांगे खैर।
ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।
काश…सचमुच,
कबीर आ जाते इक बार!