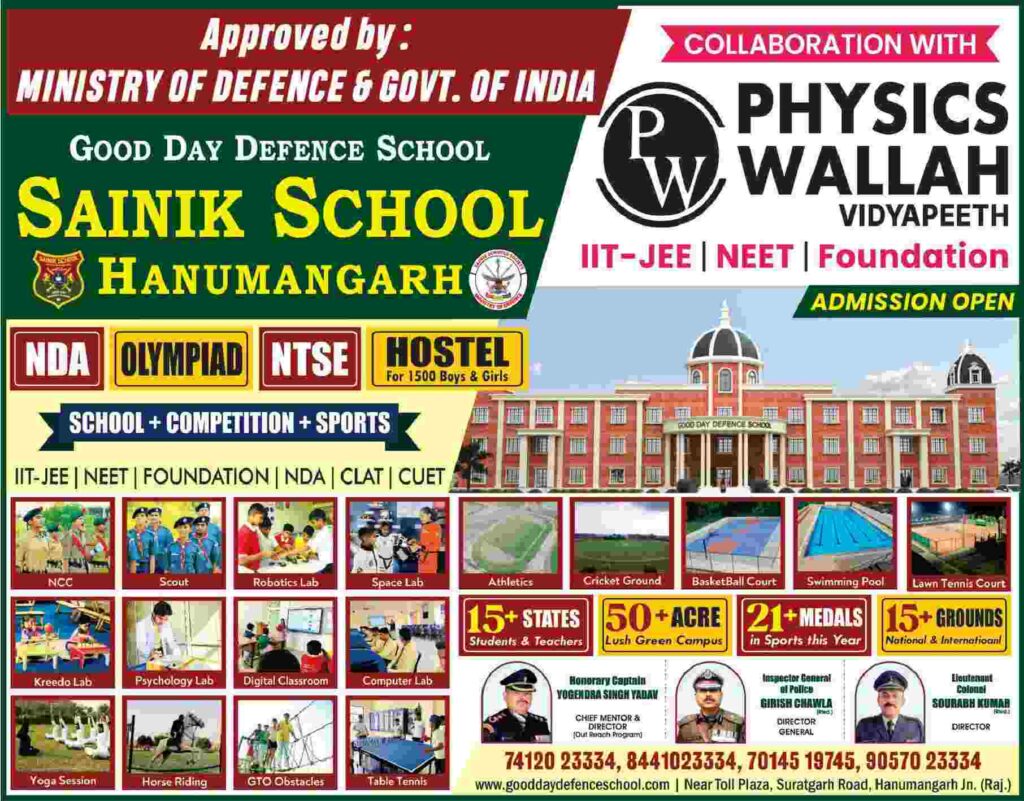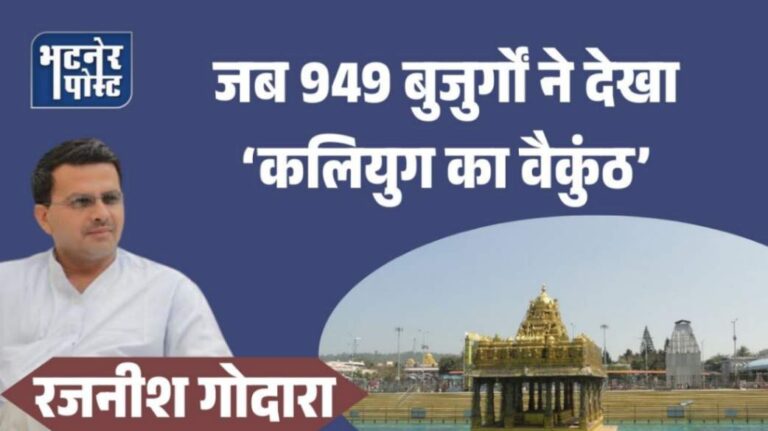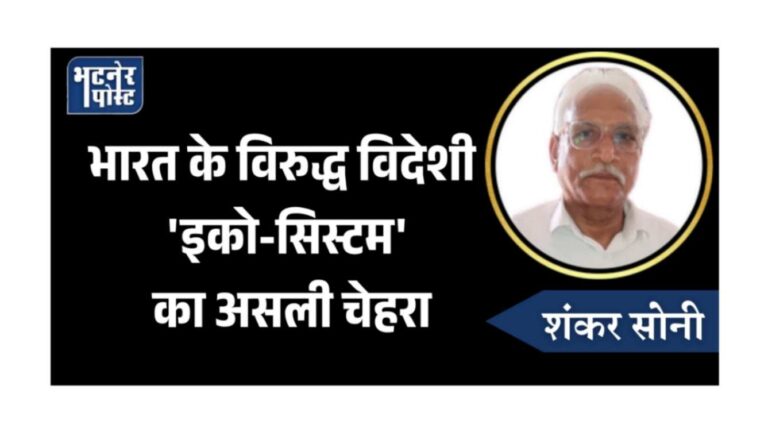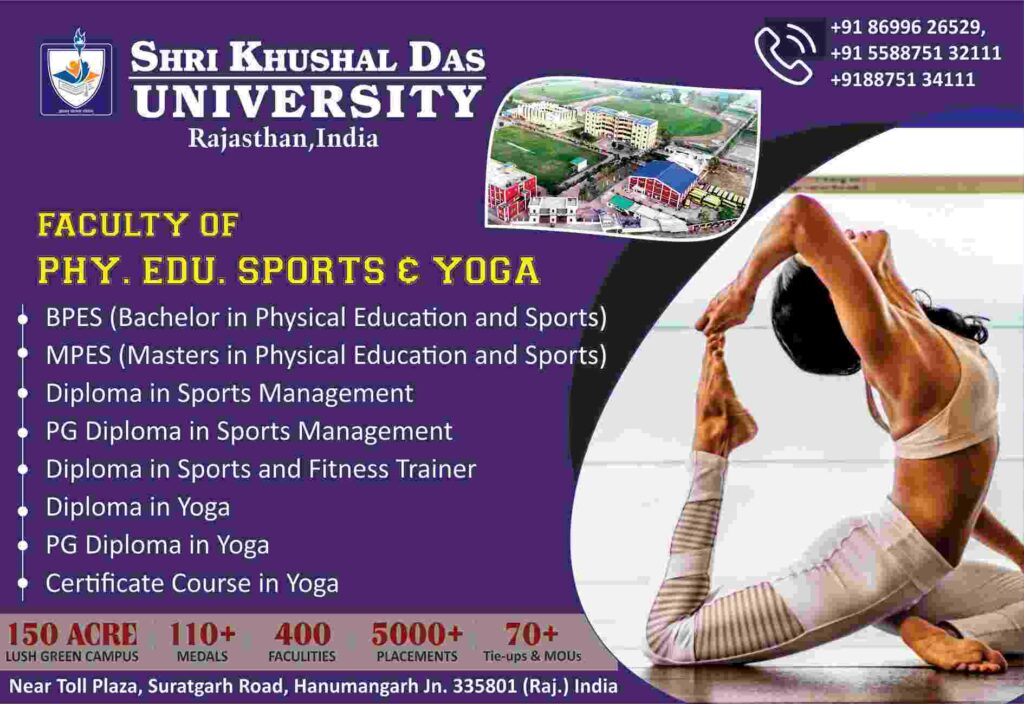
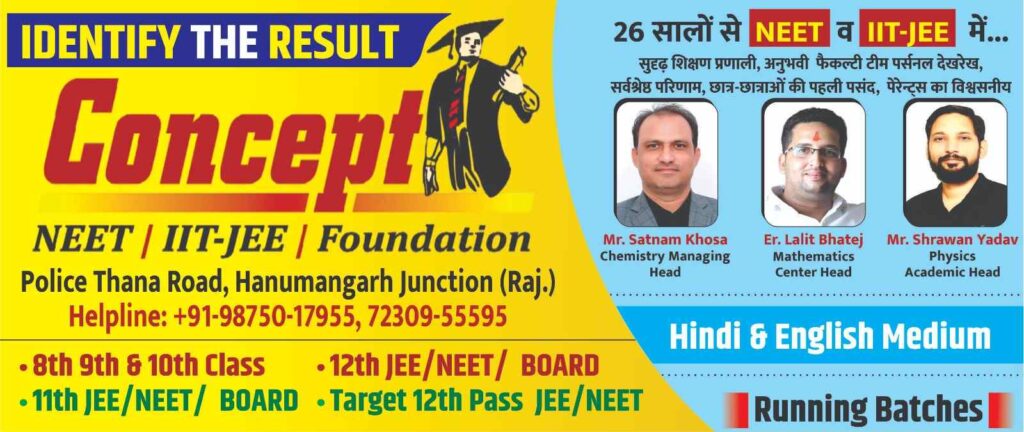
मनीष जांगिड़.
मनुष्य के जीवन का सबसे सुरक्षित और आत्मीय ठिकाना हमेशा उसका घर रहा है। घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं होता, यह भावनाओं, रिश्तों और संस्कारों का वह संगम होता है, जो व्यक्ति को पहचान और अपनापन देता है। किंतु बीते पाँच दशकों में भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने इस ‘घर’ की परिभाषा और उसकी आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है।
पहले संयुक्त परिवारों के बड़े घर होते थे। उस घर में दादा-दादी, चाचा-ताऊ, भतीजे-भतीजियाँ और पूरा कुनबा एक साथ रहता था। रसोई से उठती खुशबू, आँगन में बच्चों की किलकारियाँ घर को ‘घर’ बनाती थीं। लेकिन धीरे-धीरे यह घर मकान बनते चले गए, जहाँ परिवार तो रहा, लेकिन उसका विस्तार सिकुड़ गया। पिता, माता और बच्चों तक सीमित होते ही मकान का स्वरूप तो बचा, पर ‘घर’ की आत्मा कमज़ोर होने लगी।

इसके बाद शहरीकरण और बाज़ारीकरण की लहर आई। हर शहर में बिल्डरों ने फ्लैट कल्चर को बढ़ावा दिया। अब आँगन, बरामदे और छत की जगह बालकनी और कॉमन एरिया ने ले ली। रिश्ते अपार्टमेंट की दीवारों तक सीमित हो गए। बाज़ार का नियम है, जितनी अधिक आबादी, उतने अधिक घर; और जितने अधिक घर, उतना बड़ा कारोबार। इसी तर्क से घर, मकान और फ्लैट अब केवल एक उत्पाद बन गए, जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है।
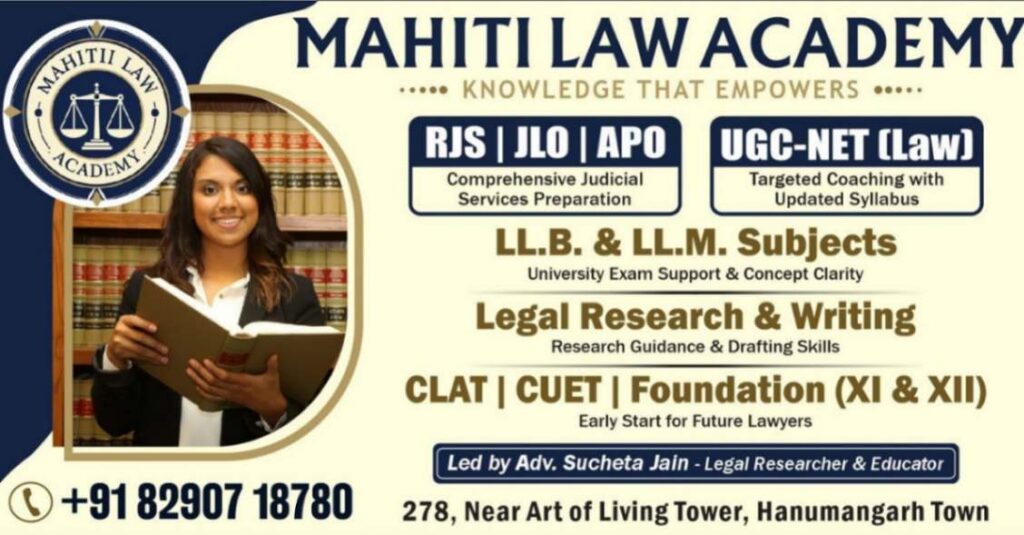
लेकिन सबसे चिंता का विषय यह है कि अब फ्लैटों के बाद समाज का अगला पड़ाव वृद्धाश्रम बनता जा रहा है। 70-80 साल के बुज़ुर्ग, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा परिश्रम और संघर्ष में लगाया, वे अब संतान के साथ न रहकर किसी संस्था की शरण में जीवन व्यतीत करने लगे हैं। हैरानी तो तब होती है जब 50 वर्ष की आयु वालों तक को यह महसूस होने लगता है कि उनकी संतान उन्हें भविष्य में अपने साथ रखने की स्थिति में नहीं होगी।

नई पीढ़ी आज डबल इनकम फैमिली और प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली में जी रही है। पति-पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई और करियर की तैयारी अलग दबाव है। ऐसे में बुज़ुर्गों की देखभाल उनके लिए कठिन कार्य बन जाता है। शहरों में तो स्थिति यह हो गई है कि सेवा-एजेंसियाँ लड़के-लड़कियाँ हायर करके माता-पिता की देखभाल कराती हैं। हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर में भी यह चलन शुरू हो चुका है।

यह स्थिति केवल आर्थिक दबाव की नहीं, बल्कि संस्कारों के क्षरण की भी गवाही देती है। भारतीय संस्कृति में ‘मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः’ का आदर्श रहा है। माता-पिता की सेवा को सर्वाेच्च धर्म माना गया है। परंतु आधुनिकता की दौड़ में यह मूल्य धूमिल पड़ रहे हैं।
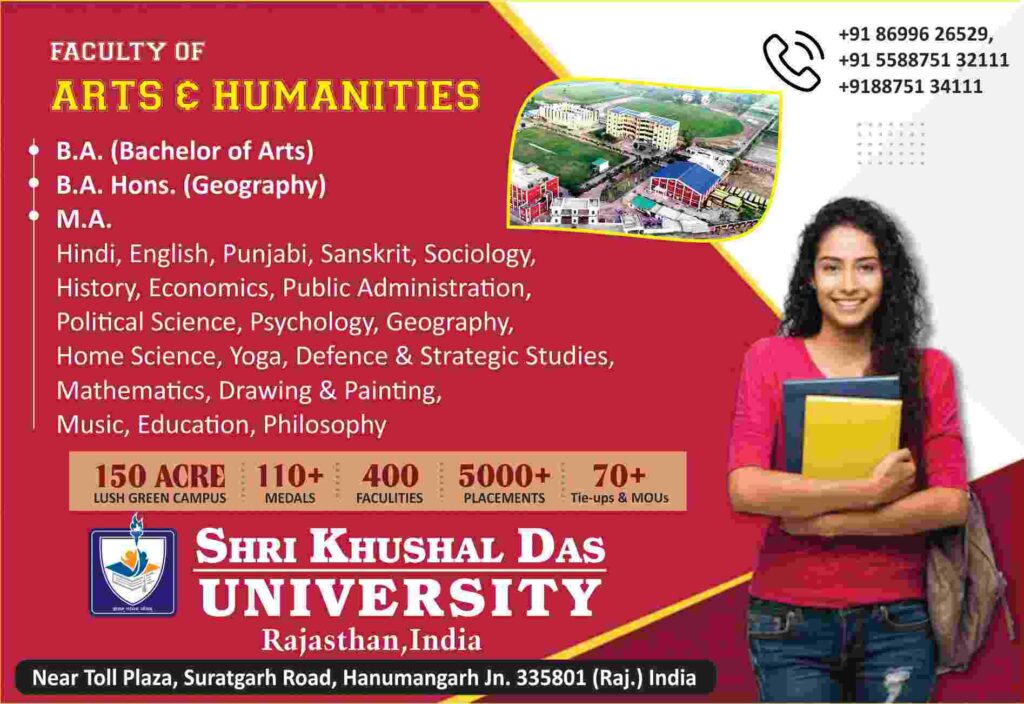
समस्या केवल सामाजिक ढांचे की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही यह शिक्षा देनी होगी कि परिवार केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग का आधार है। बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि माता-पिता केवल जन्मदाता नहीं, बल्कि जीवनभर के सहारा हैं। करियर और कमाई ज़रूरी हैं, लेकिन परिवार और बुज़ुर्गों के साथ समय बिताना उतना ही आवश्यक है।
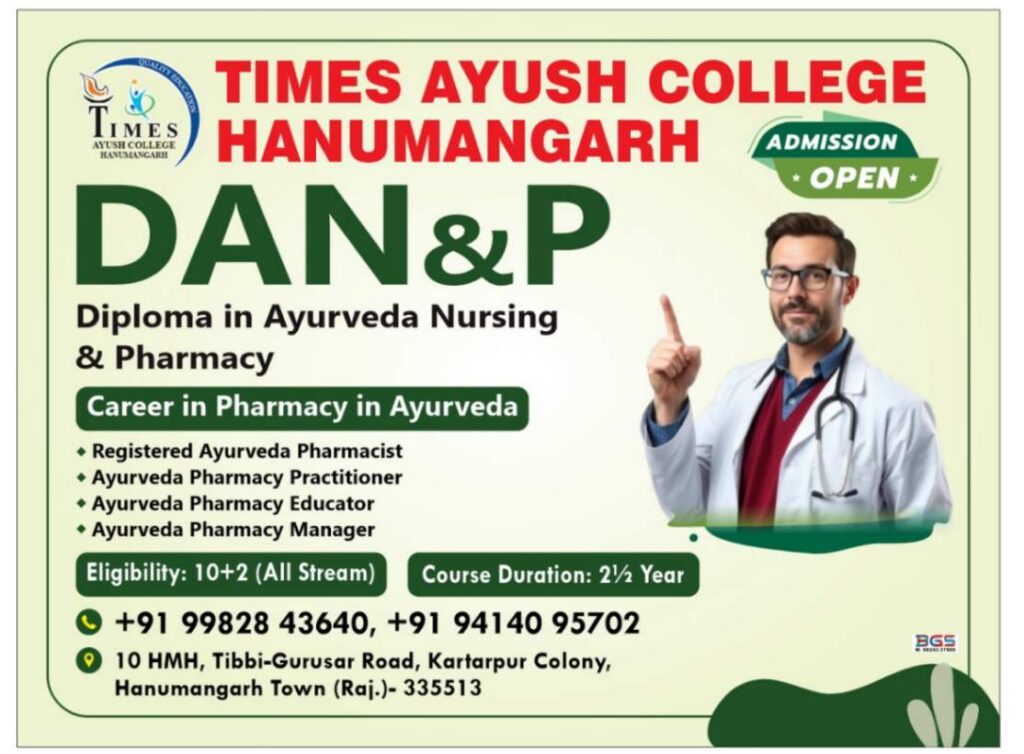
संयुक्त परिवार भले ही पूरी तरह लौट न सकें, लेकिन रिश्तों का जुड़ाव बनाए रखने के लिए सामूहिक मेल-मिलाप और परस्पर सहयोग की परंपरा पुनर्जीवित करनी होगी। सरकार और समाज को ऐसे तंत्र विकसित करने होंगे जो बुज़ुर्गों को अकेलेपन से बचाएँ। लेकिन यह ज़िम्मेदारी परिवार की जगह नहीं ले सकती, बल्कि उसका सहायक मात्र हो सकती है।

घर से मकान, मकान से फ्लैट और फ्लैट से वृद्धाश्रम तक का यह सफर केवल स्थापत्य का नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और सामाजिक मूल्यों के पतन का दर्पण है। यह सही है कि समय बदलता है और जीवनशैली में बदलाव आते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संस्कार और संवेदनाएँ किसी भी समाज की आत्मा होते हैं। यदि हमने उन्हें संभालने का प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ न केवल बुज़ुर्गों से बल्कि अपने ही अस्तित्व से कट जाएँगी। आज ज़रूरत है आत्ममंथन की। क्या हम अपने बच्चों को केवल भौतिक सुख-सुविधाएँ देंगे, या उन्हें वह संस्कार भी देंगे जो घर को फिर से ‘घर’ बना सकें?