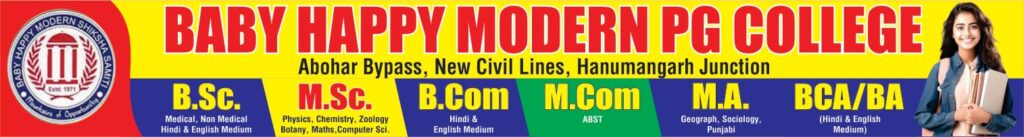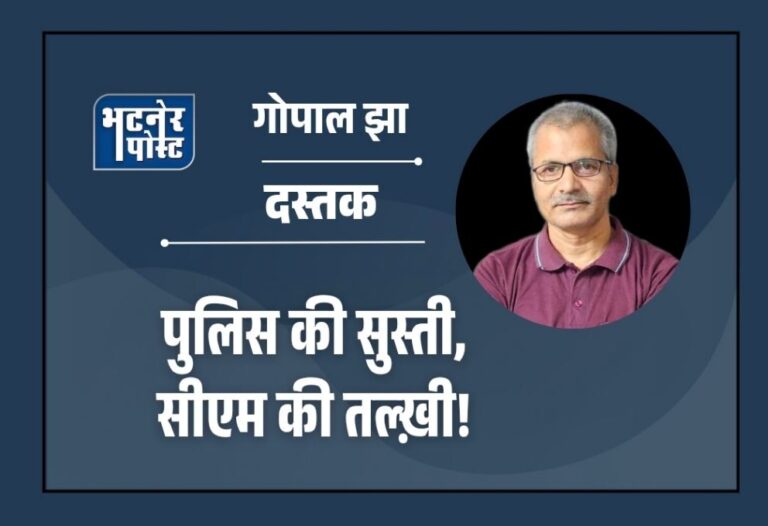गोपाल झा.
राजनीति की दुनिया अजीब है, इतनी अजीब कि कभी-कभी लगता है मानो इसे किसी बड़े रंगमंच पर खेला जा रहा ‘नाटक’ ही समझ लिया जाए। पात्र बदलते रहते हैं, संवाद बदल जाते हैं, पर कहानी का सार वही रहता है, सत्ता की भूख और जनता की सहनशीलता। हालिया दौर में जिस ‘बदलाव’ की बड़ी धूम मची है, वह असल बदलाव नहीं, नामों का बदलाव है। शहरों से लेकर भवनों तक, दफ्तरों से लेकर योजनाओं तक, जैसे हम शब्दों से देश की तकदीर को चमका देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया ‘सेवा तीर्थ’ और राजभवन ‘लोकभवन’। सुनने में मीठे लगते हैं, जैसे किसी नए युग की सूचना हो, लेकिन भीतर से खोखले, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी इमारत को बाहर से नया रंग कर देने से वह टिकाऊ नहीं बन जाती।

नाम बदलने का यह जोश 2014 के बाद से यूँ बढ़ा जैसे किसी ने जादुई मंत्र फूँक दिया हो। शहर, सड़कें, रेलवे स्टेशन, योजनाएँ, सब पर नए लेबल चिपकाने की दौड़ चल पड़ी। समर्थक तालियाँ बजाते रहे, विरोधी माथा पकड़ते रहे, पर असल सवाल हवा में ही टँगा रहा, क्या कुछ बदल भी रहा है? विडंबना यह है कि वो तमाम तीर, जो कभी डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार पर छोड़े जाते थे, रुपये की गिरावट से लेकर महंगाई तक, अब उन्हीं निशानों को चुपचाप सहते हुए बीत जाते हैं। तब डॉलर 60 के आसपास था, आज 90 पार कर हवा में तिर रहा है, पर आवाज कहीं नहीं। यह राजनीति का पुराना नियम है, सत्ता पक्ष की चुप्पी उतनी ही लंबी होती है, जितना उनका बचाव कमजोर होता है।

अब सवाल उठता है, क्या ‘सेवा तीर्थ’ लिख देने भर से प्रधानमंत्री कार्यालय का चरित्र बदल जाएगा? क्या ‘लोकभवन’ कह देने से जनता का भला हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या फाइलें तेजी से चल पड़ेंगी? क्या कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छोटा दुकानदार सिर्फ नाम बदलने से राहत पा लेगा? जवाब सबको पता है, पर कोई जोर से नहीं बोलता।

असली बदलाव वहाँ है जहाँ राजनेता देखना ही नहीं चाहते, अपने भीतर। जनता की गाढ़ी कमाई से बनी शाही सुविधाओं का भार उठाते हुए नेता जब त्याग की बात करते हैं, तो वह बुलबुले की तरह उछल कर हवा में फूट जाता है। अगर सचमुच बदलाव लाना है तो शुरुआत नाम बदलने से नहीं, चरित्र बदलने से होनी चाहिए, स्वयं पर लागू कठोरता से, अनावश्यक सुविधाओं के त्याग से, ईमानदार शासन के अभ्यास से।
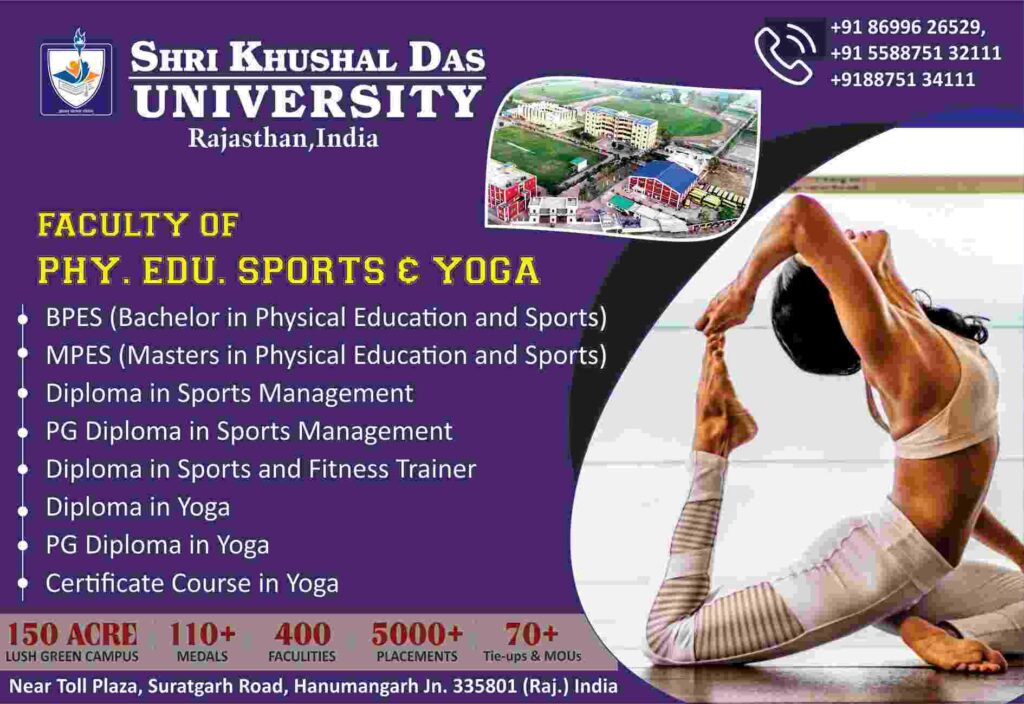
नाम बदलने की राजनीति में एक और सच्चाई छिपी है, बड़े खर्च की। यह बात आम जनता शायद ही समझ पाती है कि शहरों और संस्थानों के नाम बदलने में करोड़ों झोंक दिए जाते हैं, साइनबोर्ड, दस्तावेज़, रिकॉर्ड, स्टेशनरी, नक्शे, फाइलें, सब बदले जाते हैं। और यह पैसा जाता कहाँ से है? जनता की जेब से। महंगाई के रूप में, टैक्सों के रूप में, सेवाओं की कमी के रूप में। सत्ता पर बैठे लोग इसे नहीं महसूस करते, क्योंकि उनके ऊपर आने वाले खर्च का बोझ जनता के कंधों पर सधा होता है।
ताज्जुब यह है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता निभाती है, पर वही सबसे कम जागरूक दिखाई देती है। नेताओं की शब्द-कला और भावनात्मक नारेबाज़ी ने उसे इतना उलझा दिया है कि असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और पारदर्शी शासन। इन सबका हल नाम बदलने से नहीं, नीतियों, नैतिकता और नीयत के बदलाव से आएगा।
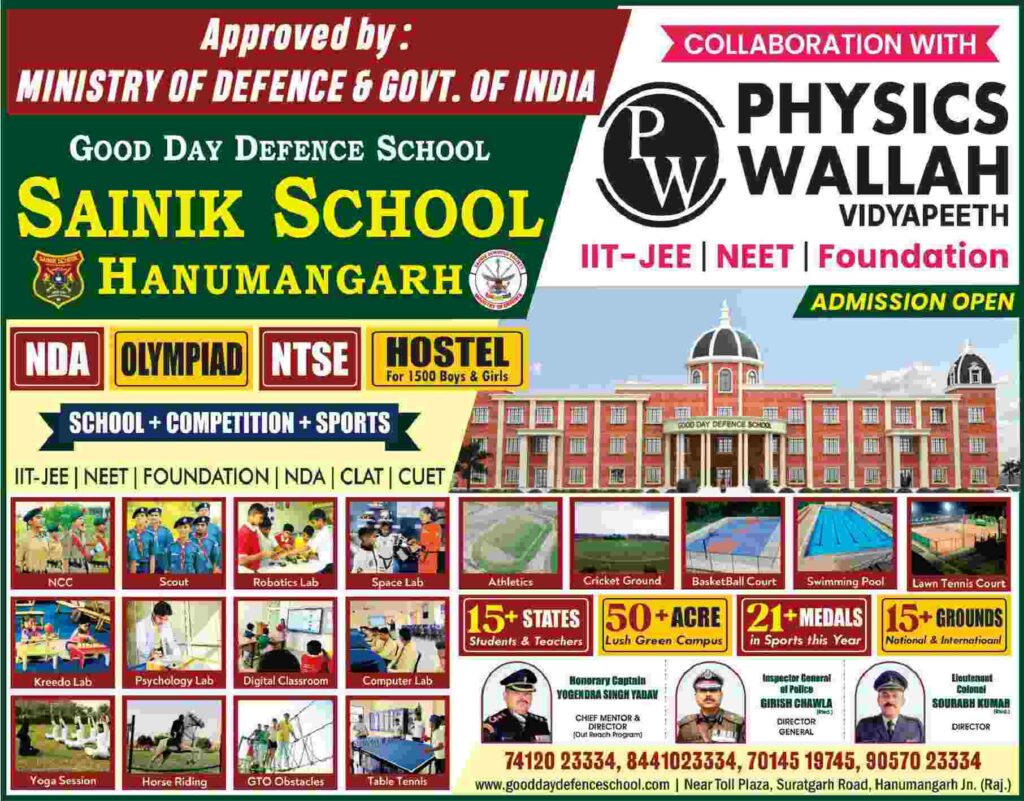
बदलाव का अर्थ तब सार्थक होगा जब नेता सुविधा-शुल्क की संस्कृति खत्म करेंगे, शाही खर्च कम करेंगे, सादगी को आत्मसात करेंगे और पद को जनसेवा समझेंगे न कि विशेषाधिकार। लोकतंत्र का उजाला तभी फैलेगा जब सत्ता अपने लिए नहीं, जनता के लिए चेतन होगी। काश, सरकारें यह समझ पातीं कि नाम बदलने से चूल्हे नहीं जलते, अस्पताल नहीं सुधरते, सड़कें नहीं बनतीं और न ही भ्रष्टाचार भागता है। असल रोशनी चरित्र के बदलाव से आती है, कार्यशैली के सुधार से, जवाबदेही के बढ़ने से। जनता जितनी जल्दी यह समझेगी, राजनीति उतनी ही कम छल करेगी। वरना, मंच पर नाटक बदलते रहेंगे, पर पर्दे के पीछे वही पुरानी पटकथा चलती रहेगी, नाम बदलो, काम वही रहने दो।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया गुप के चीफ एडिटर हैं