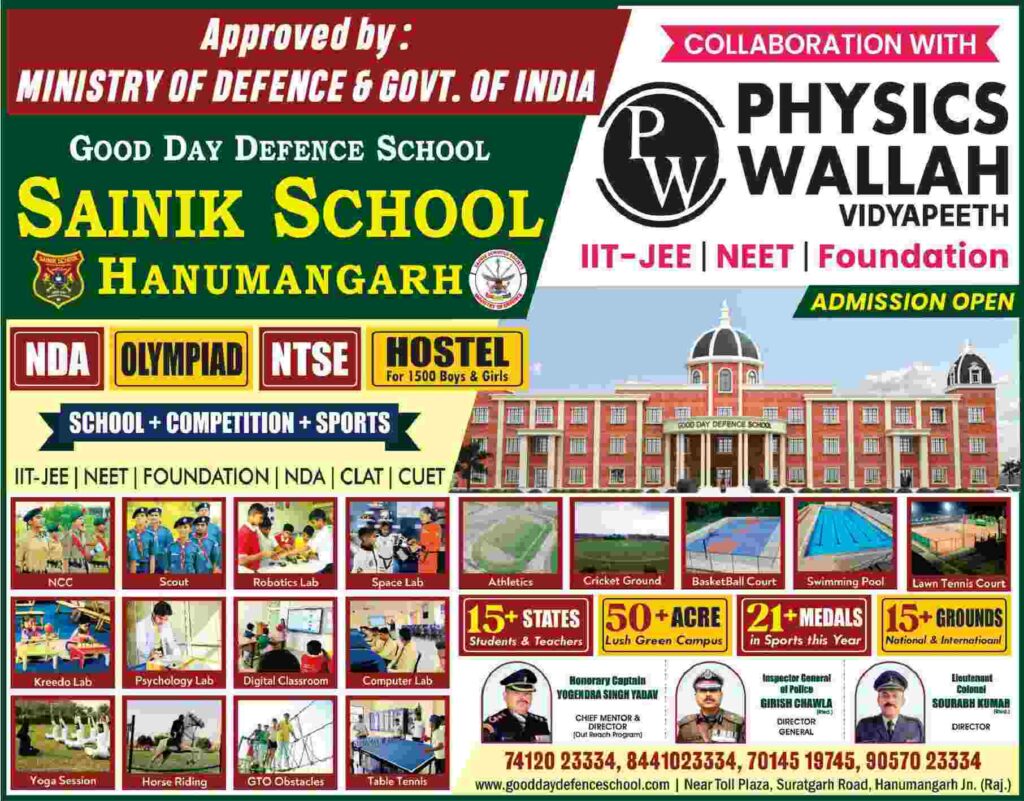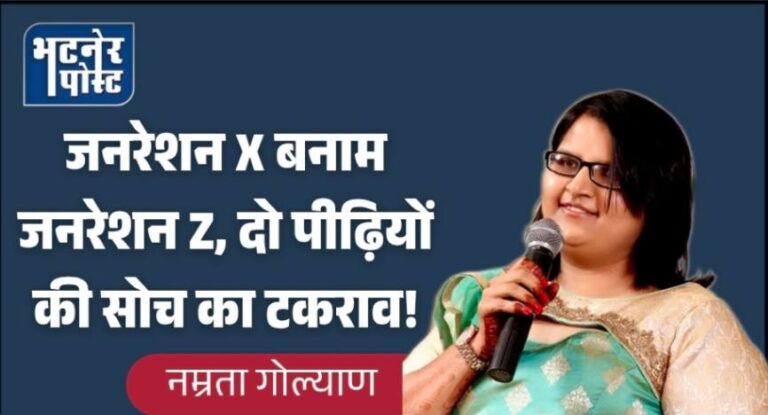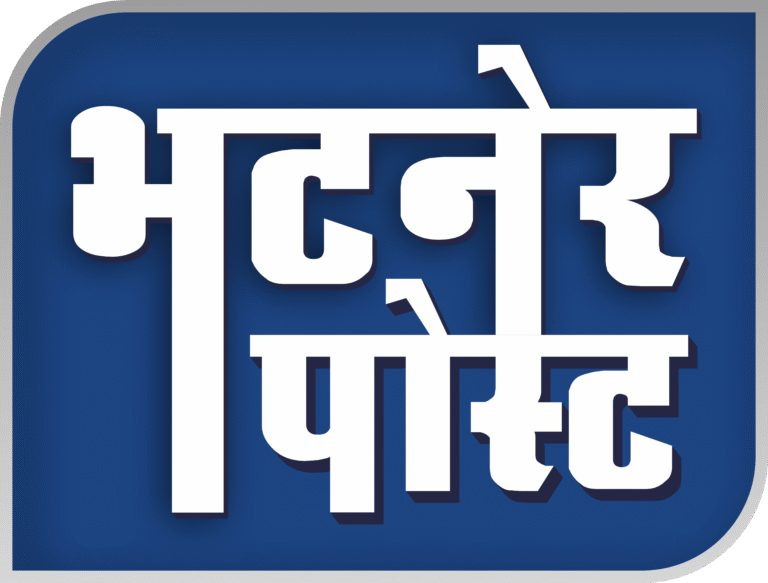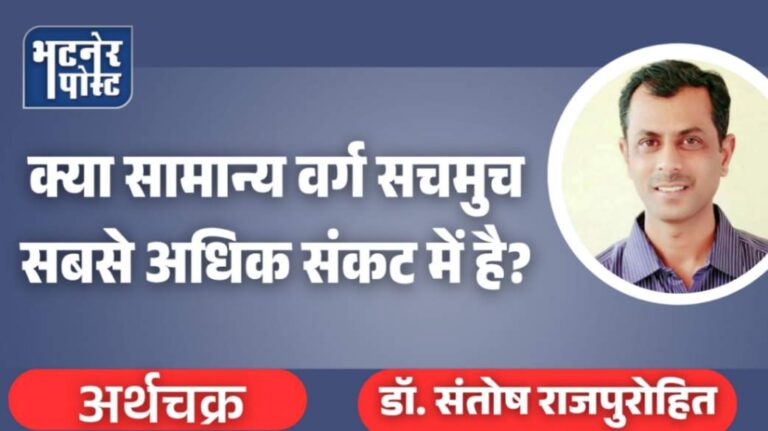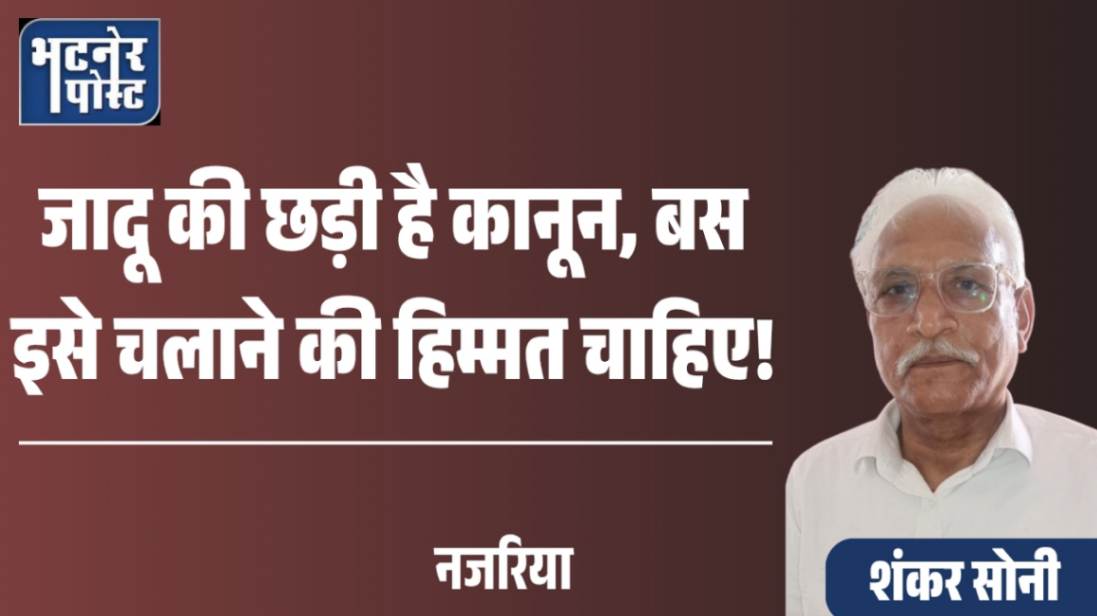


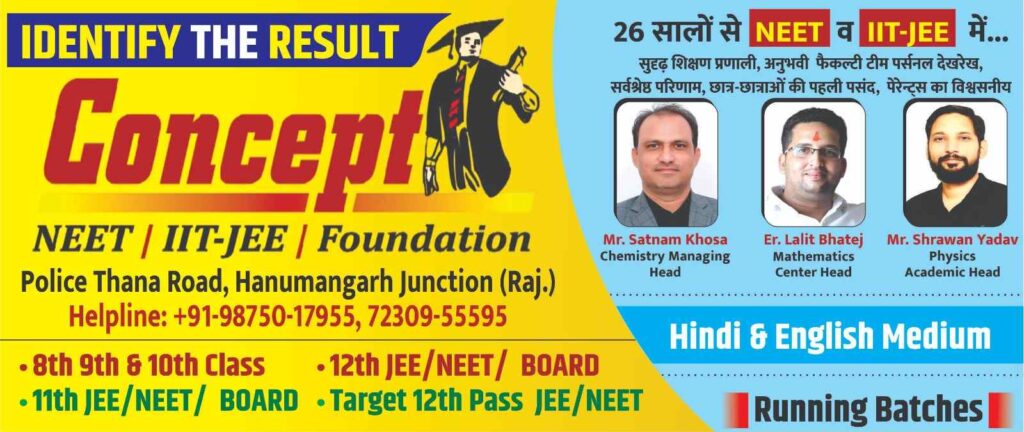

शंकर सोनी.
सिर पर धुएँ की टोपी और हवाओं में ज़हर। ऐसे माहौल में जब देश संविधान दिवस मना रहा था, तब सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी चुभ गई, ‘दिल्ली के वायु प्रदूषण को तुरंत ठीक करने के लिए न्यायपालिका के पास कौन-सी जादुई छड़ी है?’ इसे सुनकर लगा जैसे संविधान की आत्मा ने खामोशी में करवट बदली हो। लोकतंत्र के रक्षक के मुंह से ऐसी लाचारी निकलना भारतीय जनतंत्र की रीढ़ में अजीब-सा खड़खड़ाहट पैदा करता है। वायु प्रदूषण कोई स्वाभाविक विपत्ति नहीं है जिसे हम आकाश से उतरी आपदा मानकर छोड़ दें। यह इंसानी लापरवाही से पैदा हुआ संकट है, सरकारी अनुमति से मोहल्लों के बीच चल रहे कारखाने, ईंट भट्टे, खुलेआम फैलता धुआँ, बिना रोक-टोक की औद्योगिक गतिविधियाँ। कानून किताबों में है, दफ़्तरों में नोटिंग है, समितियों में बैठकें हैं, पर हवा में सिर्फ धुआँ है।

ऐसे में एक आम नागरिक का सवाल बड़ा सीधा है, जब सांस लेने की हवा और पीने का पानी तक सुरक्षित नहीं, तो संविधान का ‘जीवन का अधिकार’ आखिर किसकी शोभा बढ़ा रहा है? मौलिक अधिकार कागज पर बने रहने के लिए नहीं थे; वे जीवित रहने के आधार थे। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाए गए थे। हरियाणा-दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रेस्पांस ऐक्शन प्लान हो या औद्योगिक मानक, सब मौजूद हैं। मगर नियम तोड़ने वालों की एक खास किस्म की सुरक्षा छतरी भी मौजूद है, कहीं वोट बैंक का दबाव, कहीं नेताओं के आश्रय, कहीं अधिकारियों का मौन सहयोग और कहीं पूंजीपतियों का रसूख।

जब कानून लागू ही न हो, तो प्रदूषण करने वाले बेखौफ घूमते हैं। और यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जिन्होंने आबादी के बीच धुआँ उगलने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस दे दिए?
न्यायपालिका की भूमिका, क्या वाकई जादुई छड़ी नहीं है? मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी में निराशा झलक सकती है, पर कानून की किताबें कहती हैं कि न्यायपालिका के पास अधिकार भी हैं और औजार भी। तीखे शब्दों में कहें तो, जनता को उम्मीद है कि सर्वाेच्च न्यायालय हाथ खड़े नहीं करेगा।
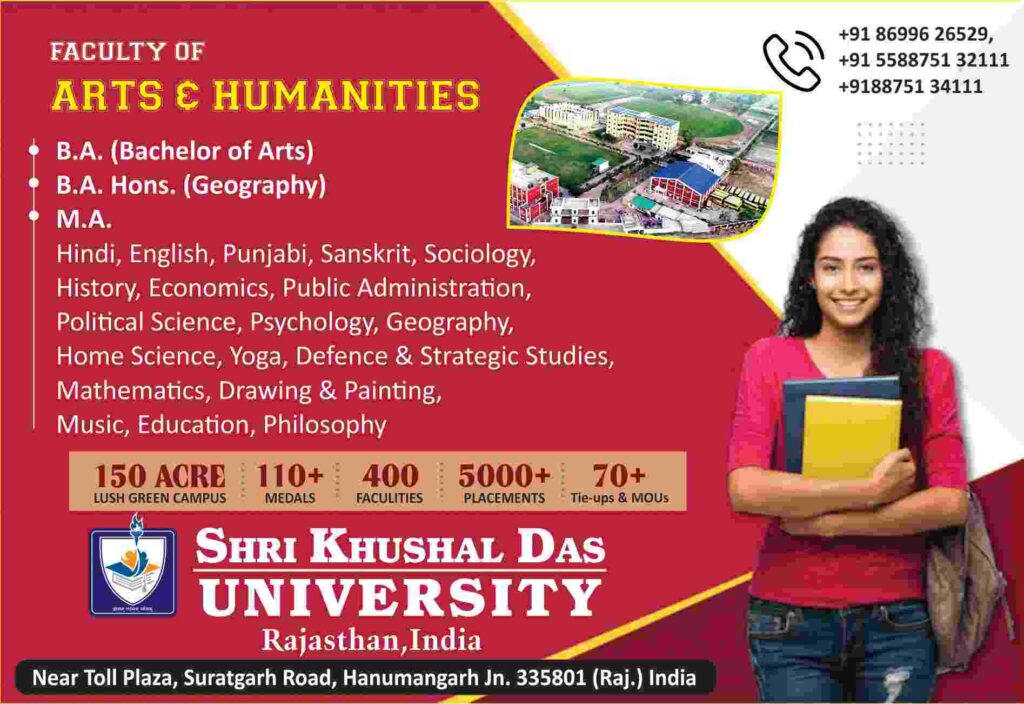
असल में समस्या के कारणों में ही समाधान का रास्ता छिपा होता है। वह इस पूरे विमर्श की धुरी है। अगर जनस्वास्थ्य की रक्षा करने में राज्य असफल होता है, तो संविधान का नैतिक आधार कमजोर हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की व्याख्या साफ है, स्वस्थ वातावरण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर सरकारें जहरीली हवा को ‘सामान्य स्थिति’ मानने लगें, तो यही अधिकार खोखला हो जाता है। जनस्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र का मूल कर्तव्य होता है। देश में सड़कें, पुल, इमारतें सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है नागरिक की सांस का अधिकार। और जब इस मूल अधिकार की रक्षा कोई संस्था नहीं कर पा रही, न सरकारें, न एजेंसियाँ, तब सुप्रीम कोर्ट से यह कहना कि वह भी मजबूर है, कहीं-न-कहीं जनता की उम्मीदों को चोट पहुँचाता है।
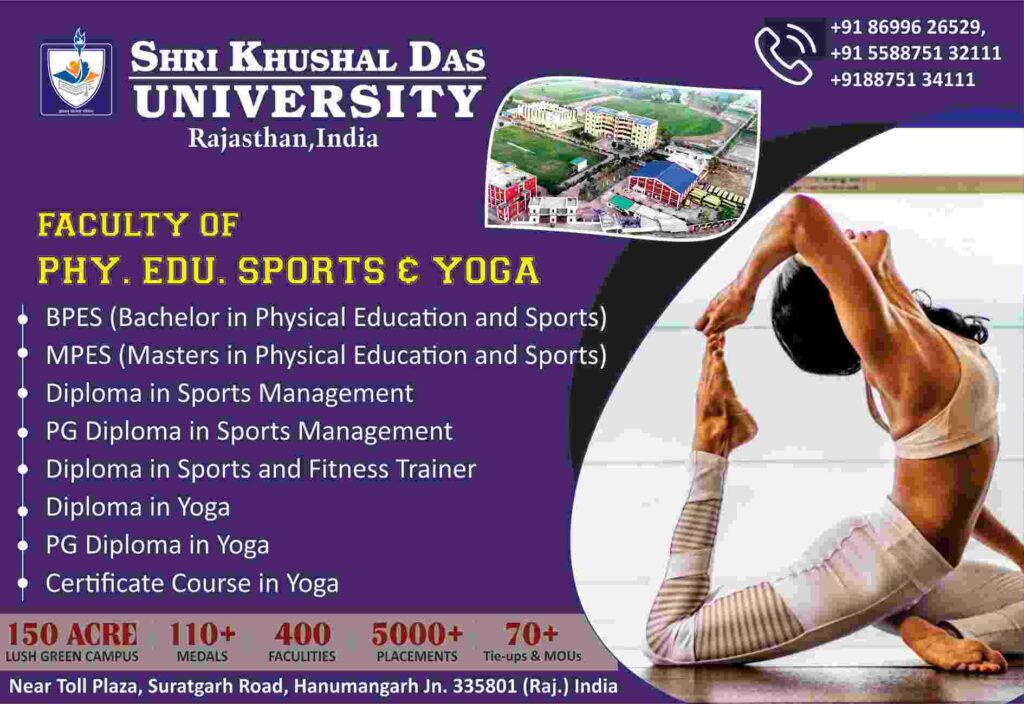
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका के पास एक ही जादुई छड़ी है, कानून का कठोर, बिना डरे और बिना दबाव के प्रयोग का आदेश। कोर्ट चाहे तो, प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों की लाइसेंसिंग की व्यापक समीक्षा करवा सकता है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत दंडात्मक कार्रवाई का मार्ग खोल सकता है। गैर-अनुपालन पर कड़े जुर्माने और तत्काल बंदी आदेश जारी कर सकता है।

‘कैसे प्रदूषण दूर नहीं होगा?’ दिल्ली और पूरा एनसीआर एक ऐसे गैस चेंबर में बदल चुका है जहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही दमा का खतरा भी जन्म लेता है। यह स्थिति किसी राष्ट्र के लिए शर्म से कम नहीं। निष्कर्ष यही कि न्यायपालिका को असहायता की नहीं, सक्रियता की जरूरत है। सरकारों को राजनीतिक चिंताओं से ऊपर उठकर जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और कानूनों का पालन करवाना ‘विकल्प’ नहीं, राष्ट्र का मूल धर्म है। अगर हवा ही जहर हो, तो कोई भी लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता, फिर चाहे संविधान दिवस के मंच पर कितने ही भाषण क्यों न गूंजें।
-लेखक नागरिक सुरक्षा मंच के संस्थापक और पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं