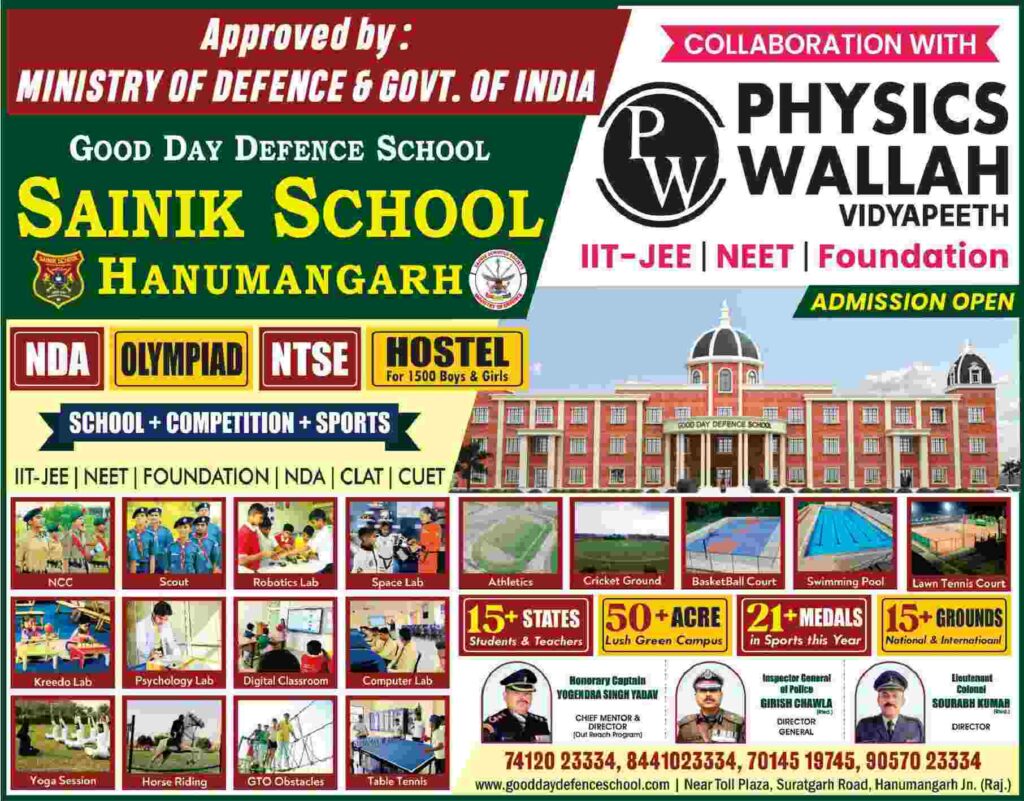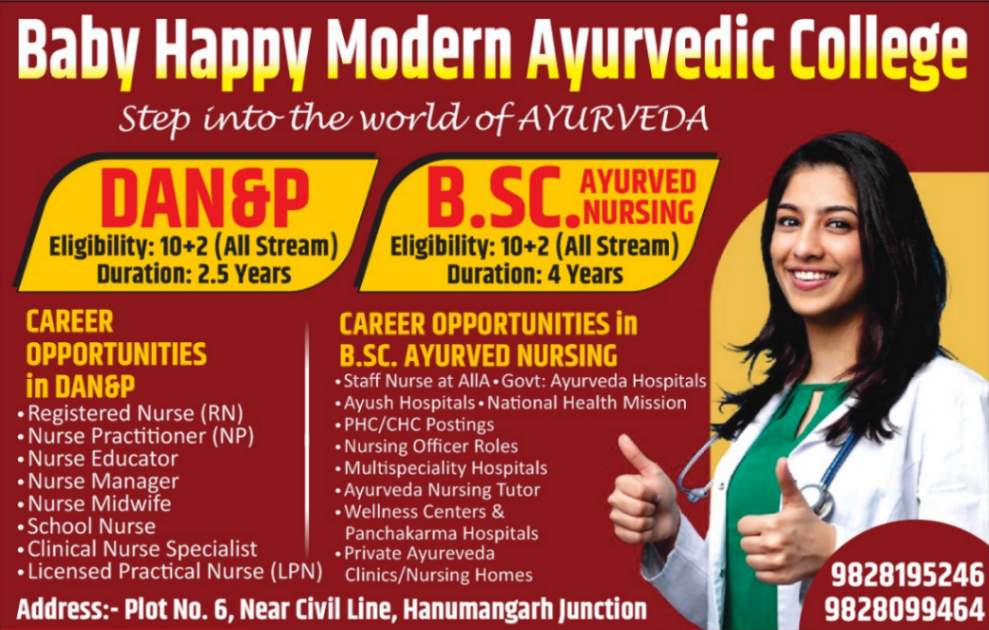


भटनेर पोस्ट ब्यूरो.
साल 2014 से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रतीकों और शब्दों की परिभाषाओं को नया आयाम देने की कोशिश की। शहरों और सड़कों से लेकर पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं के नाम बदलने तक की प्रक्रिया को इसी कड़ी में देखा जाता है। इतिहास की घटनाओं और तथ्यों की व्याख्या भी आज राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ‘स्वदेशी’ शब्द की नई व्याख्या ने इस विमर्श को और तीखा कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के व्यापारी गर्व से अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाएं, जिसमें साफ लिखा हो, ‘यहां मिलने वाला सामान स्वदेशी है।’ उनका तर्क था कि इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी, स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल सामान खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे गर्व और स्वाभिमान से जोड़कर हर नागरिक को इसे बढ़ावा देना चाहिए। त्योहारों के मौके पर उन्होंने लोगों से संकल्प लेने की अपील की कि वे स्वदेशी सामान ही खरीदें।

यह संदेश अपने आप में आकर्षक और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर इसके गहरे निहितार्थ हैं। दरअसल, मोदी जिस ‘स्वदेशी’ की बात कर रहे हैं, उसमें विदेशी कंपनियों के भारत में निर्मित उत्पादों को भी शामिल कर रहे हैं। यही वह बिंदु है जिसने विवाद और असहमति को जन्म दिया है।
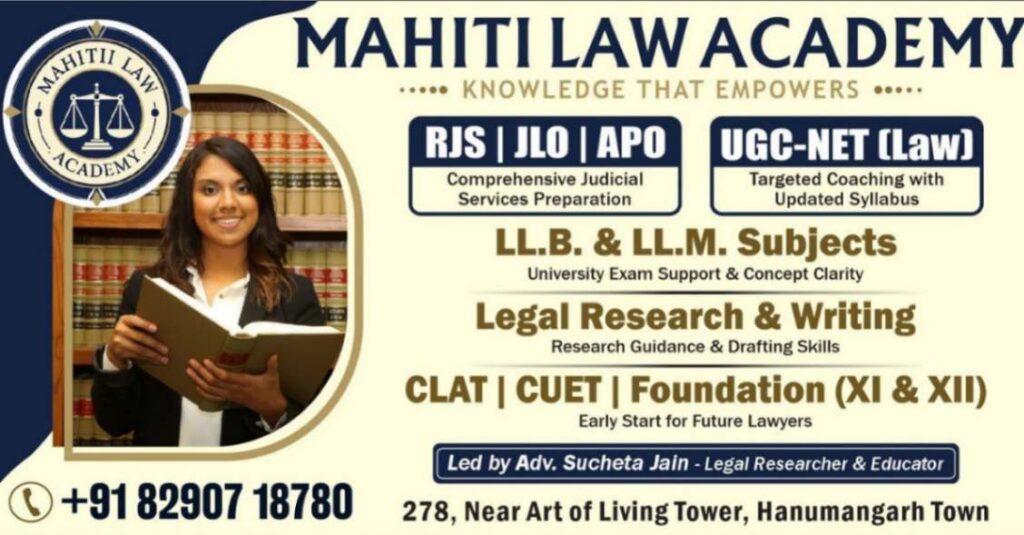
स्वदेशी का विचार भारत में नया नहीं है। महात्मा गांधी ने इसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बनाया था। उनके लिए स्वदेशी का मतलब ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योगों का विकास और स्थानीय संसाधनों के आधार पर उत्पादन था। गांधी के लिए स्वदेशी सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक क्रांति का हिस्सा था।

इसके उलट, मोदी की परिभाषा में विदेशी कंपनियों के भारत में बनाए गए उत्पादों को भी स्वदेशी मान लिया गया है। सवाल यह है कि अगर अमेरिकी, चीनी या यूरोपीय कंपनियों के उत्पाद भी स्वदेशी कहलाएंगे, तो फिर गांधी के ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों का स्थान क्या होगा? क्या यह स्वदेशी का व्यावहारिक स्वरूप है या शब्द का ‘विभत्स रूप’, जैसा कि आरएसएस के कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवक मानते हैं?

प्रधानमंत्री मोदी स्वयं लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक रहे हैं। परंतु स्वदेशी की इस व्याख्या पर संघ का रुख पूरी तरह सकारात्मक नहीं दिख रहा। एक पुराने स्वयंसेवक ने साफ कहा है कि स्वदेशी का अर्थ केवल यह नहीं है कि सामान भारत में बना हो। स्वदेशी वह है, जो भारतीय संस्था द्वारा भारतीयों की मेहनत से तैयार किया गया हो।
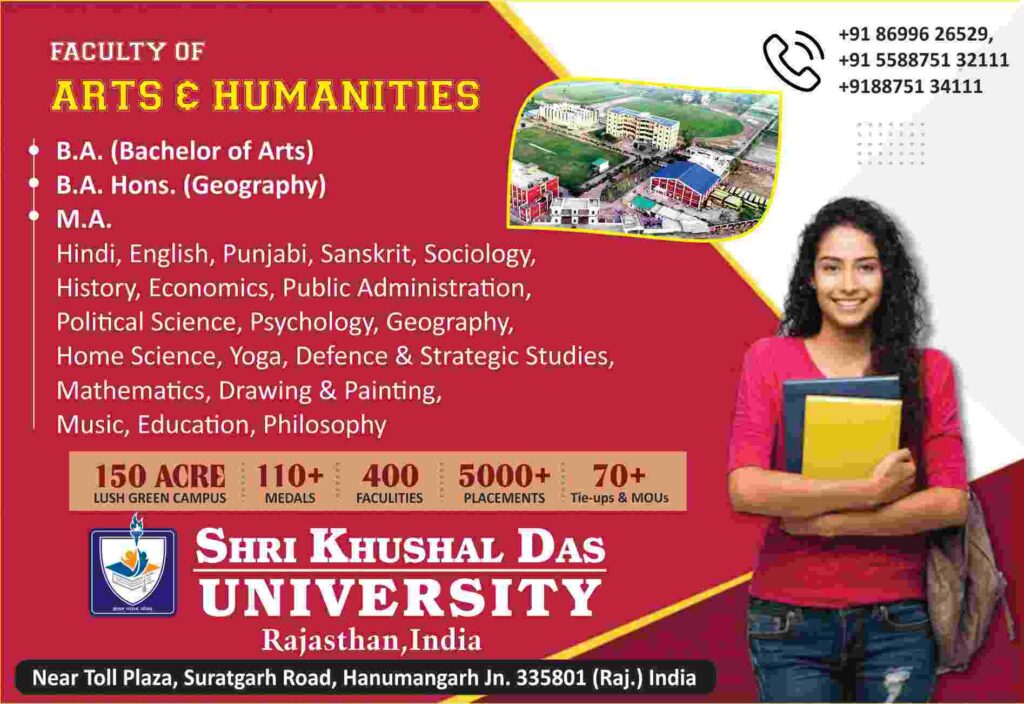
उनके अनुसार विदेशी कंपनियों के उत्पादों को स्वदेशी कहना संघ की मूल भावना के विपरीत है। इसी कारण कई स्वयंसेवक चुपचाप असहमति जता रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि संघ का घटक संगठन स्वदेशी जागरण मंच, जो कभी सक्रिय रूप से इस विचारधारा को आगे बढ़ाता था, अब परिदृश्य से लगभग गायब हो गया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंच की गतिविधियाँ ठप हो गई हैं। स्वयंसेवकों में यह खामोशी चुभती है, लेकिन वे खुलकर विरोध करने से बचते हैं।
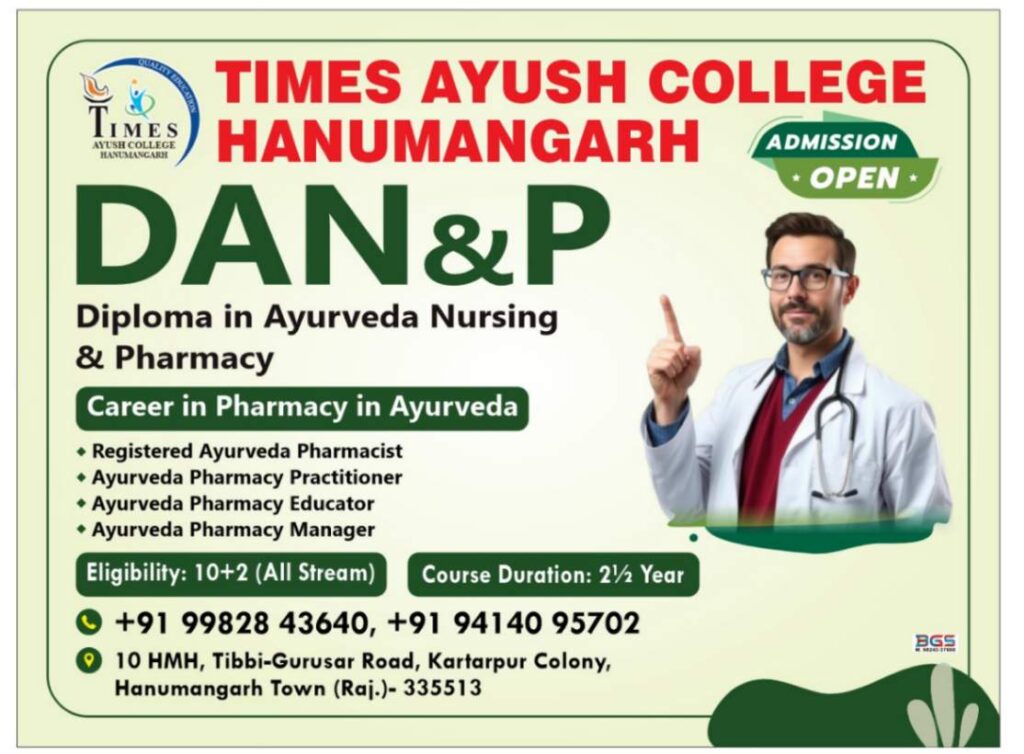
मोदी सरकार ने 2014 से ही आर्थिक सुधारों और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ‘मेक इन इंडिया’ इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें लक्ष्य विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और उत्पादन के लिए आकर्षित करना था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या विदेशी कंपनियों के उत्पादों को स्वदेशी कहना स्वदेशी के मूल दर्शन के साथ न्याय करता है?

कांग्रेस और विपक्षी दल इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। वे इसे गांधी के विचारों से विचलन और स्वदेशी की मूल भावना के साथ खिलवाड़ बताकर जनता के बीच मुद्दा बना सकते हैं। वहीं, भाजपा समर्थक इसे ‘व्यावहारिक स्वदेशी’ कहकर बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आज के वैश्विक दौर में पूर्ण स्वदेशी संभव नहीं। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान से स्वदेशी शब्द का अर्थ और मर्म अब बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ गांधी का स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर गाँव, छोटे उद्योग और स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। दूसरी तरफ मोदी का स्वदेशी है, जो विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी स्थान देता है, बशर्ते उत्पादन भारत में हो। आरएसएस के भीतर भी इस पर असहमति है। विचारधारा की इस खाई को आने वाले समय में और गहराई से महसूस किया जा सकता है। राजनीति में शब्दों की परिभाषा केवल भाषाई खेल नहीं होती, बल्कि वे नीतियों और दिशा को भी प्रभावित करती हैं।
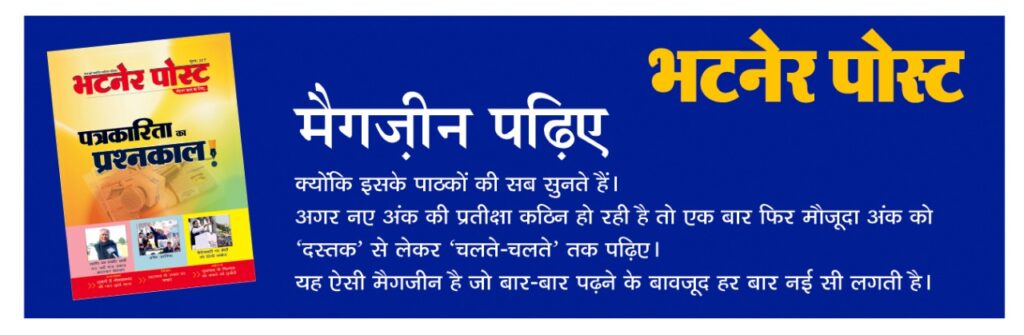
भारत की राजनीति में 2014 के बाद कई शब्दों और प्रतीकों को नए अर्थ दिए गए हैं। अब ‘स्वदेशी’ भी उसी कड़ी का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की नई व्याख्या ने जहां उपभोक्ताओं और व्यापारियों को संदेश दिया है, वहीं वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह बहस केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक भी है।
वरिष्ठ पत्रकार विमल चौहान कहते हैं, ‘आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा और संघ इस मतभेद को पाट पाएंगे या फिर स्वदेशी शब्द भारतीय राजनीति में एक नए वैचारिक विभाजन का कारण बनेगा।’