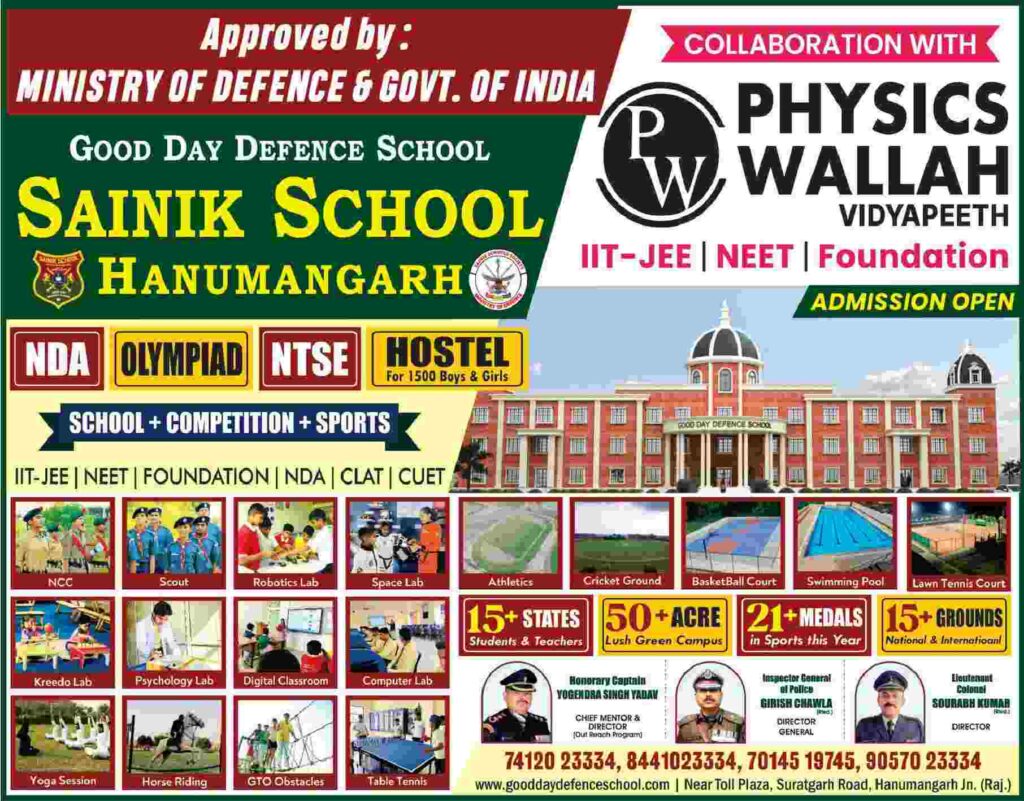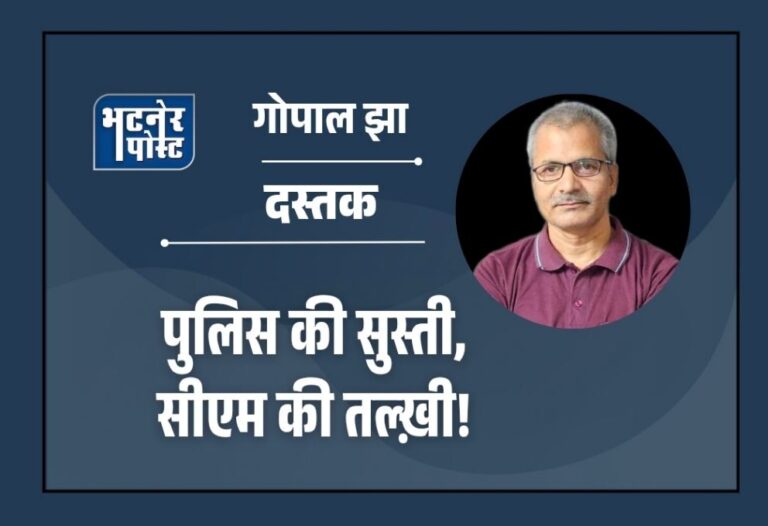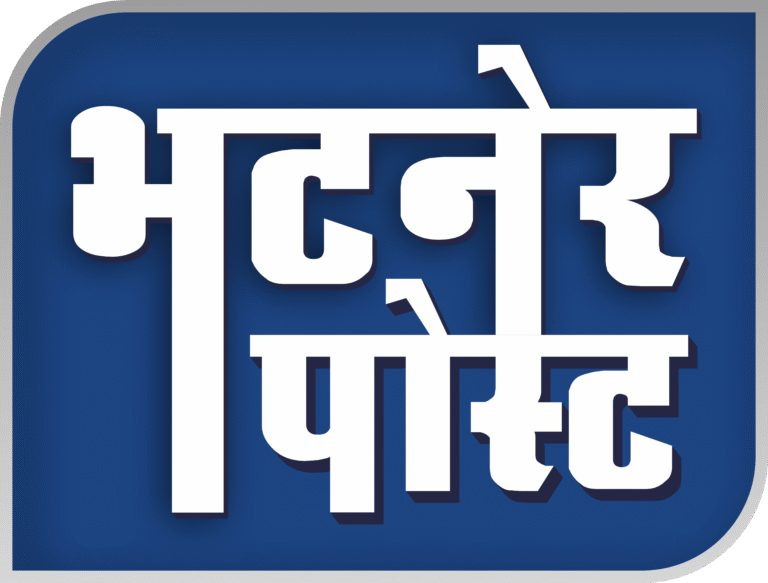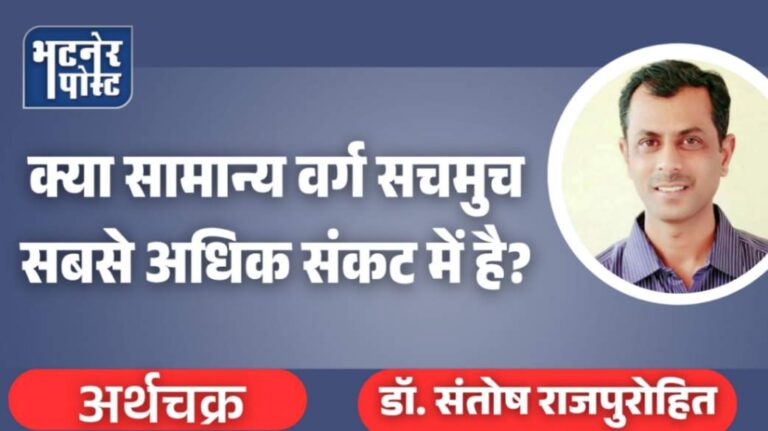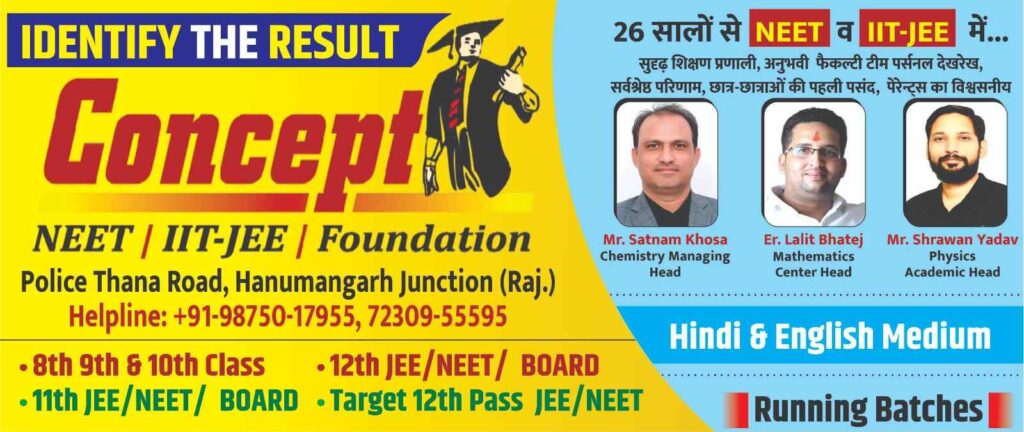

गोपाल झा.
कालखंड कैसा भी रहा हो, बिहार का महत्व सदैव बना रहा है। यह भूमि केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की गवाही है। ‘विहार’ से ‘बिहार’ बने इस राज्य का अतीत इतना समृद्ध रहा है कि पूरी दुनिया ने इसे कभी शिक्षा, ज्ञान, धर्म और संस्कृति के केंद्र के रूप में देखा। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों ने ज्ञान की मशाल जलाई थी, जिसकी रोशनी दूर देशों तक फैली थी। परंतु आज यही बिहार शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन की त्रासदी झेल रहा है।
बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने बिहार के 113 वर्षों की यात्रा गवाह है कि यहां के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अद्वितीय योगदान दिया। महात्मा गांधी को चंपारण की धरती ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। परंतु आज़ादी के बाद वही बिहार राजनीतिक असफलताओं, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक बंटवारे के दलदल में फंस गया। सवाल उठता है कि जो राज्य कभी राष्ट्र को प्रेरित करता था, आज वह स्वयं प्रेरणा से क्यों वंचित है?
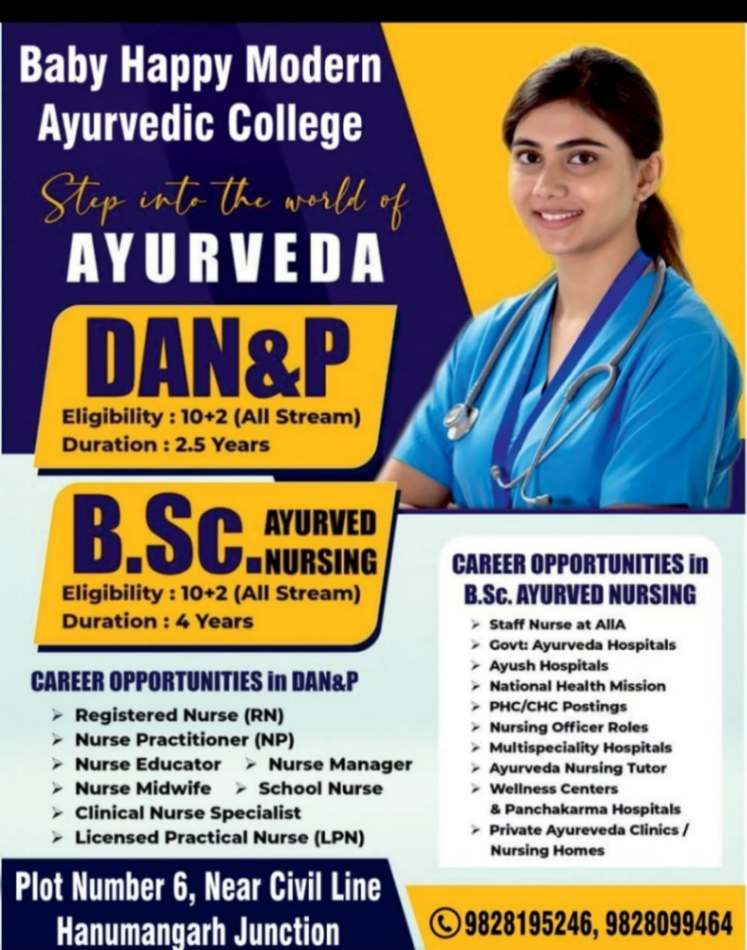
आज का सच यही है कि बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे और नौजवान देश और विदेश के विश्वविद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं। कभी ज्ञान का केंद्र रहे इस प्रदेश के विश्वविद्यालय अब छात्र राजनीति और संसाधनों की कमी के प्रतीक बन गए हैं। परिणाम यह हुआ कि ‘बिहारी’ पहचान को आज पलायन और मजदूरी से जोड़ा जाने लगा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या दक्षिण भारत का कोई भी कोना हो, आपको बिहारी मजदूर अवश्य मिलेंगे। यह विडंबना ही है कि जब दक्षिण भारत में हिंदी भाषियों पर हमले होते हैं तो सबसे अधिक शिकार भी बिहारी ही बनते हैं। यह स्थिति बिहार के आत्मसम्मान पर गहरी चोट करती है।

साढ़े तीन दशक का लंबा समय बीत चुका है, और इस दौरान बिहार विकास की मुख्यधारा से पीछे ही खड़ा नजर आता है। सरकारी आंकड़ों में रोजगार और विकास के सपने जरूर गढ़े जाते हैं, पर जमीनी हकीकत उन कागजों से मेल नहीं खाती। बिहार का एक बड़ा तबका अभी भी बदहाली की गिरफ्त में है। सच यह है कि राज्य के लगभग हर परिवार में कोई न कोई पलायन की विवशता झेल रहा है। ट्रेन की पटरी से लेकर महानगरों के फुटपाथ तक, बिहारी प्रवासियों की व्यथा हर जगह बिखरी पड़ी है।

राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो उम्मीद की किरण और भी धुंधली हो जाती है। चुनाव आते ही मुद्दे बदल जाते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसे बुनियादी प्रश्न गायब हो जाते हैं। उनकी जगह जाति, धर्म और अब ‘गाली’ जैसे हल्के विषय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ जाते हैं। यह स्थिति केवल नेताओं की विफलता का परिचायक नहीं, बल्कि जनता की चुप्पी का भी द्योतक है। जब समाज ही अपनी सबसे बड़ी समस्या को मुद्दा नहीं बनाता, तो नेताओं से बदलाव की अपेक्षा करना कैसे संभव है?

बिहार की यह विडंबना केवल वर्तमान की नहीं है; यह धीरे-धीरे गहराते उस संकट का परिणाम है, जिसे समाज ने स्वयं देखा, पर महसूस करने से इनकार किया। पलायन की पीड़ा हर घर की सच्चाई है, लेकिन चुनावी मंचों पर यह मौन हो जाती है। नेताओं के लिए जातीय समीकरण और धार्मिक ध्र्रुवीकरण वोटों की लहलहाती फसल तैयार करते हैं। और जनता भी उसी जाल में फंस जाती है।
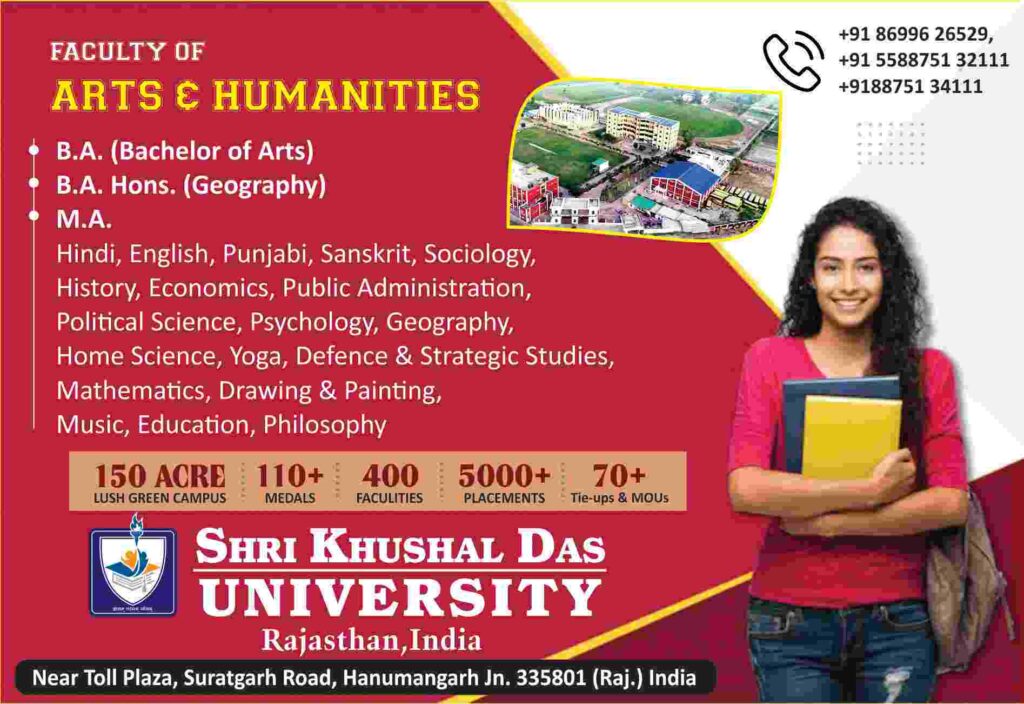
इतिहास गवाह है कि जब कोई समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है, तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बिहार के साथ भी यही हो रहा है। जिस धरती ने भगवान महावीर, बुद्ध, चाणक्य, गुरु गोबिंदसिंह, आर्यभट्ट, वात्सायन जैसे महान व्यक्तित्व दिए, वही धरती अब नेतृत्वहीनता और दिशाहीनता की शिकार हो गई है।
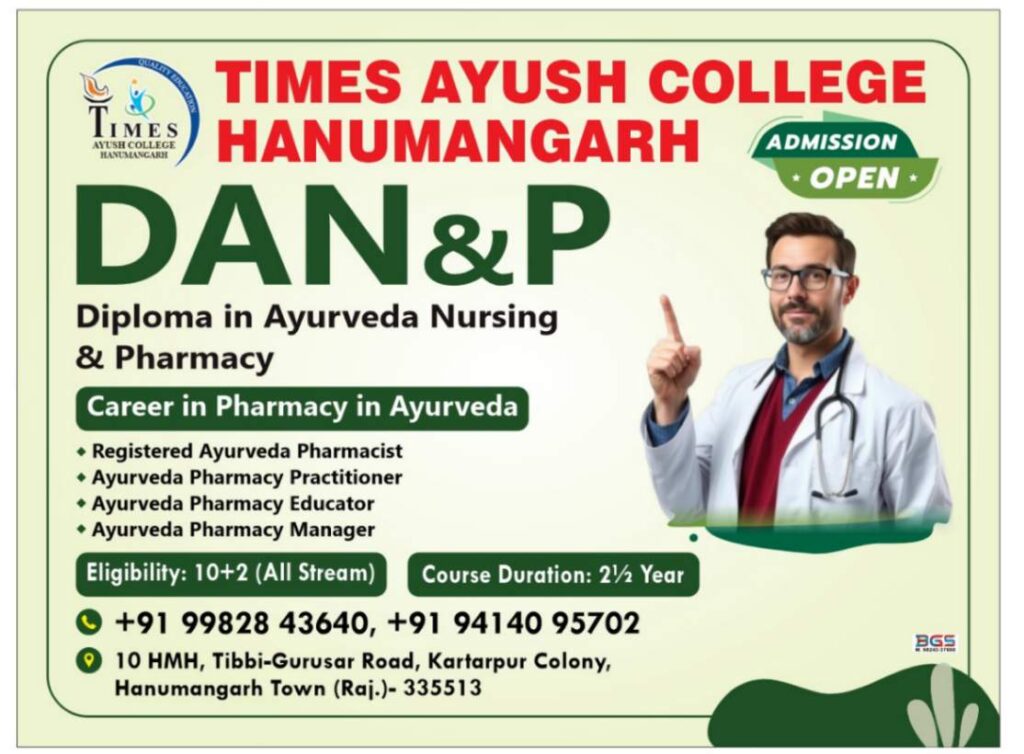
आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार अपनी पीड़ा को समझे और उसे मुद्दा बनाए। पलायन को मजबूरी नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु बनाया जाए। शिक्षा और रोजगार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। जब तक यह नहीं होगा, तब तक बिहार का इतिहास भले ही गौरवशाली रहे, पर वर्तमान बदहाल और भविष्य अनिश्चित ही बना रहेगा।
काश, कोई इस व्यथा को समझता। जनता भी यह ठान लेती कि अगली बार धर्म और जाति के चश्मे से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर वोट देगी। तभी बिहार की किस्मत बदलेगी और वह फिर से अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौट पाएगा।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर हैं