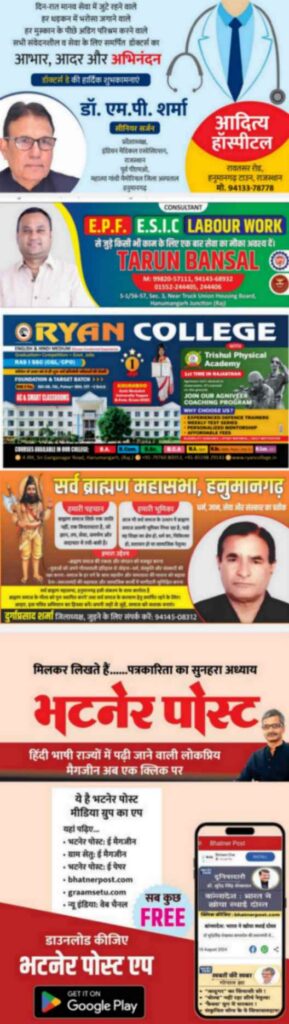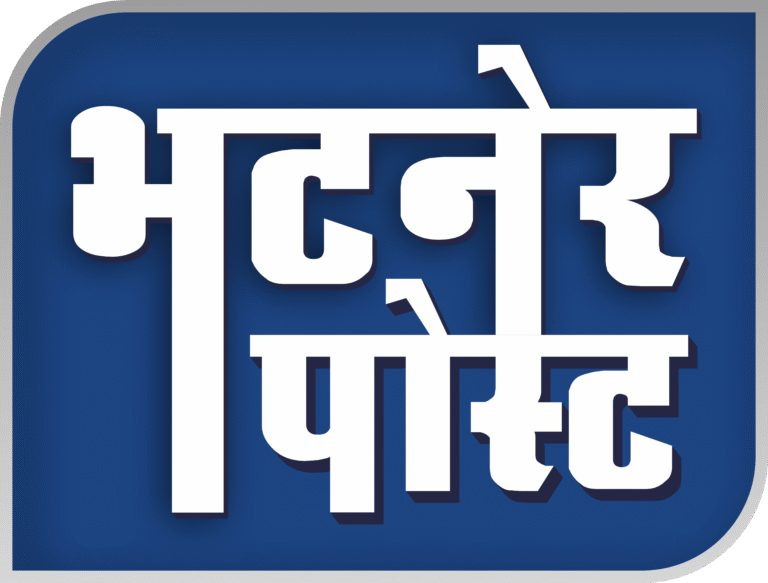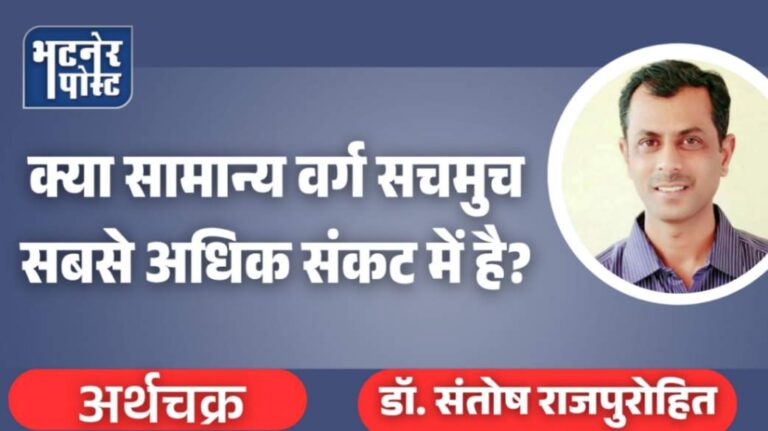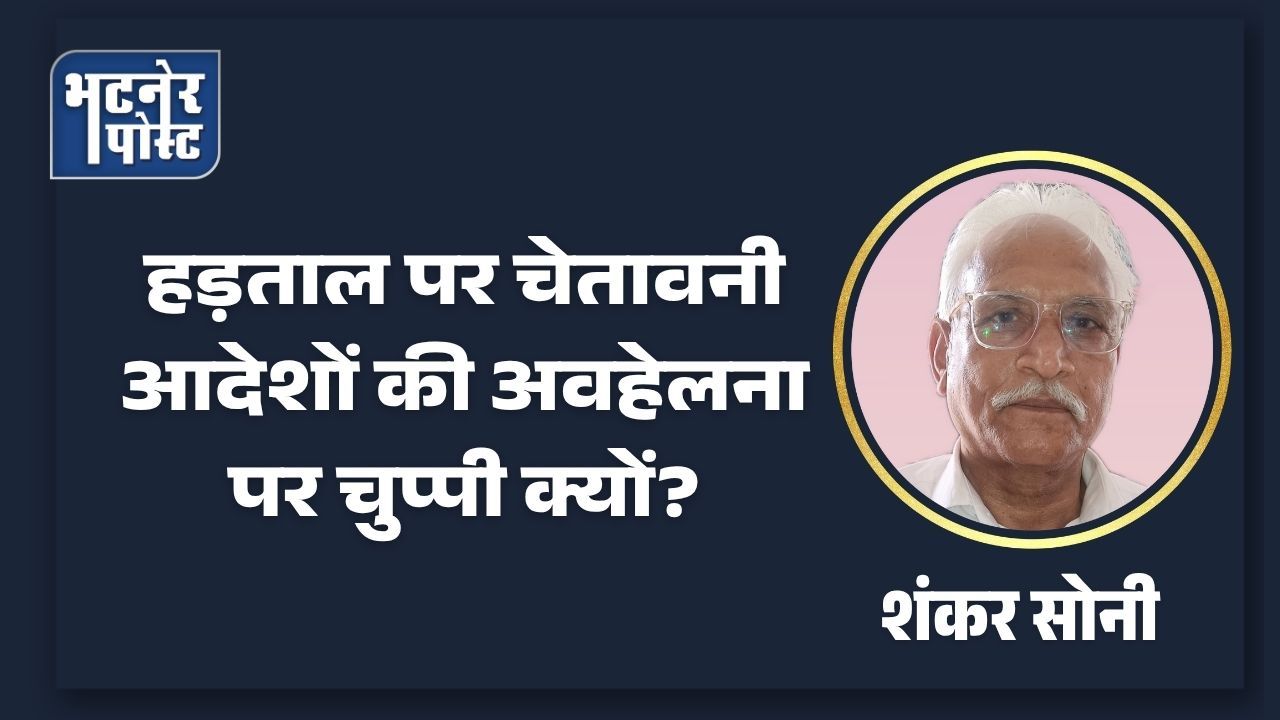
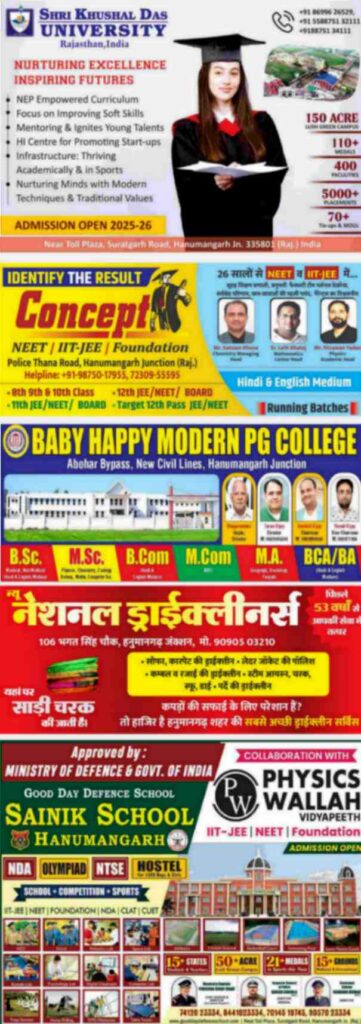
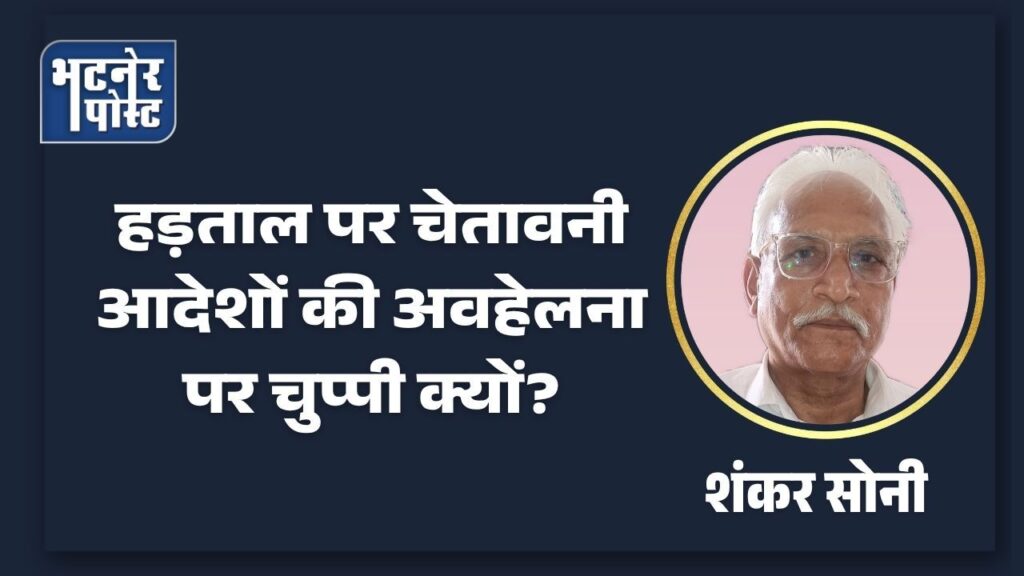
शंकर सोनी.
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारियों की हालिया हड़ताल एक बार फिर न्याय प्रणाली की नींव को झकझोरने वाली स्थितियों की ओर इशारा करती है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाला रहा माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन द्वारा पारित वह आदेश, जिसमें इस हड़ताल को ‘अवैध’ करार देते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू करने की चेतावनी दी गई। यह आदेश अब केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि गहरे संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों का विषय बन गया है।
सबसे पहला सवाल, क्या संबंधित पक्षों को न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिया गया? क्या कर्मचारियों की पीड़ा, उनके संघर्ष और लंबे समय से लंबित मांगों को जानने का प्रयास हुआ? आश्चर्य की बात यह है कि जिस आदेश में हड़ताल को अवैध घोषित किया गया, उसमें न तो कर्मचारी संघ को पक्षकार बनाया गया, न ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला।
यह स्थिति ‘प्राकृतिक न्याय’ के मूलभूत सिद्धांत ‘दूसरी पक्ष को भी सुना जाए’ का सीधा उल्लंघन प्रतीत होती है। न्यायालय स्वयं अनुशासन और निष्पक्षता के सर्वाेच्च रक्षक माने जाते हैं, लेकिन जब कोई आदेश एकतरफा होकर संवाद के अवसर को दरकिनार कर देता है, तो यह न केवल न्याय की आत्मा को आहत करता है, बल्कि व्यवस्था में विश्वास की नींव भी डगमगाने लगती है।
यह प्रसंग हमें वर्ष 2022 की उस न्यायिक पहल की याद दिलाता है, जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि वह न्यायिक कर्मचारियों के पदोन्नति ढांचे, वेतन असमानता और सेवाकालीन सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर कार्यवाही प्रारंभ करे। लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी न तो कोई ठोस नीति बनी, न ही समाधान की दिशा में कोई कदम उठाया गया। तो क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार सरकार को अब तक उत्तरदायी क्यों नहीं ठहराया गया?
यह विरोधाभास चौंकाने वाला है। यदि न्यायिक कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें ‘अवैध’ कहकर दबाने की चेतावनी दी जाती है। वहीं, सरकार जो वर्षों से न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना कर रही है, उससे कोई जवाब-तलबी नहीं होती!
इस समूचे प्रकरण का सार यही है, संवाद और संवेदनशीलता के बिना कोई भी समाधान टिकाऊ नहीं होता। राज्य की न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले न्यायिक कर्मचारी यदि लंबे समय से उपेक्षा और असमानता से त्रस्त हैं, तो इसका सीधा असर न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और गति पर पड़ता है।
यह स्पष्ट होना चाहिए कि समस्याओं का समाधान चेतावनियों, अधिनियमों या दमन से नहीं, बल्कि संवेदनशील संवाद, न्यायिक आदेशों की पारदर्शी पालना, और कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के सम्मान से ही संभव है। क्योंकि यदि न्यायपालिका के भीतर ही ‘सुनवाई का अधिकार’ उपेक्षित हो जाए, तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद और अधिक धूमिल हो जाती है।
समय की मांग है कि सरकार से स्पष्ट पूछा जाए कि 2022 के न्यायिक निर्देशों की पालना अब तक क्यों नहीं हुई? भविष्य में न्यायालय ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय सुनाए, जिससे न्याय की गरिमा और निष्पक्षता बनी रहे। न्याय केवल आदेशों में नहीं, उनके पीछे छिपे मूल्यों में होता है, और वह मूल्य है सुनवाई का अधिकार।
-लेखक सीनियर एडवोकेट हैं