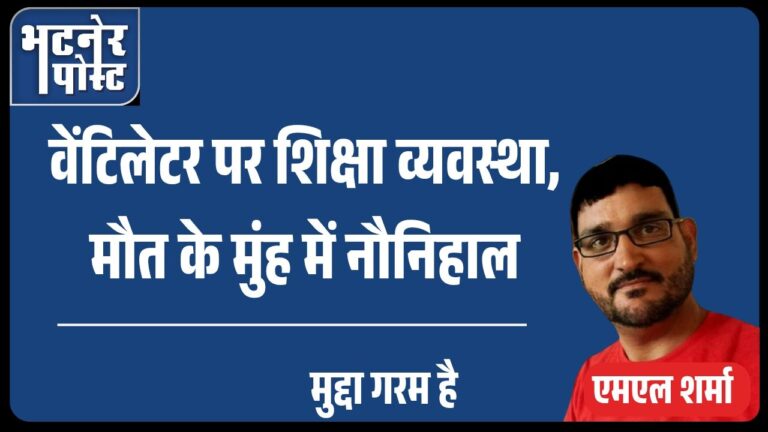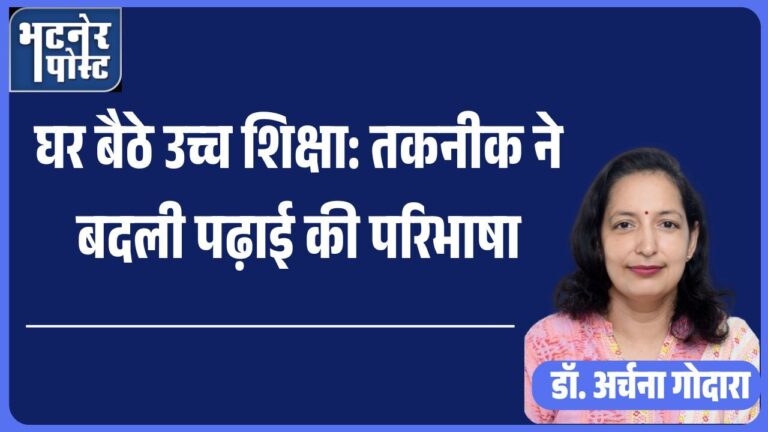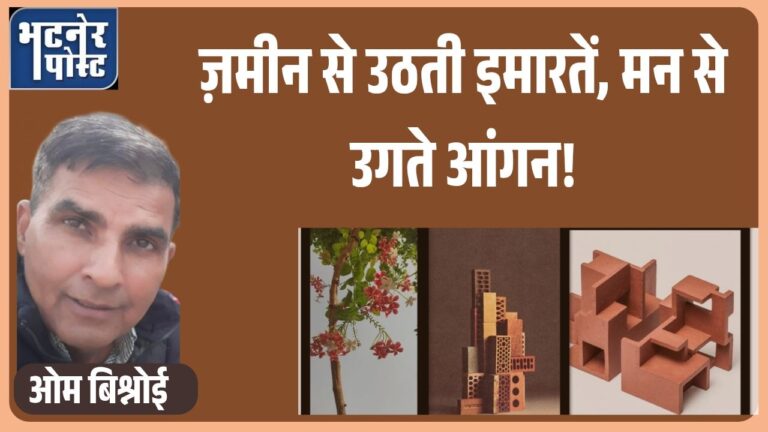डॉ. एमपी शर्मा.
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। यह केवल कोई श्लोक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का वह आदर्श है जो नारी को दिव्यता और गरिमा का प्रतीक मानता है। किंतु आधुनिक समाज में यह आदर्श केवल किताबों और भाषणों तक सीमित रह गया है। वास्तविकता में आज भी नारी को अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। घर से लेकर कार्यस्थल तक, शिक्षा से लेकर निर्णय प्रक्रिया तक, हर मोर्चे पर स्त्रियों को असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह विडंबना केवल नारी का नहीं, पूरे समाज के संतुलन और विकास का प्रश्न है। आज समय की मांग है कि हम लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को त्याग कर, समानता और सम्मान की नींव पर आधारित समाज की संरचना करें। इस आलेख में हम नारी के प्रति समाज की सोच, भेदभाव के मूल कारणों, और उनके समाधान की दिशा में उठाए जा सकने वाले ठोस कदमों पर विचार करेंगे।
यह सत्य है कि पुरुष और स्त्री के शरीर और जैविक कार्यप्रणालियों में भिन्नता होती है। लेकिन इन भौतिक भिन्नताओं को मानसिक, बौद्धिक या सामाजिक क्षमता का आधार बना देना सरासर अनुचित है। दुर्भाग्यवश, यही भेद धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्थाओं में स्थायी रूप ले चुका है। कई परिवारों में आज भी बेटियों को ‘पराया धन’ और बेटों को ‘वंश चलाने वाला’ माना जाता है। बाल्यकाल से लड़कों को निर्णय लेने की, और लड़कियों को सहने की शिक्षा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बेटियों की पढ़ाई आठवीं या दसवीं के बाद रुक जाती है, जबकि बेटों को कॉलेज तक भेजा जाता है। ‘घर की इज्जत लड़कियों से जुड़ी है’ जैसी सोच, महिला की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा है। विवाह, दहेज, विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों में समाज की सोच अब भी पुरुषवादी है। उदाहरणस्वरूप, विधवा स्त्री पर सामाजिक बंदिशें हैं, जबकि विधुर पुरुष को कोई सामाजिक दंड नहीं मिलता। जहां शिक्षा का अभाव होता है, वहां स्त्रियों की भूमिका केवल घरेलू सीमाओं में ही परिभाषित होती है। अशिक्षित महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं। पुरुष-प्रधान समुदायों में महिला को केवल गृहणी और सेवा-कर्ता की भूमिका में सीमित कर दिया जाता है।

एक बड़े वर्ग में यह धारणा है कि निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुषों को है। कई घरों में महिलाएं अभी भी वोट देने, नौकरी करने या यात्रा के लिए भी पुरुषों से अनुमति लेती हैं। यह सोच सामाजिक असमानता को गहराई देती है। यह सच है कि विज्ञापन, धारावाहिक और फिल्में कई बार महिलाओं को वस्तु या कमजोर रूप में प्रस्तुत करती हैं। ‘ग्लैमर’ और ‘सौंदर्य’ को महिला की पहचान बना दिया गया है। इससे नई पीढ़ी में महिला की भूमिका को लेकर गलत धारणाएं बनती हैं।
इस तरह की समस्याओं का अंत या बदलाव की शुरुआत परिवार से हो। लड़का-लड़की दोनों को समान अवसर और अधिकार मिलें। लड़कों को भी घरेलू कार्य, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सहयोग की शिक्षा मिले। उदाहरणस्वरूप, घर के कार्यों में दोनों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो। बेटियों की शिक्षा में कोई समझौता न हो। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ को घर-घर तक पहुँचाना आवश्यक है। महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारतीय संविधान ने लिंग के आधार पर समानता का अधिकार दिया है। घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम जैसे कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचे। महिला हेल्पलाइन नंबरों की जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

फिल्मों, साहित्य और विज्ञापनों में महिलाओं की सशक्त छवि को दिखाना जरूरी है। स्कूलों-कॉलेजों में ‘जेंडर सेंसिटिविटी वर्कशॉप्स’ अनिवार्य की जाएं। ऐसे किरदारों को बढ़ावा मिले जो लैंगिक समानता को दर्शाते हैं। यह समझना जरूरी है कि स्त्री कोई प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि समान अधिकारों की सहभागी है। पुरुषों को महिलाओं की स्वतंत्रता को सहानुभूति नहीं, संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकारना होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव एक ऐसी सामाजिक बीमारी है, जिसे केवल कानून से नहीं, सोच और संस्कारों में परिवर्तन लाकर ही समाप्त किया जा सकता है। परिवार, विद्यालय, मीडिया, शासन और समाज सभी को मिलकर एक ऐसी संस्कृति गढ़नी होगी जिसमें लिंग नहीं, गुण और योग्यता ही मूल्यांकन का आधार हो। जब बेटियों को भी वही सम्मान, वही अवसर, और वही मंच मिलेगा जो बेटों को मिलता है; जब पुरुष स्त्रियों को अपने बराबर का समझेगा, तभी एक सशक्त, समतावादी और संवेदनशील समाज की कल्पना साकार हो सकेगी। नारी कोई अबला नहीं, शक्ति का स्वरूप है, बस उसे पहचानने और स्वीकारने की देर है।
-लेखक सीनियर सर्जन, सामाजिक चिंतक व आईएमए राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं