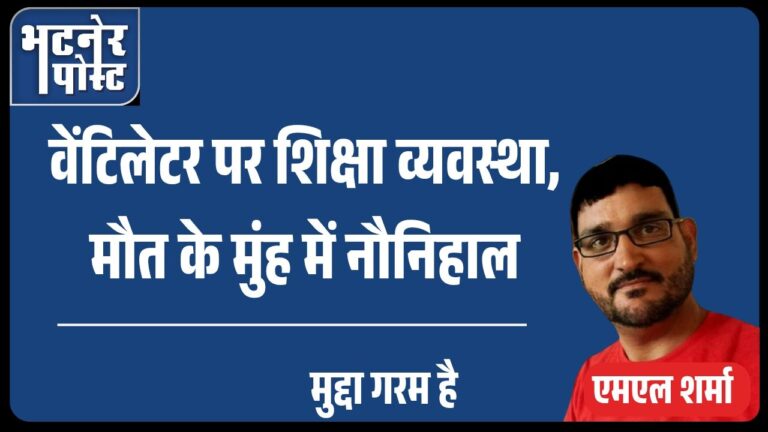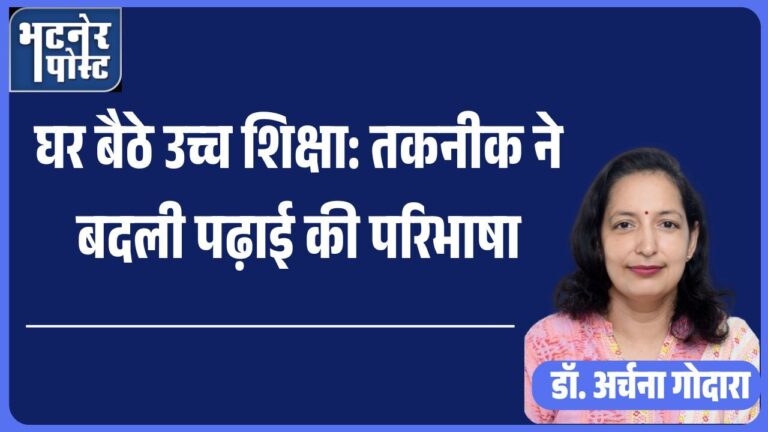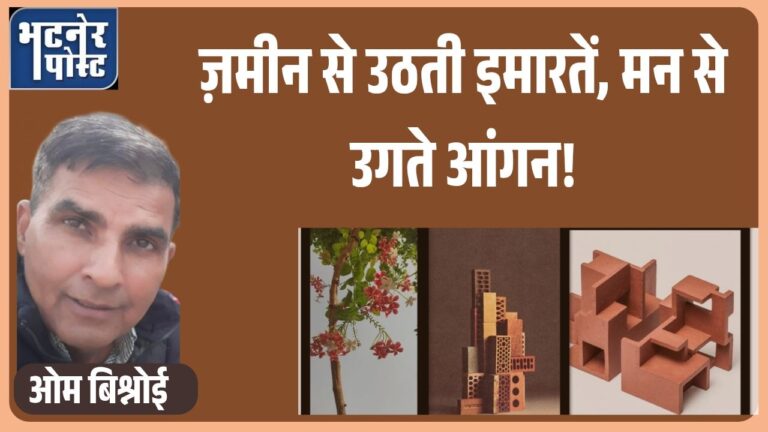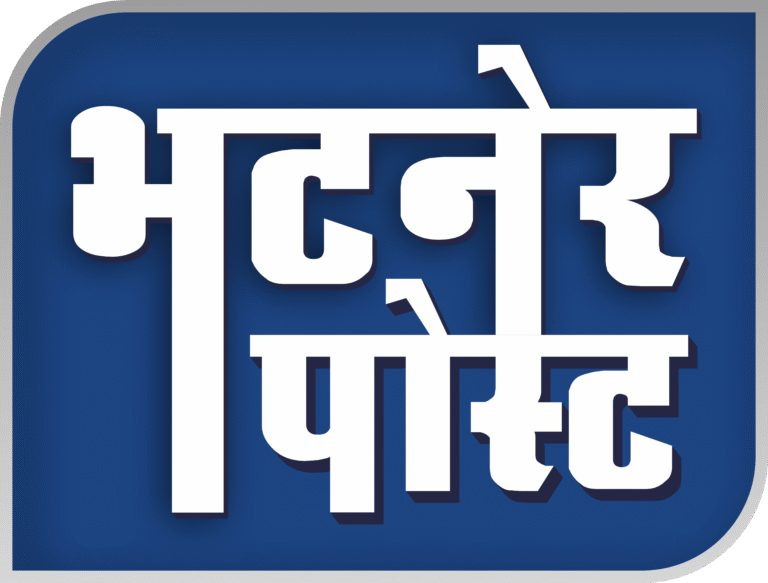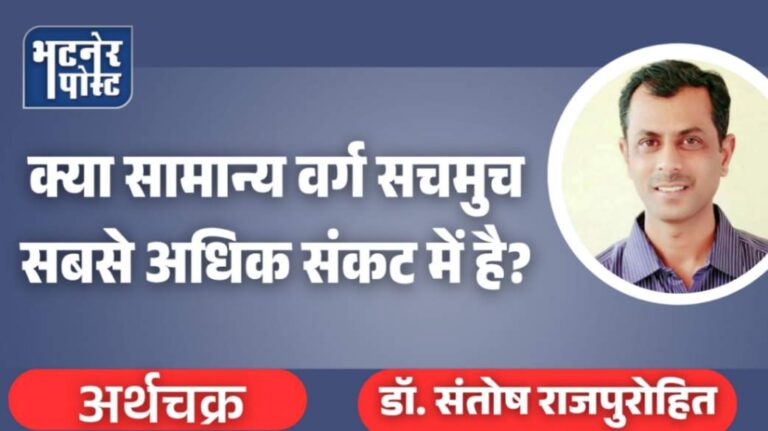डॉ. अर्चना गोदारा.
रोशनी की चमक और पैसों की खनक इतनी थी कि दौड़ा चला गया। जब रुका तो देखा, अकेला खड़ा हूं। किससे कहूं कि थक गया भागते- भागते। भागदौड़ और तेज रफ्तार से भरे शहरी जीवन में जहाँ हर व्यक्ति किसी ना किसी मंज़िल या बिना मंजिल बस मौज मस्ती की तलाश में दौड़ रहा है, वहीं पारिवारिक संरचना भी इसके प्रभाव स्वरूप चुपचाप एक बड़ा बदलाव झेल रही है। आज के समय में जब ऊँची इमारतें, वातानुकूलित दफ्तर और तकनीकी जुड़ाव को आधुनिक जीवन की पहचान माना जाता है, तब व्यक्ति को यह पता ही नहीं लग पाता कि इन सुविधाओं की चकाचौंध में वह धीरे-धीरे अकेला होता जा रहा हैं। पारम्परिक संयुक्त परिवार प्रणाली जो कभी सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहारे की प्रतीक थी, वो अब शहरों में ना के बराबर रह गई हैं। उसकी जगह एकल या लघु परिवार ने ले ली है। एकल परिवार में माता-पिता तथा उनके जन्मे हुए बच्चे ही रहते हैं। यानी की एकल परिवारों में अधिकतम दो पीढ़ी ही एक साथ रहती हैं। इस बड़े बदलाव ने समाज में व्यक्ति के लिए गहरी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।
शहरीकरण के साथ-साथ लोगों ने भौतिक सुख-सुविधाओं को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन सामाजिक रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कहीं पीछे छूट गया है। अकेलेपन की यह स्थिति केवल वृद्धों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि युवा वर्ग भी इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। उच्च शिक्षा, नौकरी और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह में जब युवा घर से दूर महानगरों में बसते हैं, तो वे सामाजिक रूप से स्वयं को काट लेते हैं। उनके पास समय नहीं होता कि वे नज़दीकी रिश्ते बना सकें, और जो बनते हैं वो अक्सर सतही होते हैं। ऐसे में अकेलेपन के कारण व्यक्ति मे मानसिक तनाव, अवसाद, नींद की कमी, और आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं और इनका एक बड़ा कारण सामाजिक अलगाव है। यही कारण है कि बड़े-बड़े टीवी स्टार एक दिन अपने आलीशान घर में चुपचाप आत्महत्या कर लेते हैं।
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, जिसे भावनात्मक सहारे, संवाद और अपनेपन की गहरी आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था कि ‘प्यार और जुड़ाव की कमी मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है।’ जब हम अपने घर में भी एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, तो परिवार केवल चार दीवारों का ढाँचा ही रह जाता है। वर्तमान जीवन शैली में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को निजी बनाए रखना चाहता है, घरवालो से भी वह औपचारिकता पूर्ण व्यवहार करता है। माता-पिता अपने करियर में व्यस्त रहते हैं, बच्चे तकनीक में उलझे रहते हैं, और बुज़ुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं हैं। यह स्थिति धीरे-धीरे मानसिक थकान और तनाव को जन्म देती है, जिसे समझने और हल करने की बेहद सक्त ज़रूरत है।
यह विडंबना ही है कि जिन शहरों में लाखों लोग रहते हैं, वहाँ लोग सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जब सार्वजनिक रूप से अपने अवसाद का ज़िक्र किया, तो उन्होंने बताया कि कैसे ग्लैमर और सफलता के बावजूद वह खुद को भीतर से टूटा हुआ महसूस करती थीं। उन्हें बार-बार रोना आता था। कभी-कभी समझ में नहीं आता था कि वह क्यों रो रही है? इसी प्रकार से आमिर खान की बेटी इरा ने भी स्वयं के तनाव ग्रस्त होने की बात को कहा था। यह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे और जान पहचान की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी ये तनावग्रस्त हैं। यह दोनों उदाहरण इस बात के प्रतीक है कि तनाव किसी भी स्तर पर, किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकता है। इसका पद, पैसे और स्तर से कोई लेना-देना नहीं।
शहरी जीवन में अकेलेपन का यह भाव साहित्य और कला में भी झलकता है। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ इस सच्चाई को सजीव कर देती हैं,
भीड़ में जब कोई अपना न दिखे,
हर शाम एक सन्नाटा भीतर चुभे।
रिश्ते हैं पर रिश्ता नहीं कोई पास,
शहर में है रौशनी, पर दिल में उदास।
इस समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि भावनात्मक पुनर्संरचना से हो सकता है। हमें संवाद की परंपरा को फिर से जीवित करना होगा। घर में, परिवार में, आस-पड़ोस में फिर से एक-दूसरे के हालचाल पूछना, समय देना, और केवल ष्कनेक्टष् नहीं बल्कि ‘कनेक्टेड’ महसूस करना आवश्यक है। बातचीत, बधाई और समय पास केवल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा ही नहीं करना है बल्कि आमने-सामने मिलकर चाय के प्याले के साथ करना होगा।
शहर भले ही कितने भी आधुनिक और सुविधायुक्त क्यों ना हों, लेकिन मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें आज भी वही हैं कृ अपनापन, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव आदि। जब तक हम इन मूल्यों को अपने जीवन में पुनः नहीं लाएंगे, तो तनाव की यह लहरे ऊंची होती-होती गहरी हो जाएगी। हमें यह समझना होगा कि प्रगति केवल तकनीक, पैसे और भवनों से नहीं, बल्कि मजबूत रिश्तों और मानसिक शांति से मापी जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो हमें परिवार को फिर से ‘घर’ बनाना होगा, एक ऐसा स्थान जहाँ न केवल सदस्य साथ में रहें, बल्कि एक-दूसरे के जीवन में वास्तविकता के साथ मौजूद भी हों।
-लेखिका राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में सहायक आचार्य हैं