



गोपाल झा.
रात थी, लेकिन वह अंधेरा केवल आकाश में नहीं, इतिहास के पन्नों पर भी उतर आया था। 14 अगस्त 1947, वह तारीख, जो एक तरफ़ आज़ादी के सपनों को सच में तब्दील कर रही थी, तो दूसरी तरफ़ करोड़ों दिलों में बिछड़ने की चुभन, कत्लेआम की आग और विस्थापन का दर्द हमेशा के लिए सींच गई। इसी रात, भारत के शरीर को चीर कर एक नया मुल्क जन्मा, पाकिस्तान। अगले दिन भारत में तिरंगा फहराया गया, देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी में लहू की गंध भी घुली हुई थी।
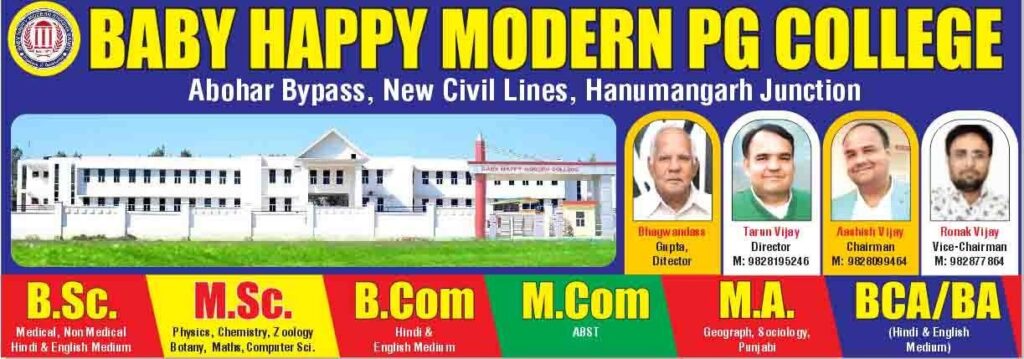
करीब आठ दशक बीतने वाले हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मधुरता का कोई वसंत नहीं आया। पाकिस्तान ने जन्म के साथ ही अपने अस्तित्व की बुनियाद भारत-विरोध पर रखी। नफ़रत उसका स्थायी मंत्र बन गया। अपने विकास की राह तलाशने के बजाय वह बार-बार सीमा पार आतंक के बीज बोता रहा। नतीजा यह कि आज वह खुद ही आतंकवादियों का मोहरा बन चुका है, एक ऐसा देश, जो अपने ही बनाये जाल में फँसकर बर्बादी की दहलीज़ पर खड़ा है।
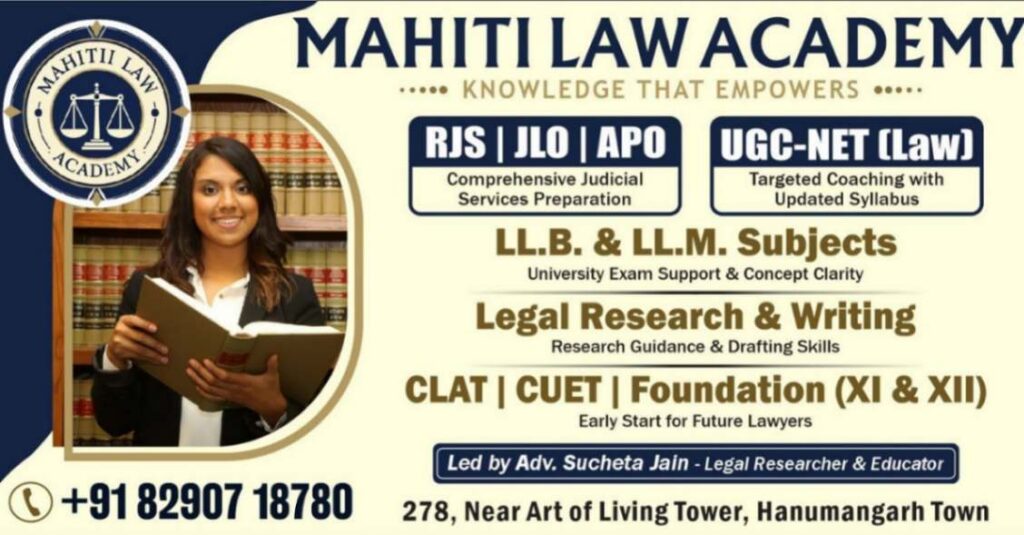
भारत में भी समय के साथ बहुत कुछ बदला। सत्ता के स्वर, राजनीति का रंग और राष्ट्रवाद की परिभाषा, सबमें रूपांतरण आया। ख़ासकर 2014 के बाद भारत का चेहरा अलग अंदाज़ में नज़र आने लगा। संसद में बैठी सत्ताधारी जमात, जो लगातार ग्यारह साल से सत्ता का रसपान कर रही है, लेकिन अब भी लगभग हर समस्या का दोष विपक्ष पर मढ़ने में कोई हिचक महसूस नहीं करती। यह प्रवृत्ति केवल राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली की झलक भी देती है।

नई पीढ़ी को एक नई घुट्टी पिलाई जा रही है कि भारत का विभाजन गांधी और नेहरू की वजह से हुआ। यह आरोप हवा में तैरता है, लेकिन धरातल पर इसके समर्थन में ठोस साक्ष्य नहीं मिलते। इतिहास का विद्यार्थी यदि निष्पक्ष दृष्टि से पन्ने पलटे तो पाएगा कि इसके पीछे कई परतें थीं, और कई ऐसे चेहरे थे जिनकी भूमिका पर चर्चा से आज भी परहेज़ किया जाता है।
उदाहरण के लिए, विनायक दामोदर सावरकर। हिंदू महासभा के अध्यक्ष। वही सावरकर, जो ‘दो राष्ट्र’ के सिद्धांत के पैरोकार थे। उनका स्पष्ट मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग कौमें हैं, जो एक साथ नहीं रह सकतीं। यह विचार महज़ मतभेद नहीं, बल्कि उस दौर के तनावपूर्ण माहौल में आग में घी डालने जैसा था। डॉ. हेडगेवार भी, जो आरएसएस के संस्थापक थे, इसी सिद्धांत को आधार बनाकर संगठन के विस्तार में जुटे हुए थे।

दूसरी तरफ़, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राष्ट्रवाद को खुलेआम हवा दे रहे थे। अंग्रेज़ों की नीति ‘फूट डालो और राज करो’ इन दोनों के लिए अनुकूल ज़मीन तैयार कर रही थी। वे एक ओर जिन्ना को प्रोत्साहित करते, तो दूसरी ओर सावरकर को भी, ताकि सांप्रदायिक खाई गहरी होती जाए और वह जाते-जाते भारत की आत्मा को छलनी कर सके।
इस परिदृश्य में गांधी का संघर्ष अलग और सबसे कठिन था। वे तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे थे। हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखना, आज़ादी की लड़ाई को अखंड भारत के सपने के साथ आगे बढ़ाना, और अंग्रेज़ों की चालों को नाकाम करना। गांधी ने बार-बार कहा, ‘बंटवारा मेरी लाश पर होगा’, लेकिन भीषण दंगों, अविश्वास और कट्टरता की आँधी के सामने यह संकल्प भी ढह गया।

तो सवाल उठता है, इन दंगों और विभाजन के लिए असल दोषी कौन था? क्या गांधी, जो अंतिम क्षण तक एकता की डोर थामे रहे, या सावरकर, जो हिंदुओं को भड़काने में लगे थे, या जिन्ना, जो मुसलमानों को अलग राष्ट्र के लिए उकसा रहे थे? या फिर वे अंग्रेज़, जिनके हाथों में इन सबकी डोर थी?
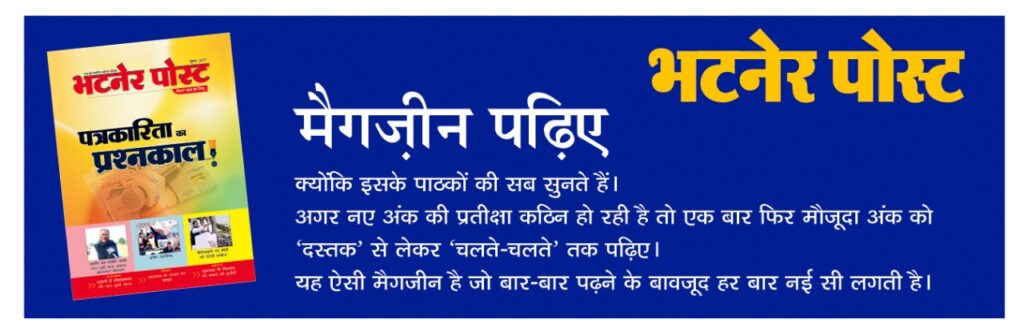
सावरकर के जीवन की एक और कड़ी इस बहस में महत्वपूर्ण है। सेल्युलर जेल में रहने तक वे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, लेकिन माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आने के बाद उनका मार्ग बदल गया। अंग्रेजों से लड़ने के बजाय वे कांग्रेस और ख़ासकर गांधी के घोर विरोधी बन गए। सावरकर हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ने पर आमादा थे और गांधी ढालकर बनकर खड़े थे। यही था उनकी नाराज़गी का मूल कारण। सावरकर की सोच का एक प्रतीकात्मक उदाहरण, हिंदू महासभा के अख़बार में छपा वह कार्टून, जिसमें रावण के दस सिरों में गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाषचंद्र बोस और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं के चेहरे बनाए गए थे। सोचिए, जब पूरा देश अंग्रेज़ी साम्राज्य से जूझ रहा था, उस समय ऐसे वैचारिक हमले क्या संदेश देते थे?
इतिहास में यह तथ्य छुपाया नहीं जा सकता कि जेल से छूटने के बाद सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम से सीधा संबंध टूट गया था। वे हिंदुत्व के राजनीतिक स्वरूप को अंग्रेज़ों की मौन सहमति से आगे बढ़ाने लगे थे।
विभाजन निस्संदेह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक ऐसी घटना जिसने लाखों परिवार उजाड़ दिए, लाखों को शरणार्थी बना दिया, और लाखों को बेमौत मार दिया। लेकिन इस त्रासदी का दोषारोपण केवल किसी एक व्यक्ति या दल पर करना, इतिहास के साथ अन्याय है। ज़रूरत है इस पर मंथन की। न किसी विचारधारा की ऐनक लगाकर, न किसी दलगत निष्ठा से, बल्कि एक सच्चे नागरिक के रूप में। क्योंकि इतिहास तब ही न्यायपूर्ण बन सकता है, जब हम उसके सभी पात्रों के चेहरे साफ़-साफ़ देखने का साहस रखें, उनकी रोशनी भी, और उनकी परछाइयाँ भी।

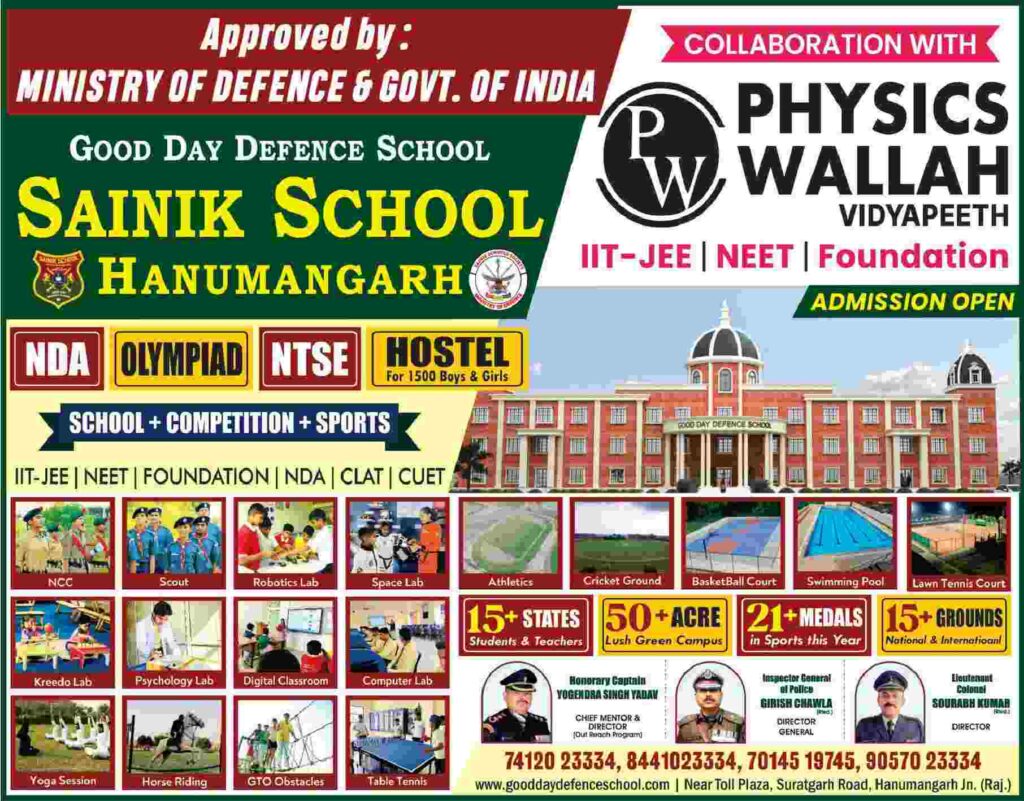




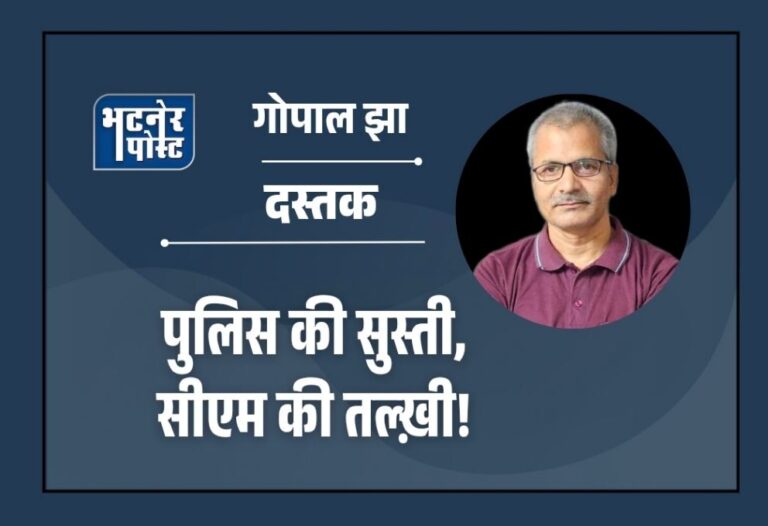





मैं सनातनी हूं। सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इतिहास की घटनाओं को उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आपके इन विचारों से मै सहमत नहीं हूं।सावरकर के बारे में मैंने काफी अध्ययन किया है। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई भी कुछ भी लिख सकता है। खिलाफत आंदोलन के बाद मोपला और कलकत्ता में जो हुआ पहले उसका अध्ययन करें उन परिस्थितियों में हिंदुओं को एक होकर ताकत बढ़ाने का आह्वान सावरकर ने किया । कभी पूर्वाग्रह
छोड़कर खुले मंच पर सौहाद्र पूर्ण बहस रखें।